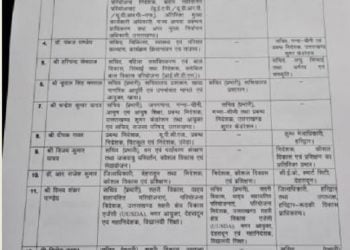डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
सरसों क्रूसीफेरी ब्रैसीकेसी कुल का द्विबीजपत्री, एकवर्षीय शाक जातीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्प्रेसटिस है। पौधे की ऊँचाई १ से ३ फुट होती है। इसके तने में शाखा.प्रशाखा होते हैं। प्रत्येक पर्व सन्धियों पर एक सामान्य पत्ती लगी रहती है। पत्तियाँ सरल, एकान्त आपाती, बीणकार होती हैं जिनके किनारे अनियमित, शीर्ष नुकीले, शिराविन्यास जालिकावत होते हैं इसमें पीले रंग के सम्पूर्ण फूल लगते हैं जो तने और शाखाओं के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। फूलों में ओवरी सुपीरियर, लम्बी, चपटी और छोटी वर्तिकावाली होती है। फलियाँ पकने पर फट जाती हैं और बीज जमीन पर गिर जाते हैं। प्रत्येक फली में ८.१० बीज होते हैं। उपजाति के आधार पर बीज काले अथवा पीले रंग के होते हैं। इसकी उपज के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। सामान्यतः यह दिसम्बर में बोई जाती है और मार्च.अप्रैल में इसकी कटाई होती है।
भारत में इसकी खेती पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात में अधिक होती है। भारत में मूँगफली के बाद सरसों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो मुख्यतया राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं असम में उगायी जाती है। सरसों की खेती कृषकों के लिए बहुत लोकप्रिय होती जा रही है क्योंकि इससे कम सिंचाई व लागत से अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसकी खेती मिश्रित फसल के रूप में या दो फसलीय चक्र में आसानी से की जा सकती है। सरसों की कम उत्पादकता के मुख्य कारण उपयुक्त किस्मों का चयन असंतुलित उर्वरक प्रयोग एवं पादप रोग व कीटों की पर्याप्त रोकथाम न करना आदि हैं सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने और शरीर में लगाने में किया जाता है। इसका तेल अंचार, साबुन तथा ग्लिसराल बनाने के काम आता है। तेल निकाले जाने के बाद प्राप्त खली मवेशियों को खिलाने के काम आती है। खली का उपयोग उर्वरक के रूप में भी होता है। इसका सूखा डंठल जलावन के काम में आता है। इसके हरे पत्ते से सब्जी भी बनाई जाती है। इसके बीजों का उपयोग मसाले के रूप में भी होता है।
यह आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसका तेल सभी चर्म रोगों से रक्षा करता है। सरसों रस और विपाक में चरपरा, स्निग्ध, कड़वा, तीखा, गर्म, कफ तथा वातनाशक, रक्तपित्त और अग्निवर्द्धक, खुजली, कोढ़, पेट के कृमि आदि नाशक है और अनेक घरेलू नुस्खों में काम आता है। जर्मनी में सरसों के तेल का उपयोग जैव ईंधन के रूप में भी किया जाता है। सर्दी का मौसम खिसकने की तैयारी में होता है तो वासंती सपने हौले से जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। खुली आंखों से दिख रहे इन सपनों की शुरूआत होती है हरे रंग की गोद में खुशबू में लिपटे हुए सुर्ख पीले रंग के फूलों से। चाहे पतझड़ की उदासी प्रकृति को वीरान करने पर तुली हो मगर छोटी-छोटी गोल मटोल सरसों के बड़े बड़े लहलहाते खेत जीवन में बहार ला देते हैं।
ऐसा लगता है जीवन की बंजर होती जा रही धरती में भी बसंत आ गया। सरसों के खेत प्रकृति के विराट आंगन में बिछे मखमली गलीचे की मानिंद लगते हैं। मन करता है इतिहास से अपने बचपन को निकाल कर प्रकृति की गोद में उन्मुक्त छोड़ दिया जाए। वैसे भी निर्मल आनंद के लिए कोई उम्र बाधा नहीं होती। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरियाली में बिछी सरसों की पीलिमा का आकर्षण अन्य फूलों जैसा ही है। माना भी गया है कि पीला रंग जिज्ञासाए जीवंतता एवं उल्लास का संदेशवाहक है इसलिए यह विशिष्ट रंग यहां भी खूब रंग जमाता है। सरसों लहलहाती है तो किसानों को व्यवसायिक अनुभूति होती है मानो खेतों में पीला सोना उग आया हो। उनको अपने सपने पूरे होते दिखते हैं। सरसों का महत्त्व कभी कम नहीं हुआ बल्कि समय के साथ बढ़ता ही गया। इतिहास में दर्ज है कि ईसा से 1800 वर्ष पूर्व जब आर्य इस धरती पर आए तब भी सरसों का उपयोग होता था। ईसा से अधिकतम 2300 बरस पहले सिन्धु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ों व हड़प्पा में हुई खुदाई बताती है कि मांस पकाने के लिए सरसों का तेल प्रयोग होता थाए सरसों के बीज मिले हैं एक जगह छानुदाड़ों से।
हमारे देश में भूरी सरसों, पीली सरसों, तोड़िया, तोरिया व राई की मिश्रित फसल को उगाया जाता है जिसे तिलहनी फसल भी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम ब्रेसिका है जो कुसिफेरी फैमिली की है। भारत में सरसों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, हिमाचल में ज्यादा होती है अन्य राज्यों में भी होती है मगर कम। पीली सरसों के दूसरे नामों में बंगा सरसों, रारा, राड़ा सरसम शामिल हैं। खाने में सरसों के तेल के बाद नम्बर आता है सरसों के साग का।
पंजाब की सरसों का साग जो अपनी पक्की सहेली मक्की की रोटी के साथ दुनिया भर में मशहूर है। मक्की का आटा पहाड़ी मीठी मक्की का और घराट में पिसा हो और रोटी चूल्हे में सिकी हो तो स्वाद कई गुणा बढ़ कर स्मरणीय हो जाता है। खाने में बाजरे की रोटीए लस्सी व सरसों के साग का संगम कई स्वादों को फीका कर देता है। साग खाने वालों को बासी साग और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ग्रामीण अंचल का तो बेहद स्वीकृत व प्रसिद्ध आहार है ही सरसों का साग। बात फिर लौट कर सरसों के खेतों पर लहलहाते पीले फूलों पर आती है। इन पीले बासंती फूलों ने कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों को भी कम आकर्षित नहीं किया। कितनी कविताओं, लोकगीतों व कहानियों में सरसों की महक के फूल खूबसूरती से खिले हैं। चित्रकारों की तुलिका ने सरसों के फूलों को नए आकर्षक अंदाज़ दिए हैं। फिल्मकारों, छायाकारों, माडलों ने सरसों की नयनाभिराम प्राकृतिकता को अपने कार्यक्षेत्र की दिलकश पृष्ठभूमि बनाया है। सरसों के चिकित्सीय गुण भी कम नहीं हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस जैसे सभी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं।
सातवीं सदी के उतरार्द्ध में हुए संस्कृत कवि बाणभट्ट के कादंबरी व हर्षचरित ग्रंथों के सन्दर्भों से पता चलता है कि उस समय सरसों के छोटे.छोटे दानों का बड़ा महत्व था जीवन के हर क्षेत्र में। बच्चे की रक्षा के लिए उसके तालु पर देसी घी की दो बूंदों के साथ पीली सरसों में मिली भस्म लगाने, मस्तक पर सरसों रखने, बाणभट्ट द्वारा अपनी शिखा में सरसों रखने का उल्लेख है। आंवला सरसों के तेल में भिगोकर, इस मिश्रण को माथे पर रगड़ने से जलन, सिरदर्द, बालों का गिरना रूकता है। यहां तक माना जाता है कि सरसों के तेल की मालिश स्फूर्ति के साथ.साथ विचारों को भी संयमित करती है। सरसों का विविध उपयोग चिकित्सा, धार्मिक, मांगलिक व अन्य कार्यों में होता रहा है और आज भी हो रहा है। तांत्रिकों ने भी सरसों का प्रयोग किया है। सरसों की चर्चा असीम है, बिल्कुल जीवन की रसीली उमंग की तरह आखिर सरसों वसंतवाहिनी जो है।विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में तेजी के बीच बुधवार को दिल्ली थोक जिंस बाजार में इनमें उतार.चढ़ाव रहा। सरसों तेल के दाम करीब 1,100 रुपये और सोया तेल के 500 रुपये से अधिक चढ़ गये। अतीत पर नज़र डालें तो राज्य के पर्वतीय जिलों में कृषि आमदनी का पूरे तौर पर आमदनी का ज़रिया नहीं बन सका। राज्य में ज्यादातर छोटे किसान हैं जो सिर्फ 3.4 महीने का गुजारा करने भर अन्न उगाते रहे। हालांकि ऐसी घाटियां भी हैं जहां किसान पूरी तरह खेती पर आत्मनिर्भर भी रहे।
पिछले वर्ष अगस्त महीने में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की बदहाल खेती और किसानों के हालात पर चिंता जतायी थी। अदालत ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि योग्य ज़मीन के मात्र 20 फीसदी हिस्से पर ही खेती बची रह गई है। 80 प्रतिशत खेती की जमीन या तो बंजर हो गई है या उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया जा रहा है।राज्य में कृषि क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वर्ष 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तराखंड की स्थापना के समय कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेअर था, वर्ष 2019 तक ये घटकर 6.91 लाख हेक्टेअर रह गया है। राज्य में जोत का औसत आकार 0.89 हेक्टेअर है। केवल 50 फीसदी खेतों में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 13 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 94 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र की बजट में हिस्सेदारी औसतन 3.80 प्रतिशत से 3.63 प्रतिशत के बीच रहती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। वर्ष 2011.12 में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018.19 में 4.67 प्रतिशत के आसपास आ गई। कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र का राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 0.70 प्रतिशत रहा। सरकार का दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की मदद के लिए यह प्रयास सराहनीय है पर इस बारे में जनता को और अधिक जागरूक करने के उचित साधन ढूंढने की आवश्यकता है। कोरोना काल में अनेक ऐसे चित्र उभर कर सामने आए हैं जो दर्शाते हैं कि यह आपदा केवल आदमी के हिस्से की है, प्रकृति के लिए तो यह एक वरदान है। विगत दो महीनो से धरती पर अधिक हरियाली है, आसमान अधिक नीला है, सब जगह चिड़ियाएं चहक रही हैं, मोर छतों पर नाच रहे हैं, नदियां प्रदूषण मुक्त हो गई हैं, वन्यजीव उन्मुक्त सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे कितने ही मनोहर और अविश्वसनीय.से दृश्य हमारी आँखों के सामने आएं हैं। गांव के काश्तकार सब्जी उत्पादन के लिए सिर्फ गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। ताकि अधिक पैदावार के साथ ही लोगों को जैविक सब्जी का स्वाद मिल सके। कद्दू, तुरई, शिमला मिर्च, करेला, बीन, बैगन, लौकी के साथ.साथ सीजन में हरी सब्जियां, पालक, लाई, मेथी, बेथुवा, सरसों, मूली का इस गांव में काफी उत्पादन होता है। गांव के काश्तकार कहते हैं कि सब्जी उत्पादन में झिझक के बजाए ग्रामीण फख्र महसूस करते हैं। मेहनत के बल पर हर परिवार गुजारे लायक आजीविका कमा लेता है। यही कारण है कि गांव में यदि सरकारी विभाग ग्रामीणों को तकनीकी जानकारी, उन्नत प्रजाति के बीजए पॉलीहाउसए सिंचाई टैंक आदि सुविधाएं प्रदान करें तो को सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में मॉडल बनाया जा सकता है। कि गांव के सभी परिवार सामूहिक सब्जी उत्पादन करते हैं। शहर के पास होने से बिक्री की कोई समस्या भी नहीं है। सब्जी उत्पादन से हर परिवार आजीविका चला रहा है। सरकारी मदद मिले तो लोगों की आय बढ़ सकती है।
आयुर्वेद में भी सरसों की महत्ता का उल्लेख