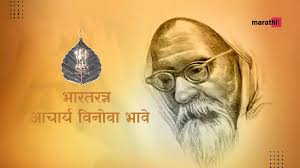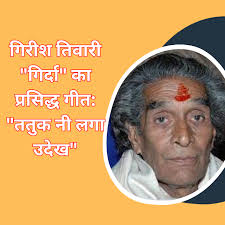डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
भूदान आंदोलन के प्रणेता, राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक
उत्तराधिकारी कहलाने वाले विलक्षण सत्यान्वेषी आचार्य विनोबा भावे के जीवन
में कर्म, ज्ञान और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम था कि बहुत से लोग उन्हें संसार
का आध्यात्मिक गुरु तो कहते ही हैं, संसारभर में समतामूलक और शोषणमुक्त
व्यवस्था का स्वप्नद्रष्टा भी मानते हैं. ‘जय जगत’ कहकर अभिवादन का उनका
आह्वान भी उनकी यही छवि गढ़ता है. वर्ष 1895 में, 11 सितंबर को महाराष्ट्र
के कोंकण क्षेत्र के गागोदा गांव के एक धर्मपरायण चितपावन ब्राह्मण परिवार में
उनका जन्म हुआ, तो शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक दिन उनके जीवन की
दिशा इतनी बदल जायेगी कि सत्य के अनुसंधान के लिए संन्यासी बनते-बनते वे
महात्मा गांधी के सान्निध्य में जाकर न सिर्फ अप्रतिम सत्याग्रही, बल्कि
सामुदायिक जीवन में लिप्त होकर उनके सत्य व अहिंसा के प्रयोगों के अभिन्न
सहचर हो जायेंगे. माता-पिता ने उनका नाम विनायक रखा था, जो उस वक्त की
परंपरा के अनुसार, उसमें पिता नरहरि भावे का नाम जुड़ने के बाद विनायक
नरहरि भावे हो गया था. परंतु माता रुक्मिणी बाई को उन्हें विन्या कहना ज्यादा
अच्छा लगता था. विनोबा नाम तो उन्हें बहुत बाद में महात्मा गांधी ने दिया,
जब वे उनके संपर्क में आये. इस संपर्क में आने की भी एक अनूठी कथा है. पच्चीस
मार्च, 1916 को जब वे इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे, तो उनकी संन्यासी
बनने की साध ने ऐसा जोर मारा कि सूरत में ट्रेन से उतरकर हिमालय की ओर
चल पड़े. परंतु जब काशी पहुंचे, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जलसे में
महात्मा गांधी को देखा तो राह बदल ली और उन्हीं के होकर रह गये. अनंतर,
अंग्रेजों द्वारा देश को जबरन दूसरे विश्वयुद्ध में धकेलने के विरुद्ध व्यक्तिगत
सत्याग्रह के महात्मा के आह्वान पर 17 अक्तूबर, 1940 को ‘प्रथम सत्याग्रही’
बने. आम तौर पर उन्हें उनकी विलक्षण स्मृति, विशद अध्ययन और तीन बड़ी
देश सेवाओं के लिए जाना जाता है. ये तीन सेवाएं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी,
भूदान आंदोलन के सूत्रधार और ‘सर्वोदय’ व ‘स्वराज’ के व्याख्याकार के रूप में
कीं. इसलिए उनके व्यक्तित्व की विराटता को प्रायः बड़े-बड़े प्रसंगों में ही देखा
जाता है, परंतु उसे छोटे-छोटे प्रसंगों में देखना भी कुछ कम प्रेरणादायक नहीं है.
एक बार महाराष्ट्र के पवनार स्थित आश्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल उत्तर
प्रदेश से गये रसोइये के ‘कच्ची रसोई’ या ‘पक्की रसोई’ के सवाल को ठीक से नहीं
समझ पाये, तो उन्होंने उन्हें समझाया था कि इस बहुभाषी-बहुधर्मी देश में
यात्राओं के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में जाने पर वहां की भाषाओं व बोलियों को
ठीक से सुनना व समझना बहुत जरूरी है. खास तौर पर सेवकों द्वारा अपने अंचल
की भाषा या बोली में पूछी गयी बात को ठीक से सुन-समझकर उत्तर देना.
अन्यथा नासमझी में अनर्थ तो हो ही जाता है, सेवाएं व स्नेह प्राप्त करने में भी
दिक्कतें आती हैं. इस प्रसंग में गौरतलब है कि अहिंदी भाषी होने के बावजूद
विनोबा कहा करते थे कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, पर
मेरे देश में हिंदी का सम्मान न हो, यह मुझसे सहन नहीं होता. वे देवनागरी की
भी विश्वलिपि जैसी प्रतिष्ठा चाहते थे. ‘भूदान यज्ञ’ के दौर में वे दिन में दो बार
प्रवचन करते और हर प्रवचन में नयी-नयी बातें कहते थे. एक दिन किसी ने उनसे
पूछ लिया कि लंबे समय से प्रवचन करते आने के बावजूद वे अपने प्रवचनों को
नीरस होने से कैसे बचाये हुए हैं, हर रोज उनमें नवीनता कैसे लाते हैं? इस पर
उनका उत्तर था- पैदल चलता हूं, तो धरती का स्पर्श होता और प्रकृति से निकट
का संबंध जुड़ता है. इससे मन को नित नयी स्फूर्ति तो मिलती ही है, नयी-नयी
बातें भी सूझती हैं.
सुरम्य शांति के लिए, जमीन दो, जमीन दो।
महान क्रांति के लिए, जमीन दो, जमीन दो।।
दुनिया में अपने तरीके के अनूठे गैर-सरकारी आंदोलन भूदान यज्ञ के पक्ष में ये पंक्तियां रामधारी सिंह
दिनकर ने लिखी थीं। आचार्य विनोबा भावे ने पचास के दशक में भूदान यज्ञ के नाम से जो आंदोलन आरंभ
किया था, वह कई मायनों में अनूठा था। इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसके द्वारा कुल 45.90
लाख एकड़ जमीन हासिल की गई थी। इस आंदोलन को लेकर तमाम रचनाकारों ने बहुत कुछ लिखा। विश्व
के तमाम बड़े नामी-गिरामी पत्रकारों ने भी इसे अपनी आंखों से देखा और हैरान हुए। आज आचार्य विनोबा
भावे का जन्म दिन है। 11 सितंबर, 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गांव गागोदा में विनोबा का
जन्म हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के रास्ते पर चले विनोबा भावे पूरे जीवनकाल में उन्हीं के
मार्ग पर चलते रहे और भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। लेकिन, बदलते समय के साथ जहां नई पीढ़ी भूमि
को लेकर बढ़ते सामाजिक तनाव को तो देख-समझ रही है, लेकिन भूदान आंदोलन धीरे-धीरे स्मृतियों से
बाहर होता जा रहा है।पोचमपल्ली में मिला नया विचार
विनोबा के जीवन के सबसे बड़े कामों में भूदान आंदोलन को माना जाता है। भूदान की भी कथा दिलचस्प
है। इसकी शुरूआत 18 अप्रैल, 1951 को आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावित पोचमपल्ली गांव से हुई, जो अब
तेलंगाना का हिस्सा है। यहीं पर जब विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला, तो उनकी सोच में बड़ा
बदलाव आया। उनको लगा कि जिस जमीन के लिए इतनी हिंसा, हत्या और मुकदमेबाजी होती है, वो
पोचमपल्ली में अगर दान में मिली है, तो ये काम वो देश भर में करके भूमिहीनों का कल्याण कर सकते हैं।
इसी के बाद, आचार्य विनोबा भावे ने पदयात्राएं शुरू कर दीं। उन्होंने गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से
अपनी भूमि का कम से कम छठवां हिस्सा भूदान के रूप में मांगा और भूमिहीन किसानों के बीच उसे बांटने
का अनुरोध करते रहे। भूदान आंदोलनएक मौन क्रांति
उन्होंने लक्ष्य बहुत बड़ा रखा था, 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का। इस आंदोलन में तमाम
नायक भी शामिल हुए, राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया। आरंभिक दौर में तेलंगाना इलाके में 200
गांवों में विनोबाजी ने दान में 12,200 एकड़ भूमि दान में हासिल की, तो सरकारी नजरिया भी बदला,
क्योंकि वह इलाका नक्सलवाद से प्रभावित था। इस आंदोलन के चलते 13 लाख भूमिहीन लोग भूस्वामी
बन सके और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। पर, इस आंदोलन की कुछ खामियां भी रहीं, जिसके
कारण मिली काफी भूमि का वितरण नहीं हो सका। कई राज्यों में मुकदमेंबाजी में फंसी भूमि और खेती के
लिए अनुपयुक्त भूमि भी मिली। राज्यों की दिलचस्पी और भूदान समितियों में गड़बड़ी जैसे मुद्दे भी सामने
आए, लेकिन इससे इस आंदोलन की सफलता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगता। इसे मौन क्रांति माना गया। एक
विख्यात लेखक एल्विन आर. फील्ड ने इसका आंखो देखा विवरण लिखते हुए कहा – "यदि मैं आपको बताऊं
कि आज संसार में एक ऐसी जगह है, जहां लोग भूमि देने के लिए कतार में खड़े होते हैं, तो आप क्या कहेंगे?
एक पेंसिल की तरह पतले आदमी ने, जिसका वजन 86 पौंड है, एशिया में एक प्रकार की क्रांति आरंभ की
है। उस एशिया में, जहां क्रांतियों से पहले ही रक्तपात हो रहा है।"दान में मिली
45.90 लाखएकड़भूमि आचार्य विनोबा भावे ने जमींदारों और अन्य लोंगों से 45.90 लाख एकड़ भूमि
दान में प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में भूदान यात्रा 1 अक्तूबर, 1951 को आरंभ हुई और 360 दिनों तक राज्य के
विभिन्न भागों में पहुंची। यहीं पर उनको देश में पहला ग्राम दान मगठौर (हमीरपुर) में मिला। पर, दुर्भाग्य
से इस गांव की 400 एकड़ जमीन खाली पड़ी रही। काफी जमीन भूमाफिया ने कब्जा कर ली। राजस्व
अधिकारियों की मिलीभगत से कई जगहों पर गड़बड़ी हुई। हालांकि, 1952 में उत्तर प्रदेश में देश का पहला
भूदान यज्ञ अधिनियम बनाकर जमीनों को दलित और भूमिहीन तबके में बांटने की प्रभावी पहल की गई।
उत्तर प्रदेश में भूदान की जमीनें 95,000 से अधिक गरीब परिवारों में बांटी गई, जिनमें अधिकतर दलित
थे। देश भर में ऐसे 13 लाख लोगों में भूदान की जमीनें बांटी गई। आज जबकि देश भर में भूमि संबंधी हिंसा
में लगातार वृद्धि हो रही है तो भूदान की महत्ता अधिक याद आती है। देश में भूमि पर दबाव बढ़ रहा है।
शहरीकरण, सड़कों, उद्योगों, आवासों आदि गैर-कृषि प्रयोजनों के कारण कृषि योग्य भूमि लगातार कम हो
रही है। खुद सरकारों के लिए भूमि अधिग्रहण मुश्किल होता जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से इतने
बड़े पैमाने पर भूमि हासिल किया जाना बड़ी बात थी। लेकिन, समय के साथ इस आंदोलन की गति मद्धिम
हुई, तो बहुत-सी कमजोरियां सामने आईं। काफी जमीनों का रिकॉर्ड ही गायब हो गया, या कर दिया गया।
पंजाब में हासिल की गई 5,000 एकड़ जमीन में मात्र एक हजार एकड़ बांटी जा सकी। बाकी दूसरों के
कब्जे में बनी रही। बिहार में 3.03 लाख दानपात्रों के माध्यम से हासिल हुई 21.18 लाख एकड़ जमीनों में
से 7.23 लाख एकड़ भूमि ही बांटी जा सकी। काफी जमीनें अवितरित ही रहीं।करीब 14 सालों तक चला
प्रयास भारत सरकार के स्तर पर 1991 में पहली बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री
पी.वी.नरसिंहराव ने भूदान की अवितरित सारी जमीनों को मार्च 1992 तक बांट देने का लक्ष्य रखा था।
पर, कई कारणों से यह संभव नहीं हो सका। फिर भी केरल, हरियाणा और असम जैसे प्रांतों में पूरा बंटवारा
हुआ। फिर भी चंद कमजोरियों से इस आंदोलन की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि
भूदान आंदोलन में विनोबाजी ने करीब 14 सालों तक प्रयास जारी रखा। भूमि राज्य सरकारों का विषय है,
लिहाजा भारत सरकार केवल समन्वय तथा सलाह-मशविरे तक सीमित रही।भूमि किसी भी आर्थिक
कार्यकलाप का प्राथमिक स्रोत होती है। संविधान की सातवीं अनुसूची में भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण राज्य
का विषय है। इससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्यों के विधान मंडलों के पास है। हर राज्य के भूमि
और इससे जुड़े मामलों के अलग विशिष्ट राजस्व कानून हैं। हाल के सालों में भूमि अभिलेखों के
कंप्यूटरीकरण तथा डिटिटलीकरण से नागरिकों को रियल टाइम भूमि अभिलेख मिलने लगा है। इन भू-
अभिलेखों से छेड़छाड़ नही हो सकती। हालांकि, आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी सरकार के पास यह
आंकड़ा नही है कि देश भर में कितने भूमिहीन किसानहैं। वर्ष 2001 की जनगणना में 10.67 करोड़
भूमिहीन कृषि श्रमिक थे। देश की कुल आबादी में कृषि कार्मिकों की भागीदारी करीब 22 प्रतिशत है। वर्ष
2011 की जनगणना में कृषि कार्मिकों की कुल संख्या 26.31 करोड थी, जिसमें से 11.88 करोड़ कृषक और
14.43 करोड़ कृषि श्रमिक शामिल थे। इस हिसाब से देखें, तो आज भी भूमिहानों की तस्वीर चिंताजनक ही
है। भूदान आंदोलन फिर चल सकेगा या नहीं, लेकिन भूमिहीनों को भूमि देने का मुद्दा अपनी जगह कायम
है। वे किसी भी काम की शुरुआत में देर न करने और शुरू करने के बाद उसे पूरा करके ही छोड़ने पर जोर
देते थे. कहते थे कि जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया. उनका
यह भी मानना था कि सच्चा बलवान वह है, जिसने अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हो.
प्रसंगवश, एक अपवाद को छोड़कर विनोबा अपने समूचे जीवन में कभी किसी विवाद में नहीं पडे़. उनके
जीवन की एकमात्र विडंबना यह है कि उन्होंने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा
नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर देश पर थोपी गयी इमरजेंसी को ‘अनुशासन पर्व’ बता दिया था.
उन्होंने 15 नवंबर, 1982 को अंतिम सांस ली. वर्ष 1958 में उन्हें पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया,
जबकि 1983 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से विभूषित किया गया
था. . *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत*
*हैं।*