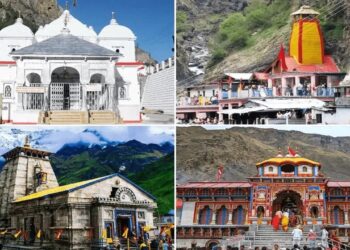डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
भारत के मुकुट के रूप में सुशोभित हिमालय देश का सीमा प्रहरी तो रहा ही है इसकी अलग गीता ने भी इसे दुनिया से अलग स्थान दिया है यह हमारी लापरवाही का नतीजा है कि अब इस को सीखने वाली नदियां सूख रही है वही पिघलते हिमखंड से कमजोर बना रहे हैं दरअसल हमने हिमालय को समझने में पहाड़ जैसी चुक की हैं और यह हमारी नीतियों में भी स्पष्ट दिखाई देता है जिसे अब आगे चलकर के सवारना होगा नहीं तो यह हिमालय हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकेगा।दरअसल हिमालय से मात्र जनजीवन ही नहीं जुड़ा है बल्कि देश की अस्मिता भी जुड़ी है हिमालय की महिमा कुछ इस तरह की है कि मात्र स्थानीय लोगों की आवश्यकता है कि ही भरपाई नहीं करता बल्कि देश का एक बड़ा भूभाग इसी की कृपा से पनपा है मोटे रूप में देश के साथ मैदानी राज्यों की खेती बाड़ी प्राकृतिक पर्यावरण हिमालय की देन है इसमें देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल जैसे राज्य आते हैं हिमालय की गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सतना जैसी नदियों ने इस देश के भूगोल को तय किया है साथ में संपन्नता का आधार भी बनी है इतना ही नहीं हिमालय में होने वाली कोई भी हलचल दुनिया के 18 देशों और 2 अरब लोगों को सीधा प्रभावित करतीहै। पहाड़ों की चोटियों ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पहले से कही अधिक महसूस किया और ये तेजी से गर्म हो गए। फिर भी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर एक अधिक ऊंचाई वाले जलवायु स्टेशन में एक अप्रत्याशित घटना देखी गई, जहां सतही हवा का तापमान औसतन बढ़ने के बजाय स्थिर रहा।पिरामिड इंटरनेशनल लेबोरेटरी या ऑब्जर्वेटरी क्लाइमेट स्टेशन, माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी ढलानों पर खुम्बू और लोबुचे ग्लेशियरों के 5,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसने लगभग तीन दशकों से लगातार प्रति घंटा मौसम संबंधी आंकड़े दर्ज किए हैं।गर्म होती जलवायु ग्लेशियरों में शीतलन प्रतिक्रिया को बढ़ा रही है, यह ढलानों से नीचे बहने वाली ठंडी हवाओं जिन्हें कटाबेटिक हवाएं कहा जाता है, उन्हें जन्म दे रही हैं। लेकिन ग्लेशियर कब तक स्थानीय स्तर पर खुद को ठंडा करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं? और कौन सी विशेषताएं ग्लेशियरों को ऐसा करने में मदद करते हैं? देखी गई घटना को समझाने के लिए, टीम ने आंकड़ों की बारीकी से जांच की। शोधकर्ता कहते हैं, हमने पाया कि कुल तापमान का औसत एक साधारण कारण से स्थिर लग रहा था। जबकि न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मियों में सतह का अधिकतम तापमान लगातार गिर रहा था। सतह के साथ अपने तापमान के आदान-प्रदान को बढ़ाकर गर्म होती जलवायु पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के ऊपर गर्म वातावरणीय हवा और ग्लेशियर की सतह के सीधे संपर्क में आने वाली हवा के बीच तापमान में अंतर बढ़ जाता है।शोधकर्ता ने बताया कि, इससे ग्लेशियर की सतह पर तापमान में वृद्धि होती है और सतह के वायु द्रव्यमान में ठंडक बढ़ जाती है। जिसके कारण, ठंडी और शुष्क सतह की हवा सघन हो जाती है और ढलानों से नीचे घाटियों में बहती है, जिससे ग्लेशियरों के निचले हिस्से और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र ठंडे हो जाते हैं।पिरामिड में विशिष्ट रूप से उपलब्ध जमीनी अवलोकनों से आगे बढ़कर, टीम ने जलवायु मॉडल में नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति को जोड़ा, वैश्विक जलवायु और मौसम पुनर्विश्लेषण जिसे ईआरए5-लैंड कहा जाता है। ईआरए5-लैंड पुनर्विश्लेषण भौतिकी के नियमों का उपयोग करके मॉडल आंकड़ों को दुनिया भर के अवलोकनों के साथ पूर्ण और सही डेटासेट में जोड़ता है। इन आंकड़ों की व्याख्या करने से टीम को यह प्रदर्शित करने में मदद मिली कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित काटाबेटिक हवाएं न केवल माउंट एवरेस्ट पर बल्कि पूरे हिमालयी इलाके में बन रही हैं।शोधकर्ता ने कहा, यह घटना 30 वर्षों के लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान का परिणाम है। अगला कदम यह पता लगाना है कि ग्लेशियर की कौन सी प्रमुख विशेषताएं ऐसी प्रतिक्रिया का पक्ष लेती हैं।इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग पर इस तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और कितने समय तक यह जारी रहता है। जबकि अन्य ग्लेशियर भारी बदलावों का अनुभव कर रहे हैं, एशिया के ऊंचे पहाड़ों में थर्ड पोल में ग्लेशियर बहुत बड़े हैं, जिनमें विशाल मात्रा में बर्फ हैं, और इनका प्रतिक्रिया करने का समय लंबा है। इस तरह, हमारे पास अभी भी ग्लेशियर को बचाने का मौका है।पामीर और काराकोरम ग्लेशियरों की ढलानें आम तौर पर हिमालय की तुलना में सपाट हैं। इस प्रकार, अनुमान लगाया जा सकता है कि ठंडी हवाएं आसपास के वातावरण में नीचे तक पहुंचने के बजाय ग्लेशियरों को स्वयं ठंडा करने का काम कर सकती हैं।शोधकर्ता ने कहा कि, काटाबेटिक हवाएं दुनिया भर में बढ़ते तापमान के लिए स्वस्थ ग्लेशियरों की प्रतिक्रिया है और यह घटना पर्माफ्रॉस्ट और आसपास की वनस्पति को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। ग्लेशियर वास्तव में अपने पारिस्थितिकी तंत्र में जल सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन स्वस्थ ग्लेशियर कब तक लड़ सकते हैं?भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रीष्मकालीन मॉनसून के दौरान बहुत ऊंचाई पर बर्फ जमा करते हैं और साथ ही, लगातार पिघलने से भारी मात्रा में बर्फ खो देते हैं। हालांकि, काटाबेटिक हवाएं अब इस संतुलन को बदल रही हैं, ग्लेशियरों से नीचे बहने वाली ठंडी हवाएं उस ऊंचाई को कम कर रही हैं जहां बारिश होती है।इससे ग्लेशियरों के पिघलने के दौरान भारी मात्रा में बर्फ गायब हो जाती है। इस तरह, ग्लेशियरों से बहने वाला कथित ठंडा तापमान ग्लेशियर को लंबे समय तक स्थिर रहने बजाय यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रति एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है। इसका मतलब यह है कि क्या ग्लेशियर अपने संरक्षण के चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं? वे कुछ जगहों पर हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कहां और कैसे।भले ही ग्लेशियर खुद को हमेशा के लिए संरक्षित नहीं कर सकते, फिर भी वे कुछ समय के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार, हम प्रभावों को समझाने की दिशा में प्रयासों को एकजुट करने के लिए अधिक शोधों की जरूरत हैं। ये प्रयास मानवजनित जलवायु परिवर्तन की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।बढ़ती गर्मी के कारण हिमालय के हिमखंड आप जिलों में परिवर्तित हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एक अध्ययन के अनुसार इन पिघलते हिम खंडों के कारण मिथेन गैस का उत्सर्जन भी हो रहा है मतलब एक साथ दो तरह की परिस्थितियों की मार हम सब पर पड़ने वाली है इन खंडों के पिघलने से जहां हम पानी का फिक्स डिपाजिट खो देंगे वही समुद्र का व्यवहार बदल जाएंगे। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड से 4 गुना घातक मिथेन जैसी गैस से वायु में बढ़ते घनत्व के कारण तापमान में वृद्धि निश्चित है इस परिवर्तन के पीछे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग रहा है यह भी स्पष्ट है कि दुनिया में बढ़ती तपन के कारण क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े दुष्परिणाम सामने आए हैं यह बदलाव का पहला असर हिमालय में ही झलकता है यही कारण है कि लगातार कुछ समय से हिमालय कई तरह से मुसीबतों से घिरा हुआ है गर्मियों में जहां इसे वनों की आग मिलती है वही मानसून में अतिवृष्टि यहां जीवन को छिन्न-भिन्न कर देती है हर वर्ष की यह घटनाएं हिमालय को पीछे धकेल देती हैं।हिमालय के प्रति एक नई नीति की पहल होनी चाहिए मातराजो में हिमालय को बांट कर हम आज तक कोई संरक्षण नहीं कर सके सच तो यह है कि पिछले 100 साल से हिमालय में होने वाले बदलाव हमारे संज्ञान में ही नहीं है और ना ही उसका कोई लेखा-जोखा हमारे पास है अगर ऐसा कोई अध्ययन होता तो शायद हम सफर को पाते और आने वाली समस्या से हिमालय की सुरक्षा पर व्यवहारिक कदम उठाते हिमालय को राज्य का दर्जा दिया जाना मात्र इसका समाधान नहीं है बल्कि हिमालय की नीतियां और ढांचा कुछ अलग होने की आवश्यकता है इस की परिस्थिति को समझते हुए यहां के विकास के ढांचे के प्रति गंभीरता दिखाना सबसे बड़ी आवश्यकता है इसके बावजूद हिमालय हमारे साथ है और किसी न किसी रूप में अनवरत सेवा में जुटा हुआ है।अभी भी हिमालय देश दुनिया की सेवा में उस निम्न स्तर पर नहीं पहुंचा जिसे हम दूर नहीं कर सकते लेकिन यह भी यह शिकार नहीं कर सकते कि हिमालय आज वैसा स्थिर नहीं है जैसा अपने जन्म के समय में था यह सारे देश की विरासत है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय के लिए अलग से सोच पर तब शायद हम हिमालय के प्रतिनिधियों को स्थान दे पाएंगे जिनसे संरक्षण जुड़ा है इसके लिए हम हिमालय में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण पर चिंतन करते हुए हिमालय के संरक्षण के प्रति चिंता करें इसी सोच के चलते वह इसके महत्व और संरक्षण पर चर्चा के लिए हिमालय दिवस की कल्पना की गई थी तब से लगातार हर वर्ष हिमालय को लेकर चिंतन की एक श्रृंखला देशभर को संदेश लेने का ऐस प्रयत्न कर रहा है जिसमें सभी भागीदारी आवश्यक है। हिमालय को नमन करने का मतलब प्रभु व प्रकृति के प्रति आदर प्रकट करने जैसा होगा। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*