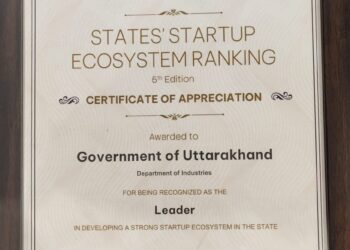शंकर सिंह भाटिया
मेरा पहाड़ पूरी तरह बदल गया है। पहाड़ में अपनी संस्कृति और बोली भाषा को छोड़ने की होड़ मची हुई है। पहाड़ की संस्कृति परंपराओं को दूसरी संस्कृतियों ने अपने ही पहाड़ में चलन से बाहर कर दिया है। इसकी भनक मुझे इतनी देर से लगी है, इससे रूबरू होकर मैं हैरान हूं। इसके लिए मेरे जैसे वे तमाम लोग कितने जिम्मेदार हैं, जो पहाड़ छोड़कर पहाड़ से पलायन कर गए हैं? और जो पहाड़ में रहकर भी अपनी संस्कृति को छोटा मानकर उसे छोड़ रहे हैं और बड़ा दिखने के लिए के लिए दूसरों की संस्कृति को गले लगा रहे हैं?
मैं अखबार की नौकरी में था, जिसमें अधिक छुट्टियां नहीं मिलती, इसलिए 20-25 साल से अपने छोटे चचेरे भाई बहनों की शादी में नहीं शामिल हो पाया। अब भतीजे-भतीजियों की शादी का वक्त आ गया है। नौकरी से बाहर होने के बाद तसल्ली से इन शादियों में शामिल हुआ जा सकता है। इसी कड़ी में अपने जुड़वां भतीजों कुलदेव-बदलेव की शादी में गांव जाना हुआ। मैं बड़े अरमान लेकर पहाड़ गया था।
पहाड़ की जिस परंपरा को हमने देखा है और बचपन से युवा होने तक उसे भोगा है, उस सामुहिक भोज के पहाड़ी अंदाज को मैं ढूंढता ही रह गया। यह अंदाज इतना निराला है कि एक पंडितजी या गांव का ही कोई जानकार आदमी अकेले एक हजार लोगों की रसोई तैयार कर लेता है। बस उसे रसोई के बाहर कुछ सहायकों की जरूरत होती है। जो जरूरत के अनुसार उसे रसद पहुंचाते रहते हैं। खाने की कोई बहुत वैराइटी नहीं, लेकिन फिर भी खाने वालों के लिए उससे लजीज कोई भोजन नहीं हो सकता। इस परंपरागत सामूहिक भोज में भात बनता है, जो तांबे के परंपरागत कूड़ों (बड़े वर्तनों) में तैयार होता है। इन्हीं तांबे के कूड़ों में लजीज गाड़ी दाल बनती है, जिसके स्वाद के लिए तरसते हुए मैं पहाड़ पहुंचा था। लोहे की बड़े भदेलों (कड़ाइयों) में पापड़ा (गागली) का साग। इसके अलावा रायता और चटनी। भोजन लौर (पंगत) में बैठकर करना है। एक लौर एक साथ खाना प्रारंभ करेगा, एक साथ खाकर उठेगा। उसके बाद अगला लौर बैठेगा। यह क्रम लगातार जारी रहेगा, जब तक सब लोग न खा लें। रसोई बनाने वाले पंडितजी को मनचाही दक्षिणा देकर खाना बनाने के इस काम को बहुत सस्ते में पूरा किया जाता रहा है।
अब इसकी जगह स्टेंडिंग अंग्रेजियत पैटर्न ने ले ली है। टेबल पर बफर में खाना रखा हुआ है। लोग खाने पर टूट पड़ रहे हैं। इस खाने में वैराइटी काफी ज्यादा हो सकती हैं। चावल, जीरा राइस, पलाव, पनीर की सब्जी, मिक्स वैज, छोले, पूरी और न जाने क्या-क्या। ये सारे मशालेदार आइटम हैं। यदि बच गया तो जानवर भी इसे खाने को तैयार नहीं। यदि जानवरों ने खा लिया तो उनका बीमार होना तय है। यदि हमारे खाने को जानवर भी नहीं पचा पा रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, हम पानी की तरह पैसा बहाकर कैसा खाना खा रहे हैं? लेकिन इस तरफ सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। सभी आधुनिकता की इस होड़ में बहते चले जाना चाहते हैं। कहीं कोई उन पर अंगुली न उठाए कि वह आधुनिकता के साथ नहीं चल पाए हैं।
पलायन कर तराई, हल्द्वानी, देहरादून तथा दूसरे शहरों में आ गए पहाड़ के लोग जब अपनी संस्कृति भूल गए हैं, वे अपने बच्चों की शादी इसी तरह आधुनिक बनकर कर रहे हैं तो पहाड़ में रह रहे लोगों से हम उन्हीं परंपराओं को ढोते रहने की अपेक्षा कैसे कर सकत हैं? इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक बनने की इस होड़ में सरपट आगे बढ़ते जाने के बजाय यदि हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो असलियत सामने आ जाती है।
बात यहीं तक नहीं है, बारात में पुरुषों से अधिक संख्या में औरतों का जाना और नगाड़े की थाप पर फुदक-फुदक कर नाचना, यह भी पलायन की संस्कृति से ही पहाड़ों तक पहुंचा है। एक दौर था, जब हमारे समाज में बारात में औरतों का जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। माना जाता था कि बारात में औरत सिर्फ या तो दासी के रूप में जा सकती है या फिर नाचने वाली हुड़क्यानी के रूप में जा सकती है। हमारी संस्कृति औरतों को खुलकर नाचने का अवसर भी देती है। जब पुरूष बारात में चले जाते थे तब रतेली में महिलाएं स्वच्छंद होकर नाचती गाती थी। अब शायद यह अवसर भी महिलाओं को नहीं मिलता क्योंकि बारात दो दिवसीय होने के बजाय एक दिवसीय होने लगी है।
दोर बरात पहाड़ की बारात की संस्कृति का सबसे रोचक पक्ष होता था। जब वर पक्ष तथा बधू पक्ष दोनों तरफ के नगाड़े दुल्हन के घर के आंगन में नगाड़ों का रोचक प्रदर्शन करते थे। अब इन परंपरागत ढोल नगाड़ों की जगह डीजे को प्राथमिकता दी जा रही है। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची तो मैं दुल्हन के पक्ष के नगाड़ों की अपेक्षा कर रहा था, जिसकी जगह पर वहां डीजे बज रहा था। बारात का स्वागत कन्याएं कलश में पानी लेकर तो कर रही थी, लेकिन गेट पर बंधा लाल रीबन कटने के इंतजार में था।
मैंने जब भाई से शादी से पहले यहां की व्यवस्थाओं पर बात की तो, उसका कहना था कि जिस राह पर पूरा समाज चल पड़ा है, उसी पर मुझे भी चलना है। यदि मैं परंपरा के नाम पर इन्हें नहीं मानूंगा तो समाज की आलोचना झेलनी पड़ेगी। संभव है कि बच्चे भी इसके लिए तैयार न हों।
हमारे पास सामूहिक भोज का एक विकल्प था, एक पंडित सबके लिए खाना बना सकता था, बहुत सस्ते में निपटने वाली इस व्यवस्था के स्थान पर हम खाना बनाने वालों को 20-25 हजार से अधिक का भुगतान कर रहे हैं। महंगी अखाद्य जीनस पर खर्च होने वाला पैसे अलग है। खाने की जीनस की जो बर्बादी ये खाना बनाने वाले करते हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
कुल मिलाकर हमने पाया कि पहाड़ की एक सीधी साधी संस्कृति पर कठमाली और पंजाबी संस्कृति पूरी तरह हावी हो गई है। वह चाहे व्याह शादी का मामला हो या फिर दूसरी परंपराएं हों। दुखद यह है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कालातीत हो गई हैं। दूसरी संस्कृतियों ने आकर उन्हें चलन से बाहर कर दिया है।
इतना ही नहीं इस दौरे में मुझे एक और झकझोर देने वाली बात से दो चार होना पड़ा। हालांकि इस पर मैं पहले भी लिख चुका हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि कुछ सालों बाद पहाड़ में भी पहाड़ी बोली-भाषा बोलने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आज के जो किशोर हैं, वे चाहे सरकारी स्कूल में पड़ रहे हैं या फिर पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई भी अपनी भाषा नहीं बोलता। जब ये बड़े होंगे तो इस समाज में पहाड़ी बोलने वाला कोई नहीं होगा। इसके लिए आधुनिक बनने की होड़ सबसे अधिक जिम्मेदार है। एक वह दौर था जब माताएं अपने बच्चे से ईजा कहलाने के बजाय मम्मी कहलाना अधिक पसंद करती थी। जब बच्चा ईजा कहता तो मां उसे डपट देती थी और मम्मी कहने को मजबूर कर देती थी। आज ठीक उसी तरह मम्मी चाहती है कि उसका बच्चा हिंदी में बोले, अपनी भाषा में बोलना हीन भावना की निशानी है। इसके पदचिन्ह भी बहुत पहले पड़ गए थे। पहले जब पहाड़ अपनी बोली भाषा और संस्कृति के साथ खड़ा था, तब शहरों तथा कस्बों में रहने वाले लोग आधुनिक दिखने की होड़ में अपनी संस्कृति बोली भाषा को छोड़ कथित मार्डन होने की तरफ बढ़ रहे थे। अब यह मार्डन बनने की होड़ गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गई है। अपनी संस्कृति से हटना, अपनी बोली भाषा न बोलना, अब पहाड़ में आधुनिकता हो गई है। अपनी जड़ों से खुद कट जाने की यह होड़ इस पहाड़ को कहां तक ले जाएगी, सोचकर ही डर लगता है।