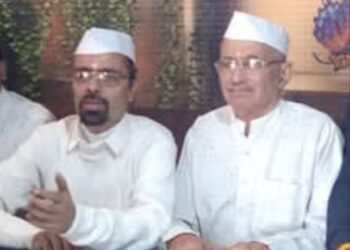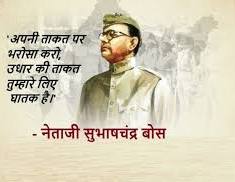. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शादी समारोह से लेकर अंतिम संस्कार, पूजा पाठ, पांडव नृत्य
के अवसर पर बजाए जाने वाले ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों की आवाज तो आपने जरूर सुनीं
होगी. जिसकी थाप पर लोक जमकर नृत्य करते दिखाई देते हैं. लेकिन सरकार की बेरूखी के
कारण अब ढोल दमाऊ बजाने का हुनर रखने वाले कलाकारों के आगे रोजी-रोटी का संकट
गहरा रहा है. यही कारण है कि अब ढोल दमाऊ बजाने वाले कलाकार इस पेशे से मुंह मोड़
रहे हैं.अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के वाद्य-यंत्रों की बात करें तो उनमें मुख्य है 'ढोल-दमाऊं,
मशकबाजा'. यह वाद्य यंत्र पहाड़ी समाज की लोककला को संजोए हुए हैं. इस कला का जन्म
से लेकर मृत्यु तक, घर से जंगल तक प्रत्येक संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में इनका
प्रयोग होता आ रहा है. इनकी थाप के बिना यहां का कोई भी शुभकार्य पूरा नहीं माना
जाता है. इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर मनाए जाने वाले त्योहारों की शुरुआत ढोल-
दमाऊं की धुन से ही होती है. ढोल-दमाऊ को प्रमुख वाद्य यंत्रों में इसलिए शामिल किया
गया, क्योंकि इनके माध्यम से ही देवी-देवताओं का आह्ववान किया जाता है. दंतकथाओं के
अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है, जिसे
सर्वप्रथम भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था. वहां मौजूद एक गण ने इन्हें सुनकर
याद कर लिया. माना जाता है तब से लेकर आज तक यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ
रही है, जिनमें हर कार्यक्रम के लिए विशेष धुनों का प्रयोग किया जाता है. ढोल-दमाऊ
वादक को कई नामों से भी जाना जाता है. वहीं प्रत्येक भारतीय महीने के प्रारम्भ में ढोल
वादक गांवों के प्रत्येक घर में यह वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिससे वह यह सूचना देते हैं कि
भारतीय वर्ष का नया महीना प्रारम्भ हो गया है. आजकल की दुनिया आधुनिक होती जा
रही है. शादी व पार्टी आदि में डीजे अथवा बैंड प्रयोग होने लगा है, लेकिन उत्तराखंड की
संस्कृति में आज भी लोग ढोल-दमाऊ का ही प्रयोग करते हैं और इसके ताल का आनन्द लेकर
नृत्य करते हैं. देवभूमि उत्तराखंड में करोड़ों देवी-देवताओं का निवास स्थान माना गया है.
यहां, प्रचलित कथाओं में दमाऊ को भगवान शिव का और ढोल को ऊर्जा का स्वरूप माना
जाता है. ऊर्जा के अंदर शक्ति विद्यमान में यानी ढोल और दमाऊ का रिश्ता शिव-शक्ति जैसा
माना गया है. उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति में विभिन्न अवसरों पर ताल और सुर
में ढोल और दमाऊ का वादन किया जाता है. आज उत्तराखंड की पर्वतीय संस्कृति पर
पाश्चात्य देशों की संस्कृति का खासा असर पड़ा है. इसलिए आधुनिकता के दौर में पहाड़ के
ही अधिकतर लोग ढोल-दमाऊ को भूलते जा रहे हैं और नई पीढ़ी इसे बजाना नहीं चाहती
है. ढोल-दमाऊ के हुनरबाज इस कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर न के बराबर होने की
वजह से खासे परेशान हैं और इसलिए इन हुनरबाजों की अगली पीढ़ी ढोल-दमाऊ की कला
को अपनाने को तैयार नहीं है.ढोल दमाऊ का उत्तराखंड की संस्कृति से गहरा रिश्ता रहा है.
वर्तमान मे उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के अन्य पौराणिक वाद्ययंत्र अंतिम चरण की सांस लेते
नजर आ रहे हैं। उक्त वाद्ययंत्रों को बनाने वाले कुशल कारीगरों व बजाने वाले सिद्धहस्त
वादकों की संख्या सिमट सी गई है। वर्तमान दौर में उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक गीत-संगीत
व मनोरंजन के आयोजनों मे हर वो आधुनिक वाद्ययंत्र उपयोग में लाये जा रहे हैं जो देश या
विदेश में संगीत के क्षेत्र में उपयोग किए जा रहे हैं।उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के लुप्तप्राय
पौराणिक वाद्ययंत्रों में बांस या मोटा रिंगाल से निर्मित ’अल्गोजा’ (जोया मुरली) जो
लोकगीतों खुदेड अथवा झुमैला गीतों तथा पशुचारकों द्वारा बजाया जाता था लगभग लुप्त
हो चुका है। धातु निर्मित छोटा सा वाद्ययंत्र ’बिणाई’ जो अधिकतर पर्वतीय अंचल की
महिलाओं द्वारा बखूबी बजाया जाता था, विभिन्न तालां में विभिन्न स्वरों के लिए अलग-
अलग प्रकार की ’बिणाई’ ताल स्वरां वाली बनाई जाती थी। यह वाद्ययंत्र अब लुप्तप्राय है।
हुड़का’ उत्तराखंड के लोकगीत व जागर गायन दोनों में प्रयुक्त होने के साथ-साथ कृषि कार्यो
तथा युद्ध प्रेरक प्रसंगों में बजाया जाने वाला लोक वाद्ययंत्र रहा है। इस वाद्य को बनाने वाले
कुशल कारीगरों तथा बजाने वाले निपुण वादकों के अभाव में, वाद्ययंत्र से प्रकट होने वाली
कर्णप्रिय गूंज के लुप्त होने से इस सु-विख्यात लोक वाद्ययंत्र ने अपना अस्तित्व खो दिया है,
जिस कारण यह लोक वाद्ययंत्र विलुप्ति की कगार पर खड़ा है।शिव को समर्पित, चार मोड
वाला व आगे का हिस्सा सांप के मुह की तरह दिखने वाला, डेढ़ मीटर लंबा पौराणिक लोक
वाद्ययन्त्र ’नागफणी’ जिसे अंचल के तांत्रिकों, साधुआें द्वारा तथा युद्ध के समय सेना में
जोश भरने, धार्मिक, सामाजिक, शादी-व्याह व मेहमानों के स्वागत समारोहों में फूक
मारकर बजाया जाता था, लगभग लुप्त हो चुका है।पर्वतीय अंचल में लोक आस्था के प्रतीक
जागर में स्थानीय देवताओं को नचाने में ’डौरू’ या ’डौर’ वाद्ययंत्र जिसकी संरचना दोनों
तरफ से समांतर, बीच में मोटाई थोडी कम होती है, वादक द्वारा जांघ के नीचे रख कर
बजाता है, विलुप्ति की कगार पर खड़ा है।बाजार भाव, सरलता व वादन की दृष्टि से अगर
आधुनिक व पौराणिक वाद्ययंत्रों का तुलनात्मक रूप से अवलोकन करते हैं तो एक
इलैक्ट्रोनिक वाद्ययंत्र जो पौराणिक वाद्ययंत्रों से भार की तुलना में हल्का, लाने ले जाने व
वादन में सरल तथा कीमत की तुलना में बीस-इक्कीस का ही आंकड़ा रखता नजर आता है।
इलैक्ट्रोनिक वाद्ययंत्र का सबसे बड़ा फायदा नजर आता है, एक वादक एक ही यंत्र से कई
वाद्यों की धुन निकाल सकता है। आधुनिक वाद्ययंत्रों की सुगमता व बहुलता ही वह कारण
माना जा सकता है जिस बल प्राचीन व पौराणिक वाद्ययंत्रों का अस्तित्व समाप्त हुआ है या
समाप्ति की कगार पर है।
लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के जनमानस का प्राचीन काल से पीढी दर पीढी
विश्वास रहा है, अंचल में प्रचलित पौराणिक वाद्ययंत्र दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत रहे हैं।
वाद्य व वादक साधारण नहीं असाधारण रहे हैं। जहां भी इन वाद्ययंत्रों का वादन सिद्धहस्त
वादकों द्वारा किया गया, वाद्यों की ध्वनि से उक्त स्थान व वहां के जन में सकारात्मक्ता का
वास हुआ है।नकारात्मक जन नाचते देखे गए हैं। सिद्धहस्त वादकां द्वारा वाद्ययंत्रों का वादन
कर समय-समय पर जन को जगा सकारात्मक्ता की राह दिखाई गई है। देवभूमि उत्तराखंड में
देवताआें का आहवान पारंपरिक तौर पर पौराणिक वाद्ययंत्रों के द्वारा ही किया जाता रहा
है, जो आज विलुप्ति की कगार पर खडे हैं।वर्तमान में उत्तराखंड की जो दशा व दिशा
चलायमान है। अनेकों प्रकार की भयावह विपदाओं से जो हा हा कार मचा हुआ है। दिव्य
पौराणिक वाद्ययंत्रों के संरक्षण की पहल को नजरअंदाज करने से उन वाद्यों पर जो विलुप्ति
का खतरा मंडरा रहा है, इसे देवभूमि उत्तराखंड के परिपेक्ष मे सकुन कहे या अपसकुन?
समझा जा सकता है।
देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति के वाहक रहे पौराणिक वाद्ययंत्रों को लुप्त होने से बचाने के
लिए अंचल वासियां को चाहिए वे दिव्य वाद्ययंत्रों के संरक्षण व संवर्धन हेतु आगे आए।
निपुण वादक देवभूमि के पौराणिक वाद्ययंत्रों का विधि-विधान से वादन कर उनकी ध्वनि से
उत्तराखंड में व्याप्त नकारात्मक्ता को दूर कर, देवभूमि उत्तराखंड के जनमानस के सामाजिक
व सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने की प्रभावी पहल करें।आज की पीढी इस वाद्ययंत्र के बावत
अंजान रही है। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और पुरुषों के सजने के बाद अगर ढोल
दमाऊ की थाप न मिले तो उनका श्रृंगार अधूरा कहा जाता है. आज भी उत्तराखंड के
सुदूरवर्ती क्षेत्रों में होने वाले विवाह व अन्य कार्यक्रमों में ढोल दमाऊ की थाप सुनीं जा
सकती है. हालांकि, धीरे-धीरे ढोल दमाऊ का काम करने वाले कलाकारों का इस पेशे से मोह
भंग होता जा रहा है. आज सरकार को इस लोक संस्कृति के बचाए रखने के लिए और
कलाकारों के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है. भारत सरकार,
भारतीय ज्ञान और परंपरा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को
अपने भारतीय ज्ञान और परंपरा की जानकारी हो. यही वजह है कि साल 2020 में लागू हुई
नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान और परंपरा पर विशेष जोर दिया गया है. इसके साथ ही
बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज कोर्स की शुरुआत भी की गई,
ताकि भारतीय ज्ञान और भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस पर शोध और अध्ययन
किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी दून यूनिवर्सिटी में एमए इन हिंदू स्टडीज
कोर्स को इस शैक्षिक सत्र से शुरू करने जा रही है, ताकि भारतीय ज्ञान परंपराओं के साथ ही
उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को विस्तार से समझा और समझाया जा सके. *लेखक*
*विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*