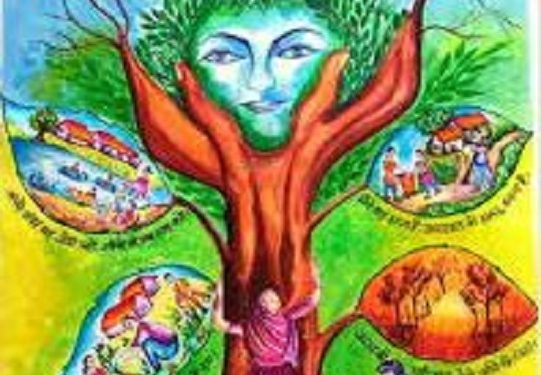डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
चीन के बाद भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और वैश्विक स्तर पर चल रहे पर्यावरण संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अगले एक दशक में इकोसिस्टम रीस्टोरेशन में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर पर्यावरणविद वेंकेटेश दत्त ने दिप्रिंट से कहा, भारत ने अपना पोजिशन स्पष्ट किया हुआ है। हमारा कार्बन फुटप्रिंट अन्य दूसरे विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। भारत का पर कैपिटा एमिशन भी काफी कम है। प्रतिष्ठित पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को हमारे बीच से गए हुए अभी करीब 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान पर्यावरण से जुड़े कई गंभीर मुद्दे एक बार फिर हमारे सामने सवाल उठाने लगे हैं। बहुगुणा की मृत्यु से कुछ दिन पहले ही भारत के कई राज्यों को अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते की मार झेलनी पड़ी और उनके जाने के चंद रोज़ बाद ही बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का भी सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरब सागर में ज्यादा तूफान बन रहे हैं।
हवा, पानी, मिट्टी और जंगल हमारे जीवन के मुख्य आधार हैं। इन्हें नुकसान भी लोगों ने ही पहुंचाया है और इसके संरक्षण के लिए भी लोग ही संघर्ष कर रहे हैं। पर्यावरण का सीधा संबंध लोगों से है, उनके अधिकारों और शांति से है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी पैरिस जलवायु समझौते से लेकर अतीत में स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रयास किए गए। स्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम इकोसिस्टम रीस्टोरेशन पर बात करें। सस्टेनेबल डेवलेपमेंट के तहत संयुक्त राष्ट्र ने 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसे 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक संकट के जो कारण हैं, वो इकोलॉजी संकट से जुड़े हुए हैं। आर्थिक विकास का फाउंडेशन इकोलॉजी में ही है।
पर्यावरण को मूलभूत मानवाधिकर के तौर पर विश्व के कई देशों ने अपने संविधान में जगह दी है। बीते कई दशकों में अदालतों ने भी अपने फैसलों में इसे संवैधानिक अधिकार के तौर पर दर्ज किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों ने पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी है, वहां पर्यावरण के सूचकांक बेहतर हुए हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले में डच सुप्रीम कोर्ट ने उरगेंडा फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ नीदरलैंड्स में डच सरकार को फटकार लगाते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने और वैश्विक तौर पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने को कहा था। लेकिन विडंबना है कि जब विश्व के कई देशों ने पर्यावरण को एक अधिकार के तौर पर जगह दी है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने इसे अब तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने वाले स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के जब 2022 में 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो पर्यावरण को एक अधिकार के तौर पर मान्यता दे। कोरोना महामारी के कारण हुए बदलावों का असर पर्यावरण पर भी पड़ा है। इस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर के देश प्रभावित हुए और कई मुल्कों में लगे लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव, दोनों होता दिखा। इस दौरान देखा गया कि वायु की गुणवत्ता, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में काफी कमी आई है।
भारत में गंगा नदी इसका उदाहरण है, जिसमें देखा गया कि कई जगहों पर इसका जल स्तर बढ़ा और उद्योगों का गंदा पानी न जाने के कारण पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, लेकिन महामारी ने कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिए हैं। इस बीच मेडिकल वेस्ट के डिस्पोसल की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में प्रकृति कुछ हद तक रीस्टार्ट हुई है और इस दौरान हमें सबक मिला है कि पर्यावरण को खुश रखे बिना हम अर्थव्यवस्था को खुशहाल नहीं रख सकते। अर्थव्यवस्था को मानवीय पहलू से जोड़ते हुए दत्त कहते हैं, हमें विकास के नए पैमाने ढूंढने होंगे। जीडीपी से इतर जाकर कुछ इंडेक्स बनाने होंगे। ह्यूम डेवलेपमेंट इंडेक्स एचडीआई भी संजीदगी से पर्यावरण की बात नहीं करता है। इसलिए हमें ह्यूमन वेलफेयर इंडेक्स बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये तय करना होगा कि हमें जीडीपी किस कीमत पर चाहिए। विकास की वजह से पर्यावरण को जो विनाश हो रहा है, उसका आंकलन नहीं हो पा रहा है। भारत में पर्यावरण और प्रकृति के पैरोकारों को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपनी जीवन में पर्यावरण के महत्व को कई बार समझाया। उन्होंने कहा था, प्रकृति हर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, किंतु किसी एक भी मनुष्य के लोभ को पूरा करने की इसमें क्षमता नहीं है। बीते कुछ सालों में पर्यावरण में आ रहे बदलावों को ही हम देख लें और उसके दुष्परिणामों पर गहन विचार करें तो हमें इसके संरक्षण की दिशा में एक समाधान मिल सकता है। वरना आने वाले सालों में तबाही का मंजर और भी बुरा हो सकता है। इसलिए मानवीय लोभ के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा और अपने स्तर पर काम शुरू करना होगाण् हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास सदियों पुराना है।
हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओत.प्रोत थी। साक्ष्य बताते हैं कि भारत में वैज्ञानिक वानिकी का शुभारम्भ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था तथा उनके शासनकाल से लेकर अशोक महान तक देश में पर्यावरण संरक्षण की सुदीर्घ परम्परा दृष्टिगोचर होती है। सम्राट अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उस समय वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु कई अभयारण्य बनाये गये थे। वन्य सम्पदा के संरक्षण के प्रति यह प्रेम मध्यकालीन भारत में भी बना रहा। दिल्ली सल्तनत ने पर्यावरण को शुद्ध रखने हेतु वृक्षारोपण के अनेक योजनाएं चलायीं। इस बात की साक्षी समूचे देश में मौजूद मुगलकालीन बाग आज भी देते हैं। परन्तु, हमारी अमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा के दोहन की विनाशकारी नीतियों के चलते देश में पारिस्थितिकी असंतुलन की जो समस्या शुरू हुई, वह आज चरम पर पहुंच चुकी है। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों और वनों को यदि समय रहते नहीं बचाया गया तो इसका दुष्प्रभाव पूरे देश पर पड़े बिना नहीं रहेगा। यदि हिमालय बचेगा, तभी नदियाँ बचेंगी और तभी इस क्षेत्र में रहने.बसने वाली आबादी का जीवन भी सुरक्षित रह पाएगा। असलियत यह है कि विकास के ढेरों दावों के बावजूद अभी भी हिमालय क्षेत्र में रहने वाली आबादी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। उनके जीवन में आज भी सुधार नहीं आ पाया है।