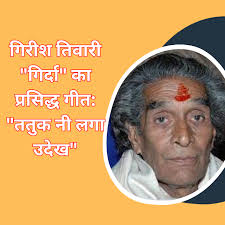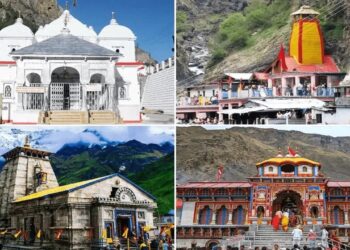डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
नौ सितंबर 1945 को अल्मोड़ा में हवालबाग में जन्मे यह भारतीय स्वतंत्रता
आंदोलन का चरम था। अल्मोड़ा जनपद की इसमें महत्पूर्ण भागीदारी थी। कोसी
नदी और सूर्य मंदिर कटारमल के पास स्थित इस गांव के पास प्रकृति और
सांस्कृतिक धरोहर दोनों थे। ‘गिर्दा’ में बचपन से ही प्रतिकार के बीज स्फुटित
होने लगे थे। उनका औपचारिक पढ़ाई में मन नहीं रमता। उन्हें लोक में बिखरी वे
सारी ध्वनियां प्रभावित कर रही थी जो ढोल-दमाऊं, हुड़़का से निकल रही थी।
वे सुर उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे जो लोक गिदारों के कंठ से निकलकर झोड़े,
चांचरी, न्यौली, भगनौले और होली के रूप में लोगों के बीच आ रहे थे।
स्वाभाविक रूप से इस तरह की प्रवृत्ति से फिर वे अपने व्यवस्थित जीवन के प्रति
सोच भी नहीं सकते थे। अपने गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गिर्दा
अपने दीदी-जीजा के साथ पढ़़ने के लिये अल्मोड़ा चले गये। यहां तो उनकी
अराजकता और बढ़़ गई। लल्मोड़ा तो ऐसे लोगों के लिये खाद-पानी का काम
करता था। यहीं उनकी रुचियों ने और विस्तार लिया। गीत-संगीत के अलावा वे
यहां अन्य विधाओं से भी परिचित होने लगे। यहां रहकर किसी तरह हाईस्कूल
पास कर वापस गांव आ गये। यहीं उन्होंने गाय-बकरियां चराते गीते लिख और
गाये।गिर्दा 1961-62 में पूरनपुर (पीलीभीत) चले गये और वहां दैनिकभोगी
कर्मचारी के रूप में पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे। यहां दिन में नौकरी और
रात में नौटंकी देखने लगे। यहां से फिर गीत लिखना और गाना-बजाना और बढ़़
गया। यहीं उनकी मुलाकात ओवरसियर दुर्गेश पंत से हुई। यहां उन्होंने विभिन्न
कुमाउनी कवियों की कविताओं का एक संकलन ‘शिखरों के स्वर’ नाम से
प्रकाशित किया। अन्य संग्रह भी छापने की योजना थी, लेकिन जगह-जगह
भटकने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। यहां से फिर ‘गिर्दा’ 1964-65 में
लखनऊ चले गये। यहां भी दिहाड़ी की मजदूरी और रिक्शा चलाने लगे।
औपचारिक शिक्षा के बजाए वह लखनऊ के पार्कों में जीवन के यथार्थ को जानने-
समझने लगे। जिन ग्वालो, हुड़़कियों और गिदारों को वह गांव में छोड़ आये थे,
उन्हें वे यहां दलितों के रूप में मिल गये। फैज और साहिर लुधियानवी जैसों की
नज्में उन्हें उद्वेलित कर रही थी। उनमें प्रतिकार की ऊर्जा पैदा कर रही थी। और
यही से उनकी ‘गिर्दा’ बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ‘गिर्दा’ पर फैज और साहिर
का कितना प्रभाव था उसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने इन दोनों
की नज्मों का कुमाउनी में अनुवाद कर डाला। फैज के ‘हम मेहनतकश जग वालों
से जब अपाना हिस्सा मांगेंगे’ का कुमाउनी अनुवाद देखने लायक है- ‘हम ओड़
बारूड़ी-ल्वार-कुली-कबाड़ी/जब य दुनी थैं हिसाब ल्यूलों/एक हांग नि मांगू-फांग
नि मांगू खाता-खतौनी को हिसाब ल्यूंलो।’ साहिर के गीत ‘वो सुबह तो
आयेगी….’ को ‘जैंता एक दिन तो आलो दिन य दुनि में’ आंदोलनों के शीर्षक
गीत बन गये।उस दौर में आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र से ‘उत्तरायण’ कार्यक्रम में
कुमाउनी और गढ़़वाली रचनाकारों की गीत-कविताएं प्रसारित हो रही थी।
‘उत्तरायण’ के लिये ‘गिर्दा’ ने कई कविताएं, गीत और रूपक लिखे। अपने गांव से
अल्मोड़ा, पूरनपुर और लखनऊ तक की गिर्दा की यात्रा हमेशा जीवन के यथार्थ
को जानने की रही। बचपन में जगरियों और हुड़़कियों, नैनीताल में हुड़़का बजाते
भीख मांगते सूरदास जगरिये की प्रतिभा को पहचानने के बाद भारत-नेपाल
सीमा में रहने वाले लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध करने तक का ‘गिर्दा’ ने
विस्तृत आयाम पाया। ‘गिर्दा’ की रचना-यात्रा का एक नया पड़ाव तब आया जब
1967 में ब्रजेन्द्र लाल साह उन्हें गीत एंव नाटक प्रभाग, नैनीताल ले आये। यह
उनके जीवन का न केवल महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि उनके पहाड़़ आने की हरसत
भी पूरी हो गयी। और यहीं से फिर एक नये ‘गिर्दा’ का गढ़़़ना भी शुरू हो गया।
यह दौर लगभग देश में और पहाड़़ में भी नई राजनीति-सांस्कृतिक चेतना की
पूर्व पीठिका बना रहा था। सत्तर का पूरा दशक जनांदोलनों का रहा जिसमें
‘गिर्दा’ ने एक रचनाधर्मी और आंदोलनकारी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान
दिया। नैनीताल में आकर ‘गिर्दा’ के व्यक्तित्व ने अपना फलक और व्यापक किया।
यहां के रंगमंचीय माहौल ने उनकी अभिव्यक्ति के और रास्ते खोले। इस दौर में
गिर्दा ने ‘अंधेर नगरी’, ‘मिस्टर ग्लाड’, ‘धनुष यज्ञ’, ‘नगाड़े़ खामोश हैं’, ‘हमारी
कविता के आंखर’ के अलावा ‘उत्तराखंड काव्य’ और ‘जागर’ की पुस्तिकाओं के
माध्यम से अपने रचनाकर्म को आगे बढ़ाया।गिर्दा की कर्मभूमि नैनीताल रही है।
गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकार के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन, नशा
नहीं रोजगार दो, समेत माफिया विरोधी आंदोलनों में गिर्दा के गीतों ने नया
जोश भर दिया। गिर्दा उत्तराखंड राज्य के एक आंदोलनकारी जनकवि थे,उनकी
जीवंत कविताएं अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देतीं हैं। वह लोक संस्कृति के
इतिहास से जुड़े गुमानी पंत तथा गौर्दा का अनुशरण करते हुए ही राष्ट्रभक्ति पूर्ण
काव्यगंगा से उत्तराखंड की देवभूमि का अभिषेक कर रहे थे। हर वर्ष मेलों के
अवसर पर देशकाल के हालातों पर पैनी नज़र रखते हुए झोड़ा- चांचरी के
पारंपरिक लोककाव्य को उन्होंने जनोपयोगी बनाया। इसलिए वे आम जनता में
‘जनकवि’ के रूप में प्रसिद्ध हुए।आंदोलनों में सक्रिय होकर कविता करने तथा
कविता की पंक्तियों में जन-मन को आन्दोलित करने की ऊर्जा भरने का गिर्दा’ का
अंदाज निराला ही था। उनकी कविताएं बेहद व्यंग्यपूर्ण तथा तीर की तरह
घायल करने वाली होती हैं-“बात हमारे जंगलों की क्या करते हो,बात अपने
जंगले की सुनाओ तो कोई बात करें।”मेहनतकश लोगों की पक्षधर उनकी कविता
उन भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की दम्भपूर्ण मानसिकता को चुनौती देती है,जो
आजादी मिलने के बाद भी मजदूर-किसानों का शोषण करते आए हैं और अपनी
भ्रष्ट नीतियों से यहां की भोली भाली जनता को पलायन के लिए विवश करते
आए हैं-
‘हम ओड़ बारुड़ि, ल्वार, कुल्ली कभाड़ी,जै दिन यो दुनी बै हिसाब ल्यूंलो, एक
हाङ नि मांगुल, एक फाङ न मांगुंल, सबै खसरा खतौनी हिसाब ल्यूंलो।”
उत्तराखंड राज्य आन्दोलन से अपना नया राज्य हासिल करने पर उसके बदलाव
को व्यंग्यपूर्ण लहजे में बयाँ करते हुए गिर्दा कुछ इस अंदाज से कहते हैं-“कुछ नहीं
बदला कैसे कहूँ, दो बार नाम बदला-अदला, चार-चार मुख्यमंत्री बदले, पर नहीं
बदला तो हमारा मुकद्दर, और उसे बदलने की कोशिश तो हुई ही नहीं।”गिर्दा
राज्य की राजधानी गैरसैण क्यों चाहते थे? उसके समर्थन में वे कहते थे- “हमने
गैरसैण राजधानी इसलिए माँगी थी ताकि अपनी ‘औकात’ के हिसाब से
राजधानी बनाएं, छोटी सी ‘डिबिया सी’ राजधानी, हाई स्कूल के कमरे जितनी
‘काले पाथर’ के छत वाली विधानसभा, जिसमें हेड मास्टर की जगह विधानसभा
अध्यक्ष और बच्चों की जगह आगे मंत्री और पीछे विधायक बैठते, इंटर कालेज
जैसी विधान परिषद्, प्रिंसिपल साहब के आवास जैसे राजभवन तथा
मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के आवास।”गिर्दा ने अपनी कविता ‘जहां न बस्ता कंधा
तोड़े,ऐसा हो स्कूल हमारा’ के द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपना
नज़रिया रखा तो दूसरी ओर उत्तराखंड की सूखती नदियों और लुप्त होते
जलधाराओं के बारे में भी उनकी चिंता ‘मेरि कोसी हरै गे’ के जरिए उनकी
कविता नदी व पानी बचाओ आंदोलन के साथ सीधा संवाद करती है।हिमालय के
जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जीवन भर संघर्षरत गिर्दा के गीतों ने
विश्व पर्यावरण की चुनौतियों से भी संवाद किया है। आज बड़े बड़े बांधों के
माध्यम से उत्तराखंड की नदियों को बिजली बेचने के लिए कैद किया जा रहा
है,जिसकी वजह से नदियां सूखती जा रही हैं, वहां के नौले धारे आदि जलस्रोत
सूखते जा रहे हैं। अनेक नदियों और जल संसाधनों से सुसम्पन्न उत्तराखंड
हिमालय के मूल निवासी पानी की बूँद बूँद के लिए तरस रहे हैं।आज के सन्दर्भ में
जब एक ओर समस्त देश जलसंकट की विकट समस्या से ग्रस्त है तो दूसरी ओर
जल जंगल का व्यापार करने वाले जल माफिया और वन माफ़िया प्राकृतिक
संसाधनों का इस प्रकार निर्ममता से दोहन कर रहे हैं, जिसका सारा ख़ामियाजा
पहाड़ के आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अंधविकासवाद के
नाम पर जल,जंगल और जमीन का इतना भारी मात्रा में दोहन हो चुका है कि
चारों ओर कंक्रीट के जंगल बिछा दिए गए हैं और नौले, गधेरे सूखते जा रहे हैं,
जिसके कारण पहाड़ के मूल निवासी पलायन के लिए मजबूर हैं।गिर्दा के गीतों में
उत्तराखंड के जीवन स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने की पीड़ा विशेष रूप
से अभिव्यक्त हुई है।दरअसल, उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य के
विकास की जो परिकल्पना गिर्दा ने की थी वह मूलतः पर्यावरणवादी थी। उसमें
टिहरी जैसे बड़े बड़े बांधों के लिए कोई स्थान नहीं था।आज यदि गिर्दा जीवित
होते तो विकास के नाम पर पहाड़ों के तोड़ फोड़ और जंगलों को नष्ट करने के
खिलाफ जन आंदोलन का स्वर कुछ और ही तीखा और धारदार होता। गिर्दा की
सोच पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ नहीं करने की सोच थी। उनका मानना था कि
छोटे छोटे बांधों और पारंपरिक पनघटों, और प्राकृतिक जलसंचयन प्रणालियों के
संवर्धन व विकास से उत्तराखंड राज्य के अधूरे सपनों को सच किया जा सकता
है। गिर्दा कहा करते थे कि हमारे यहां सड़कें इसलिए न बनें कि वह बेरोजगारी के
कारण पलायन का मार्ग खोलें,बल्कि ये सड़कें घर घर में रोजगार के अवसर
जुटाने का जरिया बनें। एक पुरानी कहावत है- “पहाड़ का पानी और पहाड़ की
जवानी पहाड़ के काम नहीं आनी”। गिर्दा इस कहावत को उलटना चाहते थे। वे
चाहते थे कि हमारा पानी,बिजली बनकर महानगरों को ही न चमकाए बल्कि
हमारे पनघटों, चरागाहों, लघु-मंझले उद्योग धंधों को भी ऊर्जा देकर खेत
खलिहानों को हराभरा रखे और गांव गांव में बेरोजगार युवकों को आजीविका के
साधन मुहैय्या करवाए ताकि पलायन की भेड़चाल को रोका जा सके।गिर्दा ने
साहित्य जगत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वह संस्कृतिकर्मी थे, उन्होंने
हिंदी, कुमाउनी, गढ़वाली में गीत लिखे हैं, जिनमें उत्तराखंड आंदोलन, चिपको
आंदोलन, झोड़ा, चांचरी, छपेली व जागर आदि के माध्यम से समाज को
परिवर्तित करने पर बल दिया गया है। वे हमेशा समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक
व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे थे।लोककवि गिर्दा एक अजीब किस्म के फक्कड़
बाबा कवि थे। उनके फक्कड़ काव्य में फक्कड़पन का लहजा भी स्वयं भोगी हुई
विपदाओं और कठिनाइयों से जन्मा था। वह खुद फक्कड़ होते हुए भी दूसरे फक्कड़ों
की मदद करने का जज़्बा रखते थे। लखीमपुर खीरी में जब एक चोर उनकी गठरी
चुरा रहा था तो उन्होंने उसे यह कहकर अपनी घड़ी भी सौप दी थी कि ‘यार,
मुझे लगता है, मुझसे ज्यादा तू फक्कड़ है।’ गिर्दा ने आजीविका के लिए लखनऊ में
रिक्शा भी चलाया। उनके फक्कड़पन की एक मिसाल यह भी है कि उन्होंने
मल्लीताल में नेपाली मजदूरों के साथ रह कर मेहनतकश कुली मजदूरों के दुःख
दर्द को नजदीक से देखा था। भारत और नेपाल की साझा संस्कृति के प्रतीक
कलाकार झूसिया दमाई को वह समाज के समक्ष लाए।हंसादत्त तिवाड़ी व
जीवंती तिवाड़ी के उच्च कुलीन घर में जन्मे गिर्दा का यह फक्कड़पन ही था कि
1977 में वन आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘हुड़का’ बजाते हुए सड़क
पर आंदोलनकारियों के साथ कूद पड़े। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी गिर्दा
कंधे में लाउडस्पीकर लगाकर ‘चलता फिरता रेडियो’ बन जाया करते थे और
प्रतिदिन शाम को नैनीताल में तल्लीताल डांठ पर आंदोलन से जुड़े ताजा
समाचार सुनाते थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी व विराट प्रकृति का था।
कमजोर और पिछड़े तपके की जनभावनाओं को स्वर प्रदान करना गिर्दा की
कविताओं का मुख्य उद्देश्य था।'गिर्दा' का यह गीत उत्तराखंड आंदोलन के दौरान
बहुत लोकप्रिय हुआ। इस गीत के बारे में 'गिर्दा' कहते हैं-“यह गीत तो मनुष्य के
मनुष्य होने की यात्रा का गीत है। मनुष्य द्वारा जो सुंदरतम् समाज भविष्य में
निर्मित होगा उसकी प्रेरणा का गीत है यह, उसका खाका भर है। इसमें अभी और
कई रंग भरे जाने हैं मनुष्य की विकास यात्रा के। इसलिए वह दिन इतनी जल्दी
कैसे आ जायेगा। इस वक्त तो घोर संकटग्रस्त-संक्रमणकाल से गुजर रहे है नां हम
सब।लेकिन एक दिन यह गीत-कल्पना जरूर साकार होगी इसका विश्वास है और
इसी विश्वास की सटीक अभिव्यक्ति वर्तमान में चाहिए, बस।”गिर्दा चाहते थे कि
सरकारें व राजनीतिक दल अपने राजनैतिक स्वार्थों और सत्ता भोगने की लालसा
से ऊपर उठकर नए राज्य की उन जन-आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करें
जिसके लिए एक लम्बे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। पर
विडंबना यह रही कि उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के लम्बे संघर्ष के बाद
राजनेताओं ने इस राज्य की जो बदहाली की उससे सुराज्य का सपना देखने वाले
इस स्वप्नद्रष्टा कवि का सपना टूट गया। गिर्दा की कविताओं में इस अधूरे सपनों
का दर्द भी छलका है।वे कहा करते थे-
“हम भोले-भाले पहाड़ियों को हमेशा ही सबने छला है। पहले दूसरे छलते थे और
अब अपने छल रहे हैं।”उन्हें इस बात का भी मलाल रहा कि हमने देश-दुनिया के
अनूठे ‘चिपको आन्दोलन’ वाला वनान्दोलन लड़ा, इसमें हमें कहने को जीत
मिली, लेकिन सच्चाई कुछ और थी।दरअसल, गिर्दा को आखिरी दिनों में यह टीस
बहुत कष्ट पहुंचाती रही कि शासन सत्ता ने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों
के कंधे का इस्तेमाल कर अपने शासकीय अधिकारों को तो मजबूत किया किंतु
आंदोलन में साथ दे रहे पहाड़वासियों से उनके जल, जंगल, जमीन से जुड़े
मौलिक अधिकार छीन लिए। उनके अनुसार 1972 में वनांदोलन शुरू होने के
पीछे लोगों की मंशा वनों से जीवन-यापन के लिए अपने अधिकार लेने की लड़ाई
थी। सरकार स्टार पेपर मिल सहारनपुर को कौड़ियों के भाव यहां की वन संपदा
लुटा रही थी। स्थानीय जनता ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बदले में
पहाड़वासियों को जो वन अधिनियम मिला,उसके तहत जनता अपनी भूमि के
निजी पेड़ों तक को नहीं काट सकती है किन्तु अपने जीवन यापन की जरूरतों को
पूरा करने के लिए उसे गिनी चुनी लकड़ी लेने के लिए भी मीलों दूर जाना पड़ता
है। सरकार के इस रवैये के कारण आमजनता का अपने वनों से आत्मीयता का
रिश्ता खत्म हो गया है और उन्हें सरकारी सम्पत्ति की निगाह से देखा जाने लगा
है। सरकारी वन अधिनियम से वनों का कटना नहीं रुका, उल्टे वन विभाग और
बिल्डर माफिया इन वनों को वेदर्दी से काटने लगे। पत्रकार जगमोहन 'आज़ाद' से
बातचीत के दौरान 'गिर्दा' अपनी लोक-संस्कृति की सोच को स्पष्ट करते हुए कहते
हैं-“लोक-संस्कृति सामाजिक उत्पाद है, पूरा सामाजिक चक्र चल रहा है,
ऐतिहासिक चक्र चल रहा है और इस चक्र में जो पैदा होता है वही तो हमारी
संस्कृति है। संस्कृति का मतलब खाली मंच पर गाना या कविता लिख देना,
घघरा और पिछोड़ा पहने से संस्कृति नहीं बनती है। संस्कृति तो जीवन शैली है,
वह तो सामाजिक उत्पाद है। जिन-जिन मुकामों से मनुष्य की विकास यात्रा
गुजरती है, उन-उन मुकामों के अवशेष आज हमारी संस्कृति में मौजूद है,यही तो
ऐतिहासिक उत्पाद हैं जिन्हें इतिहास ने जन्म दिया है।”हिन्दी लोक साहित्य हो
या कुमाउँनी लोक साहित्य, लोक संस्कृति से सम्बद्ध तथ्यात्मक समग्र जानकारी
उनके पास होती थी। इसलिए उन्हें कुमाऊंनीं लोक साहित्य और संस्कृति का
‘जीवित एनसाइक्लोपीडिया’ भी माना जाता था। उत्तराखंड संस्कृति के बारे में
'गिर्दा' कहते हैं-
“हमारी संस्कृति मडुवा, मादिरा, जौं और गेहूं के बीजों को भकारों, कनस्तरों
और टोकरों में बचाकर रखने, मुसीबत के समय के लिए पहले प्रबंध करने और
स्वावलंबन की रही है, यह केवल ‘तीलै धारु बोला’ तक सीमित नहीं है। आखिर
अपने घर की रोटी और लंगोटी ही तो हमें बचाऐगी। गांधी जी ने भी तो ‘अपने
दरवाजे खिड़कियां खुली रखो’ के साथ चरखा कातकर यही कहा था। वह सब
हमने भुला दिया। आज हमारे गांव रिसोर्ट बनते जा रहे हैं। नदियां गंदगी बहाने
का माध्यम बना दी गई हैं। स्थिति यह है कि हम दूसरों पर आश्रित हैं, और अपने
दम पर कुछ माह जिंदा रहने की स्थिति में भी नहीं हैं।”गिर्दा‘ का जन्म 10
सितम्बर, 1945 को अल्मोड़ा जिले के हवालबाग के ज्योली तल्ला स्यूनारा में
हुआ था। उनके द्वारा रचित बहुचर्चित रचनाएँ हैं- ‘जंग किससे लिये’ (हिंदी
कविता संकलन), ‘जैंता एक दिन तो आलो’’ (कुमाउनी कविता संग्रह), ‘रंग डारि
दियो हो अलबेलिन में’ (होली संग्रह), ‘उत्तराखंड काव्य’, ‘सल्लाम वालेकुम’
इत्यादि। इनके अतिरिक्त दुर्गेश पंत के साथ उनका ‘शिखरों के स्वर’ नाम से
कुमाऊनीं काव्य संग्रह, व डा. शेखर पाठक के साथ ‘हमारी कविता के आखर’
आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं हैं। गिर्दा नैनीताल समाचार, पहाड़, जंगल के
दावेदार, जागर, उत्तराखंड नवनीत आदि पत्र-पत्रिकाओं से भी सक्रिय होकर जुड़े
रहे। एक नाट्यकर्मी के रूप में गिर्दा ने नाट्य संस्था युगमंच के तत्वाधान में
‘नगाड़े खामोश है’ तथा ‘थैक्यू मिस्टर ग्लाड’ का निदेशन भी किया।‘गिर्दा’ एक
प्रतिबद्ध रचनाधर्मी सांस्कृतिक व्यक्तित्व थे। गीत, कविता, नाटक, लेख,
पत्रकारिता, गायन, संगीत, निर्देशन, अभिनय आदि, यानी संस्कृति का कोई
आयाम उनसे से छूटा नहीं था। मंच से लेकर फिल्मों तक में लोगों ने ‘गिर्दा’ की
क्षमता का लोहा माना। उन्होंने ‘धनुष यज्ञ’ और ‘नगाड़े खामोश हैं’ जैसे कई
नाटक लिखे, जिससे उनकी राजनीतिक दृष्टि का भी पता चलता है। ‘गिर्दा’ ने
नाटकों में लोक और आधुनिकता के अद्भुत सामंजस्य के साथ अभिनव प्रयोग
किये और नाटकों का अपना एक पहाड़ी मुहावरा गढ़ने की कोशिश की।
पहाड़ी पारम्परिक होलियों को भी गिरदा ने न केवल एक नया आयाम दिया,
बल्कि अपनी प्रयोगधर्मी दृष्टि से सामयिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास भी किया।
इसी संदर्भ में जल समस्या से जुड़ी 'गिर्दा' की ‘इस व्योपारी को प्यास बहुत है’
शीर्षक से लिखी गई एक होली की पैरोडी बहुत लोकप्रिय है-
इस व्योपारी को प्यास बहुत है
“एक तरफ बर्बाद बस्तियाँ
एक तरफ हो तुम।
एक तरफ डूबती कश्तियाँ
एक तरफ हो तुम।
एक तरफ हैं सूखी नदियाँ
एक तरफ हो तुम।
एक तरफ है प्यासी दुनियाँ
एक तरफ हो तुम।
अजी वाह ! क्या बात तुम्हारी,
तुम तो पानी के व्योपारी,
खेल तुम्हारा, तुम्हीं खिलाड़ी,
बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी,
सारा पानी चूस रहे हो,
नदी-समन्दर लूट रहे हो,
गंगा-यमुना की छाती पर,
कंकड़-पत्थर कूट रहे हो,
उफ! तुम्हारी ये खुदगर्जी,
चलेगी कब तक ये मनमर्जी,
जिस दिन डोलगी ये धरती,
सर से निकलेगी सब मस्ती,
महल-चौबारे बह जायेंगे,
खाली रौखड़ रह जायेंगे,
बूँद-बूँद को तरसोगे जब,
बोल व्योपारी,तब क्या होगा?
नगद-उधारी,तब क्या होगा?
आज भले ही मौज उड़ा लो,
नदियों को प्यासा तड़पा लो,
गंगा को कीचड़ कर डालो,
लेकिन डोलेगी जब धरती,
बोल व्योपारी तब क्या होगा?
वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी,
तब क्या होगा?
योजनकारी तब क्या होगा?
नगद-उधारी तब क्या होगा?
एक तरफ हैं सूखी नदियाँ,
एक तरफ हो तुम।
एक तरफ है प्यासी दुनियाँ,
एक तरफ हो तुम।”
जीवन भर हिमालय के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत गिर्दा
के गीतों ने सारे विश्व को दिखा दिया कि मानवता के अधिकारों की आवाज
बुलंद करने वाला कवि किसी जाति, सम्प्रदाय, प्रान्त या देश तक सीमित नहीं
होता। उनकी अन्तिम यात्रा में ’गिर्दा’ को जिस प्रकार अपार जन-समूह ने अपनी
भावभीनी अन्तिम विदाई दी उससे भी पता चलता है कि यह जनकवि किसी
एक वर्ग विशेष का नही बल्कि वह सबका हित चिंतक होता है। गिर्दा के
देहावसान के बाद जिस तरह नैनीताल के मन्दिरों की प्रार्थनाओं,गुरुद्वारों के
सबद कीर्तन और मस्जिदों में नमाज के बाद उनका प्रसिद्ध गीत “आज हिमालय
तुमन कँ धत्यूँछ, जागो, जागो हो मेरा लाल" के स्वर बुलन्द हुए, उन्हें सुन कर
एक बार फिर यह अहसास होने लगता है कि धार्मिक कर्मकांड की विविधता के
बावजूद हम मनुष्यों की जल,जंगल और जमीन से जुड़ी समस्याएं तो समान हैं।
उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला कोई ‘गिर्दा’ जैसा फक्कड़ जनकवि जब
विदा लेता है तो पीड़ा होती ही है। बस केवल रह जाती हैं तो उसके गीतों की
ऊर्जा प्रदान करने वाली भावभीनीयादें-“ततुक नी लगा उदेख‚ घुनन मुनई न
टेक।. राज्य 25 साल से का हो गया लेकिन गिर्दा का एक-एक गीत आज भी
उतना ही ज्वलंत है जितना उस समय था. गिर्दा के गीतों को एक बार फिर से
घर-घर तक पहुँचाने की जरूरत आन पड़ी है. जिस राज्य में हम जी रहे हैं वह
कहीं से भी किसी आंदोलनकारी के सपनों का राज्य नहीं लगता. राज्य निर्माण के
लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों व उनकी माँगों को
हम भूलते जा रहे हैं और राज्य में मची लूट-खसोट-बर्बादी के मूक दर्शक बने हुए
हैं.राज्य की युवा पीढ़ी से अगर कोई पूछ ले कि गिरीश तिवारी गिर्दा को जानते
हो तो शर्त के साथ कह सकता हूँ कुछ विरले ही होंगे जो गिर्दा और उनके
जनगीतों से वाकिफ होंगे. भू-कानून को लेकर जिस तरह कुछ युवा सामने आए हैं
उससे एक उम्मीद जरूर बंधती है लेकिन अपने राज्य व राज्य आंदोलनकारियों
के सपने के उलट चल रहे उत्तराखंड को वास्तव में अगर पहाड़ोन्मुख,
जनसरोकारी, पलायनविहीन, रोजगारयुक्त, शिक्षा-स्वास्थ्य युक्त बनाना है तो
हमें गिर्दा जैसे आंदोलनकारियों को हर दिन पढ़ना व समझना होगा और उसी
हिसाब से अपनी सरकारों से माँग करनी होगी. तब जाकर कहीं हमारे सपनों का
उत्तराखंड धरातल पर नजर आएगा.। जिस राज्य का स्वप्न गिर्दा ने देखा था वैसा
उत्तराखंड राज्य यहां की जनता के लिए जब तक नहीं बनेगा, तब तक इस
जनकवि की लड़ाई उनकी कविताओं और गीतों के माध्यम से जारी रहेगी।ऐसे
विराट व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछएक शब्दों में लिख पाना असंभव है। ऐसे जनकवि
को शत् शत् नमन। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून*
*विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*