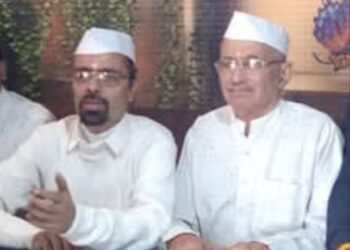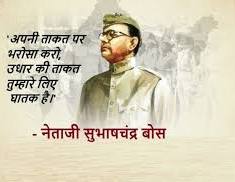शंकर सिंह भाटिया
बात 2014 की है, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत हुआ करते थे। उनसे मिलने के लिए कुछ लोगों के साथ हम लोग गए थे। उस दौरान बातचीत में बिना किसी संदर्भ के जो उद्गार तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यक्त किए थे, वह उत्तराखंड की सच्चाई हैं। यह उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों पर लागू थे, उनके बाद के मुख्यमंत्रियों पर भी वह समान रूप से आज तक लागू हैं। आगे भी न जाने कब तक यही स्थिति रहने वाली है? 19 साल के हो चुके उत्तराखंड पर इस 2014 की सच्चाई को पाठकों के सामने रखना चाहता हूं।
पहाड़़ के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। चारों तरफ से दबाव हैं। इसीलिए गैरसैंण को माध्यम बनाकर कुछ करने की सोच रहा हूं। यदि गैरसैंण को ग्रीष्म कालीन राजधानी भी बना पाया तो इसी बहाने पहाड़ के लिए कुछ करने की मंशा पूरी हो सकेगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत
बीजापुर स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री हरीश रावत से एक मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात कही। क्षेत्रीय दलों के कुछ नेता भी साथ थे। अभिवादन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के ये उद्गार सुन मैं आश्चर्य चकित था कि बिना किसी संदर्भ के वह इतनी गंभीर बात क्यों कह रहे हैं, मन में स्वतः सवाल खड़े हो रहे थे कि जब पहाड़ के लिए कुछ करने की बात आती है तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इतना विवश क्यों हो जाता हैं, चैदह साल में आठ मुख्यमंत्री देखने वाले इस अभागे प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के हमेशा हाथ बंधे क्यों रहते हैं? आखिर पहाड़ के लिए कुछ करने से रोकने के लिए एक मुख्यमंत्री के हाथ कौन बांधता है? पहाड़ों का विकास कौन रोकना चाहता है और ऐसा करके किसकी राजनीति सधती है? सरकार चाहे किसी की भी हो दिल्ली के हाथों उत्तराखंड की लगाम क्यों रहती है? कई दिनों तक मेरे मन में ये सवाल उमड़ते.घुमड़ते रहे। आज भी कौंध रहे हैं, अपनी मंद बुद्धि से उत्तर ढूंढने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उत्तर गड्मड हो रहे हैं।
गौरतनब है कि दिल्ली, लखनऊ से लेकर देहरादून और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पहाड़ को उजड़ा हुआ, जर्जरहाल देखना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ उनके लिए आज भी सिर्फ एक उपनिवेश है। वे पहाड़ को अपने पैरों पर खड़ा, अपने संसाधनों का वहां की जनता के पक्ष में इस्तेमाल होते नहीं देखना चाहते हैं। जो इसी पहाड़ में पैदा हुए और बाहर जाकर कथित बड़े हो गए, ऐसे लोग ऐसा सोचने वालों में सबसे आगे हैं। अपने बीच के लोगों का एक उदाहरण नारायण दत्त तिवारी हैं। उनका जन्म इसी पहाड़ में हुआ, वे लखनऊ दिल्ली जाकर बड़े हो गए। पहाड़ से निकले दूसरे बड़े नेताओं की तरह उनके लिए पहाड़ आज भी उपनिवेश ही है। वे इसे उपनिवेश की हैसियत से ऊपर नहीं उठने देना चाहते हैं। पिछले दिनों जब उन्हें लगा कि अब गैरसैंण की बखत बढ़ रही है, कहीं जनता इसके पक्ष में लामबंद न होने लगे, उनके दिल का दर्द छलक गया, बोले राजधानी देहरादून में ही रहनी चाहिए। अपने पांच साल के शासनकाल में दीक्षित आयोग को पुचकारते हुए उन्होंने क्या गुल खिलाए होंगे, उनकी इस मनःस्थिति से इसे समझा जा सकता है। आम उत्तराखंडवासी की तरह श्री तिवारी को मुजफ्फरनगर कांड उद्वैलित नहीं करता, इसलिए जब मर्जी आती है, वह मुलायम सिंह यादव की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अंदर और बाहर से पहाड़ों के विकास की राह रोकने वाले ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दिल्ली की हाई कमान चाहे जिस पार्टी की हो, उन्हें उत्तराखंड चलाने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं।
ऐसे ही लोगों की कृपा से संयुक्त उत्तर प्रदेश में पहाड़ों की उपेक्षा का परिणाम है, उजाड़, जर्जर और खाली होते पहाड़। उपेक्षा की जब इंतिहां हो गई तो 1994 का राज्य आंदोलन खड़ा हुआ। पांच दशक से हो रही पहाड़ों की उपेक्षा ने इसे जन-जन का आंदोलन बना दिया। अपना राज्य बने चैदह साल होने जा रहे हैं, पहाड़ आज भी उपेक्षित हैं, बल्कि उपेक्षा उत्तर प्रदेश के उस दौर के मुकाबले कहीं अधिक गहरी और पीढ़ा देने वाली है। कथित अपनों की उपेक्षा और अधिक चोट पहुंचाती है। गैरसैंण के नाटक ने शासकों की पहाड़ के प्रति सोच को उजागर किया है। अब विचारवान लोग सोचने लगे हैं कि हर क्षेत्र में हो रही उपेक्षा के इस दंश से पहाड़ों को कैसे बचाया जाए? यह सवाल आज सबसे अहम है। इस बढ़ती जा रही उपेक्षा से बचने के लिए क्या पहाड़ों को एक और आंदोलन करना चाहिए?
राज्य बनने के बाद पहाड़ों से पलायन की गति और तीव्र हुई है। पहाड़ खाली हो रहे हैं, खासकर वे सीमांत क्षेत्र जो चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने की वजह से अति संवेदनशील हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को देश की स्थायी रक्षा पंक्ति कहा जाता है। इसी स्थायी रक्षा पंक्ति पर सबसे अधिक पलायन की मार पड़ी है। पहाड़ की सबसे अधिक उपेक्षा वहां से चुनकर आए नेता कर रहे हैं। वे वहां कितनी ही बड़ी.बड़ी बातें करते हों जहां विकास की नीतियां बनती हैं, चाहे वह सरकार का चैखट हो या फिर विधानसभा-संसद का पटल, वहां पहाड़ की समस्याएं नदारद रहती हैं। विधानसभा में हरिद्वार, देहरादून की उपेक्षा पर हंगामा हो सकता है, लेकिन पहाड़ की उपेक्षा पर कोई चूं तक नहीं करता, वहां से चुनकर आए जन प्रतिनिधि भी नहीं। जब गैरसैंण पर चर्चा के लिए उत्तराखंड की दूसरी विधानसभा के सदन में सवाल रखा गया तो उस पर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। इस मुद्दे को सत्र दर सत्र टाला जाता रहा। उसके बाद भी भाजपा.कांग्रेस की तरफ से इस पर बहस करने के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ गिने चुने विधायकों ने रश्म अदायगी कर बहस को किसी मुकाम तक पहुंचने से पहले ही उस पर मिट्टी डाल दी।
चौदह साल में सात साल भाजपा और सात साल कांग्रेस का राज उत्तराखंड देख चुका है, पहाड़ की गंभीर समस्याएं उनके एजेंडे पर न तब थी, न अब हैं और न भविष्य में रहने वाली हैं। आपदा जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर सरकार राजनीति पर उतर आई है। सरकार की चिंता जून 2013 में आई आपदा से जर्जर हो चुके पहाड़ों को इस चोट से उबारने की नहीं है, बल्कि सरकार में बैठे लोगों की चिंता आपदा राहत के लिए आई राशि का हिस्सा उन जिलों तक पहुंचाने की है, जो सामान्य तौर पर उससे प्रभावित ही नहीं हैं। आपदा से सिर्फ पांच जिले प्रभावित हुए, मलाई बांटने में अप्रभावित जिले आगे रहे। आपदा प्रबंधन विभाग के सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपदा के बाद 208 करोड़ रुपये मुआवजा बांटा गया। यदि सबसे अधिक प्रभावित जिले रुद्रप्रयाग से कम प्रभावित हरिद्वार की तुलना करें तो स्थिति साफ हो जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले को 55 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। जिसमें 32 करोड़ रुपये लापता हुए जिले के 649 लोगों के परिजनों को मिले। जिस जिले में गावों और कस्बों को फाड़कर नदियां निकल गई हों, दर्जनों गांव नदी ने नीचे खींच लिए हों, वहां इस नुकसान के एवज में सिर्फ 23 करोड़ रुपये का मुआवजा बंटा, उसमें भी बहुत सारे अपात्रों को मुआवजा बांट दिया गया, जबकि हरिद्वार जिले में आपदा का कोई खास प्रभाव नहीं रहा, एक भी निर्माण वहां नहीं टूटा। वहां 30 करोड़ से अधिक रुपये का मुआवजा बांटा गया। हरिद्वार जिले को सदाबहार फसल के नुकसान पर उन्नीस करोड़ का मुआवजा दिया गया है। वह सदाबहार फसल कौन सी है और सिर्फ हरिद्वार तथा देहरादून में ही होती है? इसका जवाब बांटने वालों के पास भी नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पहाड़ में बहुत सारे पीडि़त राहत से वंचित रह गए हैं, जबकि अप्रभावित मैदान मलाई मार गया। इसकी परिणति अब आपदा प्रभावितों की आत्महत्या के रूप में सामने आ रही है। जब बहुत हो हल्ला हुआ तो जांच भी रुद्रप्रयाग जिले की ही हुई। जिसमें बहुत सारा फ्राड सामने आया है। देहरादून, हरिद्वार में जांच हो गई तो न जाने कितने बड़े फ्राड सामने आएंगे?
इस आपदा से जर्जर हो चुके पहाड़ों के पुनर्निर्माण की बात तो कोई करता ही नहीं है। पहाड़ों के पौने चार सौ गांव साल दर साल आ रही आपदा से जर्जर हो चुके हैं। इन गांवों में से अधिकांश का सर्वे भी हो चुका है। उन गांवों में रहने लायक हालात न होने के बावजूद मजबूर लोग जान हथेली में रखकर वहां रह रहे हैं। इन गांवों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार चिंतित नहीं है। जून 2013 में इतने बड़े विनाश के बाद भी केंद्र सरकार ने इन गांवों के पुनर्वास के लिए धन देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया।
उत्तराखंड राज्य गठित होने के बाद विधानसभा के पहले परिसीमन के तहत 2002 में चुनाव हुए थे। तब विधानसभा सीटों का संतुलन पहाड़ के पक्ष में था। राज्य के 88 प्रतिशत भूभाग वाले पहाड़ में 38 सीटें थी और 12 प्रतिशत भूभाग वाले मैदान में 32 सीटें थी। चार साल बाद ही 2006 में दूसरा परिसीमन हुआ और पहाड़ से छह विधानसभा सीटें कम करके मैदान में इतनी ही सीटें बढ़ा दी गई। अब सत्ता संतुलन बिल्कुल उलट गया। मैदान में 38 सीटें हो गई, जबकि पहाड़ में 32 सीटें रह गई। अगला परिसीमन 2026 में होने वाला है। जिस तरह पहाड़ में कुछ जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, जबकि बाकी जिलों में वृद्धि दर स्थिर है, जबकि मैदान में जनसंख्या वृद्धि दर 36 प्रतिशत से भी अधिक है, बीस साल बाद होने वाले परिसीमन में पहाड़ से यदि 12 से 15 सीटें कम होकर मैदान में इतनी ही सीटें बढ़ जाएंगी, तो पहाड़ों में 17 से 20 विधानसभा सीटें रह जाएंगी। यह उत्तर प्रदेश के उस दौर से भी बदतर स्थिति होगी। नेताओं का रुख जिस तरह दूसरे परिसीमन के बाद से ही पहाड़ों के प्रति बदलने लगा है, वे मैदान की ओर पलायन करने लगे हैं। इस स्थिति में क्या होगा? यह पहाड़ों के वजूद के ताबूत पर आखिरी कील नहीं होगी? यह तो तय है कि उनमें से कोई पहाड़ों के वजूद को बचाने के लिए आगे आने वाला नहीं है। यदि ऐसा होता तो 2006 में हुए परिसीमन का कम से कम उन्होंने विरोध किया होता। तब देश के पांच राज्यों ने परिसीमन आयोग को एक लाइन का प्रस्ताव भेजकर अपने राज्यों में परिसीमिन न कराने का अनुरोध किया था और उन राज्यों में नया परिसीमन नहीं हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, भाजपा भी कांग्रेस का समर्थन करती रही।
नेता उत्तराखंड को एक पर्वतीय राज्य कहकर भ्रम खड़ा करते हैं। 88 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय होने की वजह से उत्तराखंड पर्वतीय राज्य ही होना चाहिए, क्योंकि जिस उपेक्षा की प्रतिक्रिया में आंदोलन खड़ा हुआ और राज्य गठन का निर्णय हुआ, वह पहाड़ की इसी पीढ़ा का परिणाम था। राज्य बनने के बाद पहाड़ दरकिनार होता चला गया। राज्य बनने से पहले से एक मात्र आईआईटी रुड़की में स्थित था। उसके बाद एम्स आया, आईआईएम आया, कहीं से एक आवाज भी नहीं उठी कि पहाड़ों में इन संस्थानों की स्थापना हो। यहां तक कि श्रीनगर में पहले से स्थापित एनआईटी को मैदान में लाने के हथकंडे अपनाए जाते रहे, श्रीनगर के जागरूक नागरिक यदि इसे लेकर आर.पार की लड़ाई नहीं लड़ते तो एनआईटी भी किसी मैदानी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया होता। इतना ही नहीं देहरादून ने कभी पौड़ी को मंडल मुख्यालय नहीं बनने दिया। कोई निदेशालय या मुख्यालय पहाड़ों में नहीं रहने दिया गया। गोपेश्वर का पशुपालन निदेशालय ऋषिकेश में ही चलता रहा। कृषि निदेशालय तथा उर्जा निगम के मुख्य अभियंता वितरण के कार्यालयों को देहरादून से पौड़ी नहीं ले जाने दिए गए।
राजधानी का सवाल तो सबके सामने है। सारे जनमत सर्वेक्षणों में आगे रहने, प्रदेश के मध्य स्थल पर स्थित होने और पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु होने के बावजूद गैरसैंण गैर ही रह गया, राज्य के एक कौने में स्थित देहरादून अस्थायी होकर भी स्थायी राजधानी बन गई। देहरादून को राजधानी घोषित करने के लिए भाजपा तथा कांग्रेस ने मिलकर दीक्षित आयोग को खूब प्रोत्साहित किया। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि उसे सिर्फ देहरादून को राजधानी घोषित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थीए जो उसने दिन को रात कहकर भी साबित कर दिखाया।
उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज मिला, पहाड़ में एक भी उद्योग नहीं लगा। पहाड़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से उद्योग नीति बनाने का नाटक किया गया, लेकिन इसके परिणाम भी शून्य रहे। नेता कहते हैं कि पहाड़ों में उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, न ही वहां अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए वहां उद्योग नहीं स्थापित किए जा सकते हैं। असलियत यह है कि राज्य सरकार की पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने की मंशा ही नहीं है। पहाड़ों में जड़ी.बूटी का भंडार भरा पड़ा है। दिल्ली तथा हरिद्वार के आयुर्वेदिक दवाओं पर आधारित बड़े.बड़े उद्योग उत्तराखंड के पहाड़ों के कच्चे माल से ही मालामाल हो रहे हैं। लेकिन चमोली जिले के मंडल में इस प्रयोजन के लिए बने संस्थान को सरकार ने कभी इस योग्य बनने नहीं दिया। न ही पहाड़ों में छोटे.छोटे जड़ी.बूटी आधारित उद्योगों की स्थापना की पहल की।
उत्तराखंड में तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चीड़ के जंगल फैले हुए हैं, जिसमें से दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र एप्रोचेबल हैं। चीड़ की पत्तियों पिरूल को अब तक अभिशाप माना जाता हैए क्योंकि अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण यह जंगलों में आग प्रसारित करने का कारण बनते हैं। अब वैज्ञानिक शोध से यह साबित हुआ है कि पिरूल से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने दो लाख हेक्टेयर चीड़ के वनों को दिल्ली की पांच कंपनियों के सुपुर्द कर दिया है। ये कंपनियां पहाड़ों से पिरूल उठाएंगी और मैदानी क्षेत्रों में ले जाकर बिजली उत्पादन की यूनिट लगाएंगी। यदि सरकार की मंशा पहाड़ में उद्योग लगाने और इससे लोगों को जोड़ने की होती तो गांव से जुड़े चीड़ के जंगलों को उन्हें सौंपकर बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया जाता। सरकारी अनुमान के अनुसार पहाड़ में उपलब्ध पिरूल से 300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यह बिजली राज्य के ग्रिड को मजबूती प्रदान करने का काम करती और बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलता। उद्योग शून्य पहाड़ों में उद्योग दिखाई देने लगते।
उत्तराखंड सरकार की उर्जा नीति में दावा किया गया है कि जन.जन को बिजली उत्पादन से जोड़ा जाएगा। इसी नीति के तहत उत्तराखंड सरकार ने 2009.10 में 100 किलोवाट से 25 मेगावाट तक क्षमता की स्वचिन्हित बिजली परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए। करीब साढ़े सात सौ मेगावाट की 56 परियोजनाओं का आवंटन किया गया। जिसमें स्थानीय लोगों को सिर्फ 1ण्9 मेगावाट की परियोजनाएं ही आवंटित हुई। जिनके लिए नीति में बड़े.बड़े दावे किए गए थे। शेष परियोजनाएं दिल्ली चंडीगढ़ के शराब माफियाओं और कांटेªक्टरों को आवंटित कर दी गई। जबकि होना यह चाहिए था कि राज्य की घोषित नीति के अनुसार स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं को सीधे बिजली उत्पादन से जोड़ा जाता। दो मेगावाट से नीचे की क्षमता की परियोजनाओं को राज्य सरकार ने सूक्ष्म परियोजनाओं की श्रेणी में रखा है। केवल सूक्ष्म परियोजनाओं का आवंटन किया जाता। स्थानीय ग्राम सभाओंए सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को परियोजनाएं आवंटित कर अपनी ही बनाई गई नीति का अनुशरण किया जाता। उत्तराखंड में जल संसाधनों की कमी नहीं है। कमी उसके उपयोग के लिए शासकों की बेहतर सोच की है।
केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने हिमालयी राज्यों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य से एक योजना को मंजूरी दी है। जिसमें अधिकतम सौ किलोवाट तक की परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालय अनुदान देता है। एक किलोवाट के लिए एक लाख का अनुदान केंद्रीय मंत्रालय से मिलता है। इसे अब बढ़ाकर सवा लाख रुपये कर दिया गया है। इस तरह सौ किलोवाट की परियोजना के लिए सवा करोड़ रुपये का अनुदान देय है। उत्तराखंड में उपलब्ध जल संसाधनों के मद्देनजर पांच सालों में राज्य की एक हजार ऐसी परियोजनाओं को अनुदान मिल जाता। इस तरह राज्य को जहां बिना किसी प्रयास के 1250 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान मिलताए वहीं बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ.साथ बिजली उत्पादन से जन.जन की सहभागिता भी होती। इससे बिना किसी लागत के सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन होकर ग्रिड में जुड़ जाता। लेकिन हाई कोर्ट के एक निर्णय की आड़ लेकर राज्य के अफसर इस परियोजना को आगे बढ़ाने से बचते रहेए नेताओं को भी पहल करने की फुर्सत नहीं रही। इसका परिणाम यह हुआ कि इस योजना का लाभ जम्मू कश्मीर से लेकर अरूणाचल तक सभी हिमालयी राज्य उठा रहे हैंए उत्तराखंड में इस योजना के सफल होने की सबसे अधिक संभावना होने के बावजूदए यहां नौकरशाही की बदनियती और राजनीतिक नेतृत्व की अनदेखी की वजह से इतनी आकर्षक योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
राज्य सरकार तराई के किसानों को हर साल गन्ना भुगतान सुचारु बनाए रखने के लिए गन्ना महकमे के माध्यम से किसानों को करीब सौ करोड़ रुपये से अधिक देती है। दूसरी तरफ पहाड़ के किसानों को सरकार की तरफ से आज तक इस तरह की कोई मदद नहीं दी गई है। माल्टाए आलूए बागवानी से लेकर पहाड़ों में पैदा होने वाली फसलों के लिए कोई राहत न देना राज्य सरकार की भेदभाव करने वाली नीति नहीं हैघ्
राज्य प्राप्ति के बाद गढ़वाली.कुमाउंनी को राजकाज की भाषा बनाने की अपेक्षा की जा रही थी, ताकि इन मौलिक भाषाओं को अपेक्षित प्रोत्साहन मिल सके। ये भाषाएं गढ़वाल तथा कुमाऊं के राजा के शासन में शासकीय भाषाएं रही हैं। इसीलिए लोक भाषा साहित्य संस्थान की मांग की गई, जिसे कथित अपनी सरकार अब तक ठुत्कारती रही, जबकि पंजाबी और उर्दू भाषा अकादमी खोलने की घोषणा की जा चुकी है। राज्य सरकार संस्कृत को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दे चुकी है। देव भाषा संस्कृत समेत किसी भाषा का विरोध करने का यहां सवाल नहीं है। सवाल उत्तराखंड की अपनी आंचलिक भाषाओं के विकास का है। उत्तराखंड की आंचलिक भाषाओं का संरक्षण यदि उत्तराखंड राज्य में नहीं होगा तो कहां होगा? उत्तर प्रदेश में रहते हुए इन लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई, अपने राज्य में हालात उससे भी बदतर हो रहे हैं। आंचलिक भाषाओं को दरकिनार करने की यह नीति क्या संदेश देती हैघ् हवाई तौर पर कुछ नेता गढ़वाली.कुमाउनी को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने की बात करते हैंए उनकी इस तरह की बातें सिर्फ शोशेबाजी हैं। यदि जमीन पर इन लोक भाषाओं को स्मृद्ध करने के प्रयास ही नहीं हांेगे तो आठवीं अनुसूची में कैसे उन्हें स्थान मिल जाएगा? उत्तराखंड की ये लोक भाषाएं वास्तव में इतनी समृद्ध हैं कि इनमें केवल गंध बताने के लिए 50 से अधिक शब्द हैं। आवाज के लिए सौ शब्द हैं, स्वाद के लिए 32, स्पर्श के लिए 26 और संवेदना के लिए 60 से अधिक शब्द हैं। इसके बावजूद यूनेस्को की सूची में गढ़वाली तथा कुमाऊंनी भाषाएं बीमार भाषाओं की श्रेणी में रखी गई हैं। कोई भाषा.बोली इतनी समृद्ध होने के बावजूद यदि अपनों से ही उपेक्षित होती है, उसका यही हश्र होता है।
पहाड़ में नियुक्ति तथा तबादलों को आज भी कालापानी की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा, पुलिस महकमे समेत तमाम सरकारी विभागों में पहाड़ों में जाने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी तैयार नहीं होता है। जब किसी कर्मचारी या अफसर को लापरवाही समेत दूसरे कारणों से सजा दी जाती है तो उसका सजा के तौर पर पहाड़ तबादला कर दिया जाता है। मतलब यह कि उत्तराखंड की सरकार के लिए पहाड़ आज भी कालापानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सम्मेलन में अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी चार मैदानी जिलों में तबादला चाहते हैं। क्या पहाड़ों को खाली कर दें।
प्रदेश में बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात सीडी रेशो आरबीआई के बैंच मार्क से तीन प्रतिशत अधिक है। यह 60 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक 63 प्रतिशत हो गया है। मतलब यह कि प्रदेश में बैंक सौ रुपये जमा होने पर 63 रुपये ऋण के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन पर्वतीय जिलों में ऋण जमा अनुपात 40 से भी कम है। मतलब यह कि पहाड़ों में बैंकों में जमा का लाभ मैदान ले रहे हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में यह बात सामने आई है।
राज्य गठन के करीब डेढ़ दशक के सफर में दिल्ली के रिमोट से संचालित सत्ता पिपाशु पहाड़ की दुर्गति करने पर तुले हुए हैं। आने वाला समय पहाड़ के लिए और भी गर्दिश भरे दिन लाने वाला है। जब हालात इस कदर खराब हो जाएंगे और उनमें सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, तो क्या पहाड़ को एक और 1994 दोहराने के लिए आगे नहीं आना चाहिएघ् यदि पहाड़ आंदोलन न करे तो क्या करे? सवाल यह है कि इस आंदोलन का केंद्रीय बिंदु क्या होघ् क्या हमें इस हद तक जाना चाहिए कि हम मांग करें पहाड़ को मैदान से मुक्ति दे दो और केंद्र शासित प्रदेश बना दो? क्योंकि मैदान हमेशा पहाड़ के हक हड़प जाता है और डकार भी नहीं लेताए जबकि पहाड़ देखा रह जाता है?
पर्वतीय राज्यों के लिए हिमाचल प्रदेश एक उदाहरण पेश करता है। पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में महान योजनाकारए युगदृष्टा और अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तभी स्वीकार किया जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनकी इस बात से सहमत हो गया कि नवगठित हिमाचल के साथ जोड़े गए मैदानी क्षेत्र को अलग कर दिया जाएगा। फलस्वरूप पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 में संशोधन कर पैप्सू रियासत कहा जाने वाला संपूर्ण मैदानी क्षेत्र पंजाब को वापस लौटा दिया गया। एक दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत हिमाचल प्रदेश आज पहाड़ मैदान के इस विवाद से दूर है। हिमाचल प्रदेश अपनी तरह से अपना विकास कर रहा है। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश बागवानी पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मालिक है, जबकि उत्तराखंड इस विवाद में इस कदर उलझ गया है कि इन हालात में पहाड़ों का अब उबरना भी संभव नहीं दिखाई देता। सारी समस्या की जड़ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के वे प्रावधान हैं, जिसमें बिना पूर्व सहमति के हरिद्वार को जोड़ देने जैसे निर्णय थे। जिसके परिणाम अब भयावह रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के लिए ये इतने घातक होते जा रहे हैं कि अस्थित्व का संकट बन आया है।