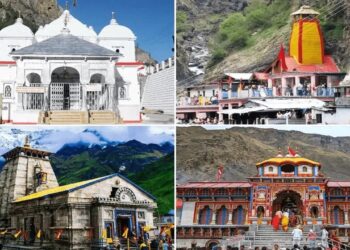हरि राम, मेरा बाल सखा, सहपाठी, फक्कड़ी में जीने वाला, लालच से दूर, एक अजीब सा व्यक्तित्व था, जिसे लोग पगला भी कह देते थे। आज उसकी असमय, दर्दनाक मौत की खबर सुनी तो मन व्यथित हो गया। हम इक्कीसवीं सदी में होने का दंभ भरते हैं, जहां जीपीएस जैसी तकनीक व्यक्ति की पल-पल की खबर रखती है, लेकिन सात दिन से उसकी लाश किसी गहरी खाई में पड़ी रही, कोई तकनीक उसे खोजने में काम नहीं आई। शरीर से उठी बदबू से उसकी लाश तक पहुंचा जा सका। हरिराम बकरियां चराने घर से निकला था, एक चट्टान से गहरी खाई में जा गिरा। सात दिन की ढूंढ खोज के बाद उसका क्षत-विक्षत शव मिला। यह खबर सुनकर दिल अंदर तक कांप गया। अभी मार्च महीने में भतीजे नवीन की शादी के लिए मैं अपने गांव गया था, शादी में हरि राम भी शामिल हुआ था, वह दमुआ बजाने वाली टीम का हिस्सा था। बड़े उत्साह के साथ उससे मुलाकात हुई थी। हरि राम से कुमाऊं की नगाड़ा वादन की परंपरा और विभिन्न विधाओं पर लंबी बातचीत हुई थी।
मेरा गांव लीमा, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के अंतर्गत पड़ता है। गांव के ऊपरी हिस्से में लटैनाथ मंदिर के सामने चोटी के उस पार किमचूरा में लाल मिट्टी के भूखंड में है, हरिराम का घर। परंपरागत कथाओं में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब कुमाऊं के इन क्षेत्रों में बसासत बसनी शुरू हुई थी, दैत्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। वह लोड़ी के निचली धार के इस तरफ अजेड़ा और दूसरी तरफ बाजानी में संहार मचाने लगा। लेकिन जब उसने लीमा की तरफ रुख किया तो लटैनाथ देवता ने उसे साध दिया। दैत्य के प्रकोप से गांव को बचा लिया। यहीं किमचूरा में ही दैत्य से लटैनाथ देवता का संघर्ष हुआ था। उसके बाद किमचूरा में भी बसासत शुरू हुई। अन्यथा दैत्य के डर से वहां बसना संभव नहीं था।
इसी किमचूरा की लाल मिट्टी में रहता है हरिराम का परिवार। यदि बारिश अच्छी हो तो यहां बहुत अच्छी फसल होती है, बारिश नहीं हुई तो मिट्टी में डाले गए बीज के बराबर भी उत्पादन नहीं होता इस भूमि से। हरिराम का घर पहाड़ की जिस चोटी पर है, उसके नीचे गहरी खाइयों की श्रृंखला चलती चली जाती है। इन्हीं खाइयों में वह सात दिन पहले कहीं गिरकर ईश्वर को प्यारा हो गया। उसका शव इन खाइयों में पड़े-पड़े सड़ता रहा। परिवार तथा गांव वाले सात दिनों तक उसे खोजते रहे। जब सड़ने के साथ शव से बदबू उठने लगी तब जाकर उसकी लाश का पता चल सका।
इन खाइयों का भूगोल मुझे अच्छी तरह याद है। हम बचपन से ही साथ-साथ कई अन्य मित्रों के साथ यहां गाय-बैल-बकरी चराने जाया करते थे। चीड़ के जंगलों के बीच पिरूल के गट्ठर बनाकर ढलानों में फिसलते हुए दूर तक चले जाया करते थे। चीड़ की पत्तियां अर्थात पिरूल बहुत अधिक फिसलन वाली होती हैं, इसलिए कई बार फिसलकर पत्थरों से चोट भी खा जाते थे, लेकिन फिर भी फिसलना नहीं छोड़ते थे। मिलकर भाप्यो घास काटते थे, जिसकी मोटी मजबूत रस्सी बनाई जाती थी, जिसे लड़ा कहा जाता था। मलैनाथ की घाड़ी में बांज के ऊंचे पेड़ की टहनी में इस रस्सी की झूला बनाते थे, और खूब झूलते थे। इस खेल में हरिराम की भूमिका हमेशा अहम् रहती थी।
इसके नीचे की तरफ स्थित जमतड़ गांव के लोगों के ये घास के मांगे हैं। जिनको लेकर लीमा-जमतड़ के बीच हमेशा से विवाद रहता था। हम अपने गाय, बैल, बकरी वहां चराते थे, जमतड़ वाले इसका विरोध करते थे। इसको लेकर अक्सर दोनों गांवों के लड़कों में विवाद हो जाता था। कभी-कभी यह मारपीट में बदल जाता था। कभी बच्चों की लड़ाई में बड़े भी शामिल हो जाते थे। हरिराम जमतड़ गांव के नजदीक, जमतड़ को जाने वाले रास्ते में रहता था, इसलिए जमतड़ के लोग चाहते थे कि वह उनका साथ दे। लेकिन हरिराम हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था, रहता भी क्यों नहीं वह हमारे गांव लीमा का रहने वाला था।
हरिराम एक गरीब अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुआ था। घर के हालात सामान्य से नीचे थे। हरिराम के पिता रुद्रराम अच्छे ढोली थे। नवरात्र में मलैनाथ, लटैनाथ के मंदिरों में नवरात्र पूजन के दौरान रात में धूनी जलाकर झोड़े गाए जाते थे। रुद्रराम को झोड़ों का अच्छा ज्ञान था। जब मलैनाथ, लटैनाथ के मंदिर में नौरात के मौके पर देवताओं के झोड़े गाए जाते थे, डंगरिया के शरीर में देवताओं का अवरतण होता था, रुद्रराम ही दैन दमुआ के साथ लरजते हुए खाणबखाण करते थे। वह पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में ले लेते थे। खाणबखाण में देवताओं की कथाओं को जोशीले ढंग से बखान करते थे। यह दमुआ की धुन के साथ देवाओं के प्रेरणापरक कथानकों का वर्णन करते थे। वीर रस से ओत प्रोत झोड़ों के खाणबखाण, नगाड़ों की लरजती धुन शरीर को झंकृत कर देती थी। डंगरियों को छोड़िये सामान्य आदमी के शरीर के बाल खड़े हो जाते थे। रुद्रराम एक तरफ दास की भूमिका में होते, दूसरी तरफ डंगरियों को निर्देशित भी करते थे।
लीमा के ढोलीराठन की गढ़देवी का डीडीहाट क्षेत्र में बड़ा नाम है। जिस व्यक्ति को कोरट, राजदरबार, पुलिस, पटवारी कहीं न्याय नहीं मिलता, वह गढ़देवी के थान में आकर अपनी पुकार लगाता है। लोक विश्वास है कि न्याय की देवी गढ़देवी दूध का दूध पानी का पानी करती है। गढ़देवी का मंदिर गरीबों का न्यायालय है। गढ़देवी के मंदिर में सबको न्याय मिलता है। रुद्रराम गढ़देवी के पुजारी थे। डीडीहाट क्षेत्र में ही नहीं, पिथौरागढ़ जिले में, यहां तक कि तराई भाबर तक लीमा की गढ़देवी की बहुत हाम है।
लोग आरोप लगाते थे कि पुजारी रुद्रराम पूजा के लिए आने वाले दोनों पक्षों से कुछ ज्यादा ही ऐंठ लेते थे। पूजा के लिए आए लोग विवश होते थे, इसलिए इंकार भी नहीं कर पाते थे। मैंने कई बार देखा हरिराम पिता के इस कृत्य का हमेशा विरोध करता था। पिता की कमाई परिवार और बेटे को ही खानी है, फिर भी हरिराम पिता का विरोध क्यों करता है? इसी वजह से कई लोग हरिराम को पागल तक कहते थे। लेकिन वास्तव में वह पागल नहीं था, बल्कि फक्कड़ किस्म का व्यक्ति था। वह कहता था कि मजबूर लोगों की विवशता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए इतना कमाने के बाद भी परिवार कभी गरीबी-गुर्बत से नहीं उबर पाया। यही वजह थी वह पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ।
आज का जमाना है कि जो मौके का फायदा उठाकर लूटमार नहीं मचाता, वह पागल ही कहा जाता है। दोनों हाथों से लूटमार करने वाला, मौके का फायदा उठाने वाला चतुर कहा जाता है। हरिराम यही नहीं था, इसलिए जीवनभर फक्कड़ी में ही जीता रहा। वह चाहता तो अपने पिता के स्थान पर गढ़देवी का पुजारी बन सकता था। जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन वह इस लालच में कभी नहीं पड़ा। उसने अपने चचेरे भाई प्रकाश को पुजारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया।
हरिराम का भगवा गमछा, साधु संतों की तरह लंबे पके बालों वाली दाड़ी, सिर पर जटाओं की मुरकी आंखों से ओझल नहीं होती। लगता है कि हरिराम सामने खड़ा है, अभी बोलेगा, साबजी कब आए, घर में सब ठीक तो हैं? हम जौरासी में नारायण की दुकान में साथ बैठकर चाय पियेंगे और वह इस दौरान इधर-उधर की सुनाता रहेगा। हरिराम अब तुम कभी नहीं सुना पाओगे। तुम चतुर नहीं बन पाए हरिराम, फक्कड़ के फक्कड़ ही रहे और फक्कड़ ही चले गए, इसलिए तुम्हारे पाल्य भी तुम्हारी फक्कड़ी की सजा भुगतने को मजबूर हैं। यह दुनिया ऐसी ही है दोस्त, यहां कुछ पाने के लिए चतुर बनना पड़ता है। चतुर बनना अब बहुत सारे लोगों ने सीख लिया है, लेकिन तुम जैसे फक्कड़ कभी चतुर नहीं बन सकते। वे फक्कड़ के फक्कड़ ही रह जाएंगे, फक्कड़ी का भी अपना आनंद होता है मित्र, जिसे चतुर बन गए लोग महसूस नहीं सकते हैं।