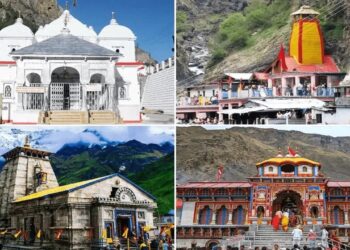डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला दून विश्वविद्यालय देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यह कई हर्बल पौधों और फलों का घर है, जो अपने अद्वितीय और अद्भुत उच्च पोषक गुणों के लिए जाने जाते है। लंबे समय से इन हिमालयी पौधों की प्रजातियों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है।च्यूरा मूलत: नेपाल का पौधा है जो कि वहाँ से होते हुए भारत से फिलीपिंस तक पाया जाता है| भारत के गढ़वाल के कुमाऊँ क्षेत्र से पूरब की ओर सिक्किम तथा भूटान (उप-हिमालयी दर्रों तह बाह्य हिमालयी घाटियों) तक भी यह पाया जाता है| यह अंडमान द्वीप समूह के उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, पर्णपाती अर्ध- पर्णपाती तथा सदाबहार जंगलों में भी पाता जाता है| यह एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष मूल तिलहन है जो कि मुख्यत: 400-1400 मीटर तक की ऊँचाई वाले दर्रों के किनारे तथा छायादार घाटियों में पाया जाता है|पिथौरागढ़ और चम्पावत जिलों में काली और सरयू नदी घाटी में बहुतायत में पाया जाने वाला च्यूरा अभी भी उपेक्षित है। जड़ से लेकर पत्तियों तक बहुउपयोगी इस वृक्ष को अभी तक सरकारी संरक्षण नहीं मिला है। प्रकृति में उगे हर वृक्ष की अपनी विशेषताएं होती हैं, काली और सरयू नदी घाटी में नाप और बेनाप भूमि पर पाया जाने वाला च्यूरा वृक्ष कई विशेषताओं को समेटे है। विशाल आकार के च्यूरा के फल, फूल, पत्ती, छाल, लकड़ी सभी उपयोगी हैं। सदियों से इनका उपयोग होता आया है। शहद, घी, तेल, साबुन, धूप, अगरबत्ती। च्यूरा के फूलों से शहद बनता है। इसके फूलों में दोनों तरफ पराग होता है, जिस कारण इससे बनने वाले शहद की मात्रा काफी अधिक रहती है। च्यूरा के फल बेहद मीठे और रसीले होते हैं, जिन्हें पराठों आदि में प्रयोग किया जाता है। फलों की गुठली से वनस्पति घी और तेल बनता है। इसमें वसा की मात्रा काफी अधिक होने से इससे साबुन भी बनने लगा है, जिसकी मांग काफी अधिक है। इसकी खली जानवरों के लिए सबसे अधिक पौष्टिक मानी जाती है। इसे जलाकर इसके धुएं से मच्छर भगाए जाते हैं। च्यूरा के पुष्प से धूप और अगरबत्ती भी बनती है। च्यूरा से एक कीटनाशक दवा बनने का भी शोध हो चुका है च्यूरा स्थानीय आस्था से भी जुड़ा है। गृह प्रवेश से लेकर अन्य मांगलिक कार्यो में च्यूरा के पत्तों की माला बनाकर मकान के चारों तरफ लगाने की परंपरा रही है। आज भी गांवों में इस परंपरा का पालन किया जाता है। च्यूरा वृक्ष विशाल होते हैं। इसकी जड़ें भी गहरी होती हैं जिसके चलते यह भू क्षरण रोकने में सहायक रहता है। च्यूरा बहुतायत वाले क्षेत्रों में भू कटाव का अनुपात अन्य स्थानों की अपेक्षा काफी कम रहता है। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के लिए सर्वोत्तम चारा होती हैं। च्यूरा वृक्ष अपने आप में एक विशेष प्रजाति है। मौन पालन के लिए यह वरदान है। च्यूरा फल की गुठलियों में वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे घी बनता है। यह काफी अधिक पौष्टिक है। च्यूरा पर आधारित उद्यम पहाड़ की आर्थिकी उत्थान में सहायक साबित हो सकती है।च्यूरा का घी काफी होता है| इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा एश (भस्म) की मात्रा क्रमश: 5-20%, 30% तथा 3.8% तक होती है| इसके रस का उपयोग शीतल पेय के रूप में भी किया जाता है| च्यूरा के रस विद्यमान मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं:-
कूल घुलनशील ठोस तत्व
17-230 बी
नॉन – रिड्यूसिंग सुगर
8.31-11.9%
पी.एच
5.4
रिड्यूसिंग सुगर
4.8-6.1%
विटामिन सी
38 मि. ग्रा. प्रति 100 ग्राम
कुमाऊँ के के स्थानीय कृषक समुदाय द्वारा च्यूरा के उप्तादों का उपयोग किया जाता और इनका उपयोग खासकर घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है| उन्हें च्यूरा के उत्पादों के बाजरा भाव की सही – सही जानकारी नहीं होती है| च्यूरा का फल जितना सूखा होता है उसी के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होता है| कच्चे फलों की तुलना में सूखे फलों की अधिक कीमत मिलती है| व्यापारियों को फसल तैयार होने के पहले ही फसल बेच दिया जाना आम बात है| व्यापारी, फसल बेचने वाले किसानों को आवश्यक्तानुसार किस्तों में इसकी कीमत अदा करता रहता है| उत्पादकों द्वारा अधिकतर तो सीधे ही व्यापारियों को उत्पाद/ फसल बेच दिए जाते हैं इसलिए उन्हें फसल तैयार किए जाने वाले स्थानों से संग्रह केंद्र तक के किराए के खर्चे का वहन नहीं करना पड़ता है| व्यापारियों द्वारा 15-20 रूपए प्रति बैग की दर से पैकेजिंग का खर्च किया जाता है| सामान्यत: व्यपारियों द्वारा लगभग दो महीनों तक च्यूरा का भंडारण किया जाता है ताकि इसमें मौजूद नमी की मात्रा कम हो सके| खरीदने से पहले व्यापारियों द्वारा इस बात की ताकीद की जाती है कि च्यूरा अच्छी क्वालिटी का हो| च्यूरा के बड़े व मासल फल, अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं| उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में तो कुछ लोगों द्वारा दशकों से च्यूरा घी का उपभोग सामान्य घी के तौर पर किया जा रहा है| वे इसके उपभोग के अभ्यस्त हो चुके हैं| च्यूरा के पौधारोपण तथा रख रखाव का खर्च, पौधारोपण के स्थान, निवेश की लागत, मजदूरी इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसके अनुसार प्रति हैक्टेयर लगभग 9000-10000/- रूपए की दर से खर्च होता है| 7-8 वर्षों के बाद इससे फल प्राप्त होना शूरू हो जाता है जिससे कि 50-60 वर्ष तक हरेक वैकल्पिक वर्षो में उपज/फसल प्राप्त होती है| च्यूरा के बीज के बाजार भाव 10-15 रूपए/ किलो ग्राम तक प्राप्त हो जाता है| इस प्रकार इससे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष लगभग 70,000 -1,20,000/- रूपए तक की औसत आमदनी होती है| च्यूरा के पेड़ के ताजा हरे पत्ते जानवरों के लिए अच्छा चारा है और सूखने के बाद यही पत्ते खेतों के लिए अच्छी खाद भी है। बारिश के दिनों में पानी के बहाव से पहाड़ों में होने वाले मिट्टी के कटाव को भी ये पत्ते रोकते हैं। च्यूरा का पेड़ जब सूख जाता है तब इसकी लकडिय़ां कई प्रकार से फर्नीचर आदि बनाने एवं ईंधन के रूप में जलाने के काम आती हैं। लकडिय़ों को जलाने के बाद जो राख बच जाती हैं, उस बची हुई राख को गरीब लोग गंदे हाथ-पैर तथा कपड़े एवं बर्तन साफ करने के काम में लाते हैं। इस प्रकार यह राख गरीब लोगों के लिए सस्ता, अच्छा और हािन रहित डिटर्जेंट पाउडर है। लेकिन तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास हेतु तथा जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण इन पेड़ों की संख्या दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। और एक दिन यह पेड़ यहां से लुप्त हो जाएगा। एक अंग्रेज ने इसका नाम ही ‘घी का पेड़’ यानी ‘इंडियन बटर ट्री’ रख दिया। स्थानीय लोग इसको ‘च्यूरा’ कहकर पुकारते हैं। इस पेड़ से न केवल फल व ईंधन ही प्राप्त होता है, बल्कि इससे घी, गुड़, शहद, औषध, जानवरों के लिए चारा, कीटनाशक एवं हाथ तथा कपड़ा धोने का पाउडर भी मिलता है यह पर्वतीय इलाकों की आर्थिकी एवं पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों को पूरा करने में बेहद मददगार है। आसमान छूती महंगाई के इस दौर में कोई पेड़ घी देने लगे, तो इससे सुखद स्थिति और क्या होगी। चौंकिए नहीं, इस तरह का पेड़ उत्तराखंड में है। च्यूर नाम का यह पेड़ देवभूमि वासियों को वर्षों से घी उपलब्ध करा रहा है। इसी खासियत के कारण इसे इंडियन बटर ट्री कहा जाता है। बस, जरूरत इसके व्यावसायिक इस्तेमाल की है उत्तराखंड में यह बहुतायत में पाया जता है. लेकिन लोगों को अभी इसके महत्व का पता नहीं है. है भी तो वे इसे भुलाते जा रहे हैं. नाबार्ड समेत गैर सरकारी संस्थाओं के अध्ययन बताते हैं कि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 120 टन यानी बारह हजार कुंतल च्यूर घी [वनस्पति घी] के उत्पादन की संभावना है। हालांकि, फिलहाल करीब 110 कुंतल ही उत्पादन हो पा रहा है। लेकिन तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास हेतु तथा जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण इन पेड़ों की संख्या दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। और एक दिन यह पेड़ यहां से लुप्त हो जाएगा।
उत्तराखण्ड सरकार के अधीन उद्यान विभाग के वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर चुके हैं वर्तमान में दून विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।
पर्यावरण और हरियाली को बचाने को लेकर जब भी बात की जाती है तो उत्तराखंड प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में 1970 के दशक के ‘चिपको आंदोलन’ का जिक्र होना स्वाभाविक है। पहाड़ के जंगलों को बचाने के लिए अलख जगाने वाली गौरा देवी और उनके सहयोगी इस आंदोलन के जनक और प्रेरणाश्रोत के रूप में देश-दुनिया में पहचाने जाते हैं। उत्तराखंड के दूर-दराज के जिले चमोली की ग्रामीण महिलाओं के अथक प्रयासों और चिपको की नीति पर आधारित लंबी लड़ाई के बाद जंगल माफियाओं और ठेकेदारों के साथ सरकार को भी अपनी नीति में बदलाव लाकर घुटने टेकने पड़े थे। यह एक बड़ा सच है कि जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की राह सदियों तक जनता के हक-हकूकों को हासिल करने के लिए एक मागदर्शी का काम करती रहेंगी। दून घाटी में चूना पत्थरों की खुदाई से मसूरी और उसके आस-पास की पहाडि़यों को भारी नुकसान पहुंचने के साथ पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इस दौरान प्रकृति के स्वरूप और पर्यावरण को बचाने आगे आए पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई में जीत हासिल की। पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिपको आंदोलन की तर्ज पर देशभर में हुए अन्य कई आंदोलन भी जनता की जीत के पर्याय बन गए। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के जनक रहे उत्तराखंड में मानवीय आवश्यकताओं के बढ़ने से पर्यावरण का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। हरियाली को बचाना प्रदेश के पर्यावरणविदों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े संगठनांे और बुद्धिजीवियों के बीच एक अहम चिंतनीय मुद्दा बन गया है चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीप्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी. चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी. उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली अलकनंदा घाटी के मंडल गांव में लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया था. 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी. वनों को इस तरह कटते देख स्थानीय लोगों खासकर महिलाओं ने इसका विरोध किया. इस तरह चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई. इस आंदोलन को 1980 में तब बड़ी जीत मिली, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्ष के लिए रोक लगा दी. बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य में विंध्य तक फैला था.उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रंगथरा-मजगांव-चौनाला मोटर मार्ग निर्माण में आ रहे पेड़ों को बचाने के लिए सेरी के बाद अब जाखनी की महिलाएं भी आगे आई हैं. महिलाओं ने चिपको की तर्ज पर आंदोलन शुरू कर दिया है. यहां की महिलाएं बांज और बुरांश के पेड़ों से लिपट गई हैं. महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि देवी को चढ़ाए गए जंगल की बलि सड़क निर्माण में नहीं दी जाएगी महिलाओं ने बारे में आरोप लगाया कि वन विभाग ने सर्वे गलत किया है. उनके सर्वे में सड़क निर्माण में कुछ ही पेड़ आ रहे हैं. जबकि उनका हरा-भरा जंगल निर्माण में आ रहा है. पेड़ कटते ही उनके गांव में पानी का भी संकट गहरा जाएगा. मजगांव के लिए सड़क कट चुकी है. अब यहां से आगे निर्माण को सहन नहीं किया जाएगा. जंगल भगवती को चढ़ाया गया है. इस जंगल से वह खुद चारापत्ती आदि नहीं काटते हैं. ऐसे में जंगल में निर्माण कार्य नहीं होने देंगे करीब 300 पेड़ सड़क निर्माण की जद में आ रहे हैं. इन पेड़ों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है. अपने जंगल को उन्होंने देवी को समर्पित किया है. इस जंगल से वो चारा तक नहीं लाते. सड़क निर्माण के लिए वो अपने जंगल की बलि नहीं चढ़ने देंगी. चिपको आंदोलन’ की तर्ज पर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है. यहां की महिलाएं बांज और बुरांश के पेड़ों से लिपट गई हैं. उन्होंने अपने बेटे-बेटियों की तरह इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है. चौड़ी पत्तीदार पेड़ों से गांव के प्राकृतिक जल स्रोत सुरक्षित और संरक्षित हैं। अगर पेड़ काटे गए तो पानी स्रोत नष्ट हो जाएंगे। पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। चौड़ी पत्तीदार पेड़ों से गांव के प्राकृतिक जल स्रोत सुरक्षित और संरक्षित हैं। अगर पेड़ काटे गए तो पानी स्रोत नष्ट हो जाएंगे। पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी संरक्षित होता जाएगा। वहीं आनंद जैन ने बताया कि आज शहरों में आक्सीजन खरीदा जा रहा है और गांव में यह स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम जंगलों की, पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आएं। चिपको आन्दोलन’ के दौरान ये नारा भी बहुत मशहूर हुआ था. 48 साल पहले जंगल माफियाओं से वनों को बचाने को लेकर इस गांव ने सुर्खियां स्टोरी थीं. तब गांव की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में जंगल बचाने के लिए संघर्ष किया था. चिपको आंदोलन चलाया था. ये महिलाएं पर्यावरण की बर्बादी रोकना चाहती थीं
क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।
पहाड़ी राज्यों में नीतियां दिल्ली या उत्तर प्रदेश के समान नहीं हो सकती हैं। विकास को स्थानीय वास्तविकताओं और सीखों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यहीं पर चिपको आंदोलन की विचारधारा और कार्य अमूल्य प्रतीत होते हैं। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपने और भावी पीढ़ी के अस्तित्व की खातिर आगे आना होगा। चिपको आंदोलन की तरह देश-दुनिया में पर्यावरण बचाने के लिए किए गए प्रयासों का अनुसरण करना होगा। हरित सोच और प्रकृति की अमूल्य धरोहरों को संजोकर पहाड़ी राज्यों में इन्हें जीविका और विकास मंत्र बनाया जा सकता है। तब यह निश्चित रूप से हिमालयी राज्यों के हित में सबसे समझदार बात होगी। हिमालयी राज्यों में रहने वाले लोगों के प्रति न्याय हित इसकी सीमाएं समझते हुए नीतियां बनानी होंगी। पहले तो हमें इसके आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा, ना कि खास आदमी के ऐशो-आराम को। दूसरा इसके प्राकृतिक संसाधनों पर उतना ही बोझ डालना होगा जितना ये सह पाएं। हमारे जल-जंगल-जमीन हमारी विरासत हैं जिन्हें हमें संजोए रखकर अगली पीढ़ी को सौंपना होगा। देश और प्रदेश की सरकारों को अपनी हर नीति को दो कसौटियां पर कसने की जरूरत है। पहली कसौटी कि नई नीति कितने आम लोगों का भला कर पाएगी और दूसरी कि हमारे कुदरती संसाधनो पर कितना दबाव पड़ रहा है। जिस दिन हमारी सरकारें जनता की जरूरत और संसाधनों के इस्तेमाल के बीच स्थायी संतुलन बनाना सीख लेंगी उस दिन नीतियां जरूर कामयाब होगी। नीति निर्धारकों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता और कड़े प्राविधानों को अमल में लाना होगा। हर देशवासी और प्रदेश के लोगों को अपने पेड़ों, जंगलों, जल और जमीन को नए सिरे से सर माथे से लगाना होगा, उनसे फिर से चिपकना हो। हरित सोच से ही हरियाली बचेगी और पर्यावरण बचाने की दिशा में किए गए हर एक देशवासी के प्रयास दुनियाभर में मिसाल कायम करेंगे।
*लेखक उत्तराखण्ड सरकार के अधीन उद्यान विभाग के वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर चुके हैं वर्तमान में दून विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।*