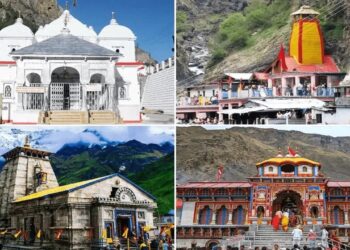डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं।
कभी ज्यादा बारिश हो रही है तो कभी सूखे से फसलों पर असर पड़
रहा है। लगातार बढ़ते तापमान से गेहूं चावल जैसी फसलों पर खतरा
मंडरा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि मिलेट्स आने वाले
समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते
हैं। आज देश में मिलेट्स पर शोध बढ़ाए जाने के साथ ही किसानों को
ज्यादा से ज्यादा अच्छे बीज उपलब्ध कराने की जरूरत है। पिछले कुछ
समय में जागरूकता बढ़ने के साथ ही लोगों में मिलेट्स की मांग भी
तेजी से बढ़ी है।बढ़ते तापमान, ज्यादा बारिश और बदलते मौसम के
चलते कई फसलों के उत्पादन में कमी आई है। भारत में कृषि क्षेत्र
जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। उच्च तापमान फसल की पैदावार को
कम करते हैं और खरपतवार और कीट पतंगों को बढ़ाते हैं। तापमान में
वृद्धि और पानी की उपलब्धता में कमी के कारण जलवायु परिवर्तन
सिंचित फसलों की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक 2030 तक पूरी दुनिया में लगभग 8.5
बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा
सुनिश्चित करनी होगी। बदलते मौसम के बीच आम लोगों को उचित
पोषण उपलब्ध कराने में मिलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
पूरी दुनिया में मिलेट्स के लिए जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत
है।फसलों, खास तौर पर शुष्क मौसम में उगाई जाने वाली फसलों पर
शोध करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी
मिलेट के एक पौधे की तुलना में धान के एक पौधे को उगाने में लगभग
2.5 गुना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। गेहूं और धान का पौधा
जहां 38 डिग्री तक का तापमान बरदाश्त कर पाता है, वहीं मिलेट्स का
पौधा 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बरदाश्त कर लेता है। यही
कारण है कि मिलेट्स की ज्यादातर खेती एशिया, अफ्रीका और लेटिन
अमेरिका के देशों में की जा रही है।भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च बुलेटिन
में प्रकाशित एक अध्ययन में एक गंभीर चिंता जताई गई है, जो देश में
वर्षा के वितरण में तेजी से आ रहे बदलाव और खाद्यान्न फसलों पर
इसके असर से जुड़ी है। अध्ययन कहता है कि भारतीय कृषि अब भी
काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं के
विस्तार और जलवायु परिवर्तन से बेअसर रहने वाले नई किस्मों के
बीज तैयार होने से राहत तो मिली है मगर मॉनसूनी बारिश अब भी
निर्णायक होती है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा
खरीफ सत्र में कृषि उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।वर्षा का तरीका
बदलने या सूखे जैसी स्थिति से फसल उगाने का चक्र बिगड़ जाता है
और कीटों एवं पौधों से जुड़ी बीमारियों की समस्या भी बढ़ जाती है।
पर्याप्त और समान वर्षा होने से कृषि उत्पादकता बढ़ जाती है। मॉनसून
में अच्छी बारिश रबी सत्र के अनुकूल होती है। मिट्टी में पर्याप्त नमी
रहने और जलाशयों में पानी का स्तर अधिक रहने से गेहूं, सरसों और
दलहन जैसी फसलों की बोआई के लिए आदर्श स्थिति तैयार होती
है।खरीफ सत्र में मोटे अनाज, तिलहन, दलहन और चावल की उपज में
सालाना वृद्धि के आंकड़े देखें तो जिस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सभी
फसलों के लिए बेहतर रहा उस साल उत्पादन भी ज्यादा रहा। लेकिन
अतिवृष्टि ने मक्के और तिलहन की उपज बिगाड़ी। अध्ययन में कहा गया
है कि उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मॉनसूनी बारिश
कब आती है। उदाहरण के लिए जून और जुलाई में कम बारिश मक्का,
दलहन और सोयाबीन के लिए खास तौर पर नुकसानदेह होती है
क्योंकि मिट्टी में नमी कम होने के कारण बोआई अटक जाती है और
पौधों की शुरुआती बढ़वार पर भी असर पड़ता है।इसी तरह कटाई के
समय अत्यधिक वर्षा से तिलहन उत्पादन घट जाता है। पिछले साल
मॉनसून में शानदार वर्षा और सटीक ठंड रहने से चालू वित्त वर्ष में
फसलों का उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि पिछले
साल के मुकाबले खरीफ का उत्पादन 7.9 प्रतिशत और रबी का 6
प्रतिशत बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 2025 के लिए
मॉनसून के अनुमान जारी नहीं किए हैं मगर विश्व मौसम विज्ञान
संगठन का अनुमान है कि भारत में इस साल वर्षा सामान्य या इससे
अधिक हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन के कारण
बारिश के पैटर्न में आने वाले बदलाव कृषि उत्पादन पर ज्यादा असर
डाल सकते हैं। मौसम की अतिरंजना अब अनोखी बात नहीं रह गई है।
भारत में पिछले साल 365 में से 322 दिन मौसम की अति दिखी थी।
इससे देश में 4.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें प्रभावित हुईं।
2023 में 318 दिन मौसम ऐसा रहा था। जब तक इन प्रतिकूल
परिस्थितियों से निपटने के लिए बहु-आयामी नीति नहीं अपनाई जाती
है तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती ही रहेंगी।पिछले साल कम और असमान
वर्षा के कारण गर्म हवा और बाढ़ की 250 घटनाएं सामने आईं।
जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान और बाढ़ के कारण
फसलों का उत्पादन घटने और इनमें पोषक तत्व कम होने का खतरा
बढ़ता जा रहा है। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए जलवायु के
अनुकूल कृषि कार्यों की तरफ कदम बढ़ाना आवश्यक हो गया है। कृषि
में जलवायु परिवर्तन सहने की क्षमता रखने तौर-तरीके, नालियों की
प्रणाली में सुधार, बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन और तकनीक अपनाकर कृषि
क्षेत्र में क्षमता एवं टिकाऊपन बढ़ाया जा सकता है।लंबे अरसे के लिए
जल प्रबंधन पर भी हमें सतर्क रहना होगा। जैविक या रसायन रहित
कृषि के बजाय प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना होगा। इससे अलग-
अलग मियाद वाली विविध फसलों से किसानों की आय ही नहीं बढ़ती
बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर भारत को जलवायु
परिवर्तन का प्रभाव कम करने और अनुकूल रणनीति अपनाने के लिए
काम करना होगा। मिलेट्स, जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं, भारतीय
कृषि और आहार परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। बदलती जीवनशैली
के कारण इनका उपयोग घट गया है, लेकिन इनकी पोषण क्षमता को
देखते हुए इन्हें फिर से मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। इस
प्रकार के आयोजन न केवल छात्राओं को इनकी उपयोगिता समझाते हैं
बल्कि समाज में इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम बनते हैं।"
मोटे अनाज न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि यह टिकाऊ
और पर्यावरण-अनुकूल कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. इससे किसानों
की आय भी बढ़ेगी. ऐसे में इसे खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए
वरदान कहा जा सकता है. बदलते समय में किसानों को पारंपरिक और
टिकाऊ खेती की ओर लौटने की जरूरत है. केंद्र और राज्य सरकारों के
सामूहिक प्रयास से मोटे अनाज की खेती को पुनः कृषि के मुख्यधारा में
लाना संभव है. सरकारी प्रोत्साहन और सामाजिक जागरूकता के साथ
यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मोटे अनाज का महत्व फिर से
स्थापित हो. यह कृषि और मानव स्वास्थ्य, दोनों ही दृष्टिकोण से
लाभदायक है *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून*
*विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*