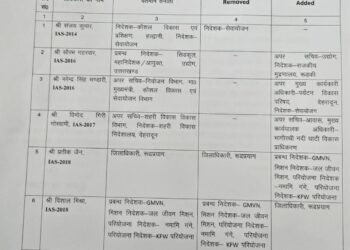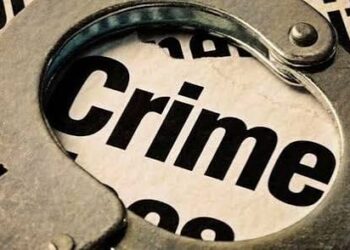डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न संस्कारों में गाए जाने वाले मांगलिक गीत जिन्हें मांगल भी कहा जाता है, देवभूमि की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान रहे हैं। इतना ही नहीं स्त्री शक्ति के प्रतीक भी माने जाने वाले मांगल गीत पौराणिक दौर से ही पहाड़ की सांस्कृतिक धरोहर भी रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके मांगल गीतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अब नये सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं, जिससे इनके अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट के बीच है। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं की विशिष्टताओं की वजह से देश.विदेश में अलग पहचान रखता है। इसी कड़ी में गढ़वाल-कुमाऊं में पौराणिक दौर से विभिन्न मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले मांगल गीत पहाड़ी संस्कृति की खास पहचान रहे हैं, लेकिन आधुनिक दौर में मांगल गीतों की जगह पहले आर्केस्ट्रा और फिर डीजे ने ले ली। यही कारण रहा कि विभिन्न शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले मांगल गीत लगभग लुप्त हो गए।
संस्कृतिकर्मी इसके पीछे विभिन्न कारणों को जिम्मेदार मानते हैंण् खास बात यह है कि मांगल गीतों को बचाने की इस कवायद में पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मांगल गीतों से रूबरू करवाने के साथ इन्हें हस्तांतरित भी कर रही है। पूर्व में भी युवतियां जब ब्याहकर अपने ससुराल जाती थीं, तो इस परम्परा को अपने ससुराल ले जाती थी। मांगल गीत प्रतियोगिता में पहुंची विवाहित महिलाएं, जहां मांगल के पुराने दौर को याद कर भावुक हो जाती हैं तो वहीं नई पीढ़ी की युवतियां इसे खुद के लिए महत्वपूर्ण बताती हैं। पहाड़ की बहुआयामी गौरवशाली संस्कृति की पहचान एवं धरोहर रहे मांगल गीत न केवल सगाई, शादियों में बल्कि पौधरोपण, भवन निर्माण, चूड़ाकर्म के साथ देवी.देवताओं की डोली यात्राओं का भी अहम हिस्सा रहे हैं। इनकी एक विशेषता ये भी रही है कि अलग.अलग क्षेत्रों में मांगल गीतों को गाने की शैली भी अलग.अलग रही है। मांगल गीतों को गाने के वक्त गाने और सुनने वालों की अनायास छलक जाने वाली आंखें एक तरफ इसके प्रभाव का उदाहरण हैं। बदलते परिवेश में मांगल गीतों की जगह डीजे और आधुनिक संगीत बजने लगा। लेकिन अब फिर से मांगल गीत शादी विवाह का हिस्सा बन रहे हैं।
शादी समारोह में सुमधुर सुर और साजबाज के साथ मांगल गीतो को गाती इन महिलाओं को देखकर आपकों कुछ सूकून सा मिलेगा। यह हमारी परंपरा रीति रिवाज है। लेकिन आपको बता दे कि ये महिलाये लगातार रियाज कर और बुजुर्ग महिलाओं से मांगल गीत सुनकर इसे व्यवसाय के रूप में भी अपना रही है। लोककलाओं पर काम करने वाली गौरांगना ग्रुप की प्रमुख सरिता भट्ट का कहना कि समय के सदपयोग और संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने अपनी मांगल टीम बनाई गई है। वही इसी ग्रुप की युवा कलाकार कहत हैं कि कैसेटों में बजने वाले मांगल गीत केवल रस्म अदायगी लगती है। मांगल गीत तभी सजते हैं जब महिलाएं इसे विवाह स्थल पर गाएं। और भी अच्छा है कि महिलाएं पूरा श्रंगार करके इन मागलों को गाए। इसलिए हम मांगल गीतों को गाने वाली महिलाओं की टीम बन रही है। और यह आय का भी जरिया बन रहे है। शादी और शुभ कार्यो में मांगल गीतों को बहुत शुभकारी माना जाता है। अब उत्तराखंडी समाज अपने पुरानी संस्कृति व विरासतों की ओर बढता दिखाई दे रहा है। भले ही वह आधुनिक तरीके और व्यवसायिक तरीके से इन सब चीजों को अपना रहा हो।
मांगल गीत आयोजकों को भी खूब भा रहे है और शादी समारोह में इन मांगल गीतों की टोली का प्रचलन भी चल पडा है। सुधा भण्डारी व अनिरूध भण्डारी का कहना है कि हमें यह परम्परा बहुत अच्छी लगी। हमने इसलिए मांगल गीतों को कार्यक्रम रखा ताकि हमारी आने वाली पीडी भी अपने लोकपरम्पराओं व संस्कति से रूबरू हो सकें।मांगल गीत शुभ और सुंदर हैं। मांगल गीतों की धुन बहुत मधुर है। बहुत अच्छा है कि मांगलगीतों की परंपरा फिर लौटती दिख रही है। शादी विवाह के शुभ अवसरों पर मांगल गीत गाती महिलाओं की टोलियां अब नजर आने लगी है। अच्छा यह भी है कि इसे परंपरा के साथ साथ यह आय का जरिया भी बन रहा है। जरूरत इस बात की है कि गांव से शहरों में आये उत्तराखंडियों को अपनी परम्पराओं व संस्कृति संरक्षण के लिए खुले मन से आगे आये ताकि युवा पीढी उससे जुड़ सके।तो इसके संरक्षण.संवर्द्धन की कवायद एक सराहनीय कदम हैण् जागरए मांगलए पुरोहित और तीलू रौतेली पेंशन योजनाएं सिर्फ नाम के लिए रह गई हैं। ढाई वर्ष में एक भी आवेदन इन योजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग के पास नहीं पहुंचा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले पहले से बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन योजना में कवर हो चुके हैं। विभाग की ओर से पुरोहित पेंशन योजना शुरू करते समय भी परेशानी हुई थी। दरअसल कैटेगिरी में कौन पुरोहित शामिल होंगे, यह क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि, इस पर पंडितों की राय भी ली गई थी। योजना के लिए जब कोई आवेदन ही नहीं मिला तो विभाग ने इस पर ज्यादा कसरत नहीं की। आवेदन नहीं आने की वजह से ये योजनाएं शुरू नहीं हो पाईं।
अब उत्तराखंडी समाज अपने पुरानी संस्कृति व विरासतों की ओर बढता दिखाई दे रहा है। भले ही वह आधुनिक और व्यवसायिक तरीके से इन सब चीजों को अपना रहे है। मांगल गीत आयोजकों को भी खूब भा रहे है और शादी समारोह में इन मांगल गीतों की टोलीयों का प्रचलन भी चल पडा है। आयोजको का कहना है कि हमें यह परम्परा बहुत अच्छी लगी हमने इसलिए मांगल गीतों को कार्यक्रम रखा है ताकि हमारी आने वाली पीडी भी अपने लोकपरम्पराओं व अपनी संस्कति से रूबरू हो सकें। भले ही उत्तराखंड में पलायन की मार से लोकसंस्कृति व परम्पराओं के पुराने स्वरूप को खोता जा रहा हो लेकिन इन लोक परम्पराओं को समय के अनुसार अब नये अवतार में देखना एक सुखद अहसास है। पुराने समय में महिलाओं द्वारा शुभ कार्यो में गये जाने वाले मांगल गीतों ने अब व्यवसाय का रूप ले लिया है, जिससे लोककलाकरों की आय के साथ.साथ सांस्कृतिक विरासतों का भी संरक्षण व सवर्धन हो रहा है। अपनी परंपरा से दूर होने वाला शख्स का समाज में भी कोई महत्व नहीं रहता। ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड के लोगों ने अपनी परंपराओं को अपने भीतर जीवित रखा है। त्यौहार, खुशी, पर्वों में ये परंपरा स्वाभाविक रूप से झलकती भी है। इसी परंपरा का एक सबसे बेहतरीन रूप है मांगल गीत। मांगल गीत यानी खुशी के गीत, देवताओं के आह्वान के गीत, दुनिया को राज़ी खुशी रखने की कामना करने वाले गीत। मांगल निर्विवाद रूप से उत्तराखंड के संगीत की आत्मा है। इसे जो भी एक बार सुन लेए वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि गांव से शहरों में आये उत्तराखंडियों को अपनी परम्पराओं व संस्कृति संरक्षण के लिए खुले मन से आगे आये ताकि युवा पीड़ी अपनी जड़ों को न भूल सकें।