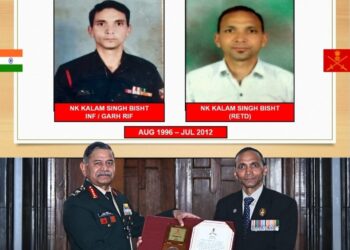डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला दून विश्वविद्यालयए देहरादूनए उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार में मुख्य रूप से मसूर की खेती की जाती है। इसके अलावा बिहार के ताल क्षेत्रों में भी मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चना तथा मटर की अपेक्षा मसूर कम तापक्रम, सूखा एवं नमी के प्रति अधिक सहनशील है। दलहनी वर्ग में मसूर सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण फसल है। प्रचलित दालों में सर्वाधिक पौष्टिक होने के साथ.साथ इस दाल को खाने से पेट के विकार समाप्त हो जाते है यानि सेहत के लिए फायदेमंद है। मसूर के 100 ग्राम दाने में औसतन 25 ग्राम प्रोटीन, 1.3 ग्राम वसा, 60.8 ग्राण् कार्बोहाइड्रेट, 3.2 ग्राण् रेशा, 68 मिग्राण् कैल्शियम, 7 मिग्राण् लोहा, 0.21 मिग्रा राइबोफ्लोविन, 0.51 मिग्राण् थाइमिन तथा 4.8 मिग्राण् नियासिन पाया जाता है। अर्थात मानव जीवन के लिए आवश्यक बहुत से खनिज लवण और विटामिन्स से यह परिपूर्ण दाल है।
रोगियों के लिए मसूर की दाल अत्यन्त लाभप्रद मानी जाती है क्योकि यह अत्यंत पाचक है। दाल के अलावा मसूर का उपयोग विविध नमकीन और मिठाईयाँ बनाने में भी किया जाता है। इसका हरा व सूखा चारा जानवरों के लिए स्वादिष्ट व पौष्टिक होता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में गाँठे पाई जाती हैं, जिनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु वायुमण्डल की स्वतन्त्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि में करते है। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अतः फसल चक्र में इसे शामिल करने से दूसरी फसलों के पोषक तत्वों की भी कुछ प्रतिपूर्ति करती है। इसके अलावा भूमि क्षरण को रोकने के लिए मसूर को आवरण फसल के रूप में भी उगाया जाता है। मसूर की खेती कम वर्षा और विपरीत परस्थितिओं वाली जलवायु में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। मसूर एक दलहन है। इसका वानस्पतिक नाम है। इसकी प्रकृति गर्म, शुष्क, रक्तवर्द्धक एवं रक्त में गाढ़ापन लाने वाली होती है। दस्त, बहुमूत्र, प्रदर, कब्ज व अनियमित पाचन क्रिया में मसूर की दाल का सेवन लाभकारी होता है।
मसूर एक प्रमुख फसल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत उत्तराखंड के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को इसी माह से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सस्ती दरों पर मसूर दाल मिलेगी। सरकार ने मसूर दाल के रेट 50 रुपये प्रति किलोण् तय किया है। इसमें सरकार आठ रुपये की सब्सिडी देगी। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दालें वितरित करने के लिए 12 सितंबर को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना शुरू की गई थी। योजना में प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति माह दो प्रकार की दाल एक.एक किलो देने की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक कार्ड धारकों को 41 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दो किलो चना दाल ही दी जा रही थी। योजना में अब सरकार ने मसूर दाल के रेट निर्धारित कर दिए हैं। सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को 50 रुपये प्रति किलो की दर से मसूर दाल उपलब्ध होगी। जबकि बाजार में इस दाल की कीमत 65 से 70 रुपये प्रति किलो है। इस बार दलहन फसलों की रिकार्ड घरेलू पैदावार हुई है। चालू फसल वर्ष में दलहन फसलों की पैदावार 2.40 करोड़ टन तक होने का अनुमान है, जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है दालों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। पैदावार ज्यादा होने के कारण ही घरेलू बाजार में दालों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे बनी हुई हैं। इसके बावजूद विदेशों से दालों का आयात अभी भी लगातार हो रहा है जबकि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई मात्रा पहले ही पूरी हो चुकी है, अप्रैल से अगस्त के दौरान 8.12 लाख टन आयातित दालें भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुकी हैं।
मसूर जैसी अन्य फसलों की बुवाई होगी। रोजगार के लिए पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है। लोग अपने गांव.खेत छोड़कर शहर जा रहे हैं। बंजर धरती पर उग आई झाड़ियां और पलायन कर चुके गांवों में वन्य जीवों की हलचल बढ़ती जा रही है। राज्य में कृषि क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वर्ष 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तराखंड की स्थापना के समय कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेअर था, वर्ष 2019 तक ये घटकर 6.91 लाख हेक्टेअर रह गया है। राज्य में जोत का औसत आकार 0.89 हेक्टेअर है। केवल 50 फीसदी खेतों में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 13 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 94 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र की बजट में हिस्सेदारी औसतन 3.80 प्रतिशत से 3.63 प्रतिशत के बीच रहती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। वर्ष 2011.12 में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018.19 में 4.67 प्रतिशत के आसपास आ गई। कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र का राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 0.70 प्रतिशत है। सरकार ने सूबे में दलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दलहन बीज उत्पादन के लिए में केन्द्र हब बनाने का निर्णय लिया है। बीज हब से मसूर, मूंग, चना, मटर के बीच का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढाया जाएगा। इन हबों के जरिए न सिर्फ बीज बल्कि बीज का उत्पादन करने वाले किसानों की उपज को बीज के रूप में खरीददारी सुनिश्चित करने का इंतजाम भी सरकार करेगी। किसानों को उनके द्वारा तैयार किये गये बीज की कीमत बाजार भाव से 15 से 20 प्रतिशत अधिक दिया जाएगा। देखना होगा इस व इन जैसे दूसरे उपायों से सूबे में लुप्त होते दाल को बचाया जा सकता है या नहीं मसूर की दाल पहाड़ो में रवि की मुख्य फसल है। इस दाल को आप आसानी से पका सकते हैं।
पहले जब प्रेशर कुकर नहीं होते थे मिट्टी और पत्थर के चूल्हे होते थे, लकड़ी ही ईंधन होता था, उस जमाने में हल्की सी आंच में मसूर की दाल आसानी से पक जाती थी। और पचाने में भी आसान होती है। यह दाल विशेष रूप से छोटे दानों वाली है। रंग इसका काला होता है। इस दाल को कई तरह से बनाया जा सकता था उन्नत प्रजाति का चयन करना आवश्यक है। इसके साथ.साथ प्रजाति अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक पैदावार देने वाली तथा विकार रोधी होनी चाहिए। हमारे देश में मसूर की दो प्रकार की अनेक किस्मे उपलब्ध है। पहली छोटे दाने वाली और दूसरी बड़े दाने वाली एक प्रगतिशील किसान को इन सब की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वो प्रजाति का सही से चयन कर के मसूर की खेती से अपनी इच्छित पैदावार प्राप्त कर सके इस किस्म के पौधे की ऊचाई 25 से 30 सेंटीमीटर, पकने की अवधि 145 से 150 दिन, छोटा दाना और रंग भूरा, जड़ विगलन तथा झुलसा रोग के प्रति सहनशील, उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु अनुमोदित और उपज लगभग 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। क्योंकि यहां से पलायन की मार से पूरा उत्तराखंड प्रभावित है। इसमें एक मुख्य मुद्दा जमीन का सही तरीके से उपयोग न होना है। साथ ही बटी खेती ने ऐसा रास्ता भी नहीं छोड़ा, जहां लोग वापस घर की तरफ रुझान कर सकें। दिल्ली में उगे कंक्रीट के जंगल का दायरा उत्तराखंड की ओर भी तेजी से सरक रहा है। जिसने यहां जमीनी विवादों को और तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वक्त रहते यदि इसे पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में उत्तराखंड में जमीनी विवाद और बढ़ने से इंनकार नहीं किया जा सकता।