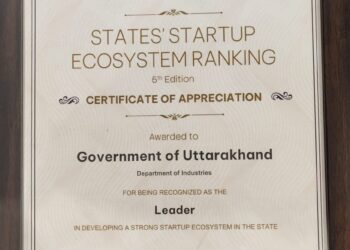डा. हरीश चंद्र अंडोला
उत्तराखंड को औषधि प्रदेश, यानी हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। यह बात दीगर है कि औषधीय वनस्पतियों के उत्पादन और मार्केटिंग को लेकर सरकार राज्य गठन के बाद से पिछले सालों में अब तक कोई सुस्पष्ट नीति अमल में नहीं ला पाई है। भारत की स्थानीय संस्कृति में कई चमत्कारिक कुछ ऐसे भी पौधे हैं च्यूरा मूलत नेपाल का पौधा है जो कि वहाँ से होते हुए भारत से फिलीपिंस तक पाया जाता है। भारत के गढ़वाल के कुमाऊँ क्षेत्र से पूरब की ओर सिक्किम तथा भूटान उप.हिमालयी दर्रों तह बाह्य हिमालयी घाटियों तक भी यह पाया जाता है। यह अंडमान द्वीप समूह के उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, पर्णपाती अर्ध. पर्णपाती तथा सदाबहार जंगलों में भी पाया जाता है।
यह एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष मूल तिलहन है जो कि मुख्यतः 400.1400 मीटर तक की ऊँचाई वाले दर्रों के किनारे तथा छायादार घाटियों में पाया जाता है इस तरह के पौधे व जड़ी.बूटियां और क्या आज भी पाए जाते हैं। डिप्लोक्नेमा ब्यूटरीसा, भारतीय मक्खन का पेड़, एक बहुउद्देश्यीय पेड़ है। पेड़ का मुख्य उत्पाद घी मक्खन होता है, जो बीज से निकाला जाता है और नामित चीउरी घी या फूलवाड़ा मक्खन होता है। डी। ब्यूटरीरा ब्लॉक रोपण के लिए उपयोगी है और पहाड़ियों की चट्टानों में भी उगाया जा सकता है। लेटेक्स उपज संयंत्र जैसे डी। ब्यूटरीसा विभिन्न जलवायु स्थितियों के लिए उपयुक्त है और इस प्रकार पारंपरिक फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। ठंड के मौसम के दौरान फूल और जून जुलाई में फल पकते हैं।
यह समुद्र तल से 300.1500 मीटर के बीच उप हिमालयी पथ में आमतौर पर होता है। नेपाल में ग्रामीण परिवारों द्वारा कई उपयोगों के लिए चिउरी पेड़ का उपयोग किया गया है। घी दैनिक खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, दीपक के लिए ईंधन, और शरीर लोशन, फल ताजा खाया जाता है और अल्कोहल आसवन के लिए उपयोग किया जाता है, तेल केक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, और पेड़ को स्वयं लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है, आदि। इसमें नेपाल के चेपांग समुदाय के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आजीविका संघ हैं। यद्यपि वाणिज्यिक रूप से खेती नहीं की जाती है। यह कुमाऊँ क्षेत्र में भोजन सामग्रीए पशु आहार तथा औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है और इसे कल्प दृवृक्ष भी कहा जाता है च्यूरा की पत्तियों का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है। च्यूरा की पत्तियों चौड़ी होती है अतः इनका उपयोग भोजन परोसना के लिए पत्तल दोने के रूप में किया जाता है। ऐसे पत्तल, बायो.डिग्रडेबल भी होते हैं जिनसे पर्यावरण.प्रदूषण नहीं होता है। सब्जियाँ व भोजन पकाने व तलने के लिए च्यूरा के तेल का उपयोग घी मक्खन में के रूप से असंतृप्त वसा अम्ल, पाल्मिटिक स्टीयरिक एसिड ओलेइक, लेनोलिक अम्ल भरपूर होता है यह फूलवारा घी के नाम से भी जाना जाता है। च्यूरा के मक्खन का उपयोग औषधि, मलहम, मोमबत्ती, क्रीम एवं अन्य ऐसे उपयोगी उत्पाद तैयार करने में किया जाता है च्यूरा के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त खली का प्रयोग खाद रूप में किया जाता है। इसमें कीटनाशक तत्व विद्यमान रहता है अतः इसका उपयोग कीटनाशक, गोलकृमि नाशक निमेटिसइड, चूहा नाशक रोडेन्टोसाइड आदि के तौर पर भी किया जाता है। खली को विनाशकारी रासायनिक कीटनाशकों की जगह क्रूड फ़ीस प्वायजन विष के तौर पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें सैपोनिन भी काफी मात्रा में पाया जाता है इसलिए यह, ऐसे उद्योग सैपोनिन का प्रयोग किया जाता है, कि लिए भविष्य में एक अच्छे स्रोत के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
च्यूरा के फूल में चीनी का अंश, प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है इसलिए इसे गुड तथा अल्कोहल देशी शराब बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। इसकी लकड़ी साधारण गृह.निर्माण में फर्नीचर बनाने में तथा जलावन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। स्थानीय समुदाय द्वारा च्यूरा के उप्तादों का उपयोग किया जाता और इनका उपयोग खासकर घरेलू उपभोग के लिए किया जाता हैद्य उन्हें च्यूरा के उत्पादों के बाजरा भाव की सही- सही जानकारी नहीं होती है। च्यूरा का फल जितना सूखा होता है उसी के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होता है। कच्चे फलों की तुलना में सूखे फलों की अधिक कीमत मिलती है। व्यापारियों को फसल तैयार होने के पहले ही फसल बेच दिया जाना आम बात है। व्यापारी, फसल बेचने वाले किसानों को आवश्यक्तानुसार किस्तों में इसकी कीमत अदा करता रहता है। उत्पादकों द्वारा अधिकतर तो सीधे ही व्यापारियों को उत्पाद, फसल बेच दिए जाते हैं इसलिए उन्हें फसल तैयार किए जाने वाले स्थानों से संग्रह केंद्र तक के किराए के खर्चे का वहन नहीं करना पड़ता है। व्यापारियों द्वारा 15.20 रूपए प्रति बैग की दर से पैकेजिंग का खर्च किया जाता है। सामान्यतः व्यपारियों द्वारा लगभग दो महीनों तक च्यूरा का भंडारण किया जाता है ताकि इसमें मौजूद नमी की मात्रा कम हो सके। खरीदने से पहले व्यापारियों द्वारा इस बात की ताकीद की जाती है कि च्यूरा अच्छी क्वालिटी का हो। च्यूरा के बड़े व मासल फल, अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में तो कुछ लोगों द्वारा दशकों से च्यूरा घी का उपभोग सामान्य घी के तौर पर किया जा रहा है। वे इसके उपभोग के अभ्यस्त हो चुके हैं।
च्यूरा की खेती की लागत व इससे प्राप्त होने वाली आमदनी च्यूरा के पौधारोपण तथा रख रखाव का खर्चए पौधारोपण के स्थानए निवेश की लागत, मजदूरी इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसके अनुसार प्रति हैक्टेयर लगभग 9000.10000ध्. रूपए की दर से खर्च होता है। 7.8 वर्षों के बाद इससे फल प्राप्त होना शूरू हो जाता है जिससे कि 50.60 वर्ष तक हरेक वैकल्पिक वर्षो में उपजध्फसल प्राप्त होती है। च्यूरा के बीज के बाजार भाव 10.15 रूपए किलो ग्राम तक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इससे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष लगभग 70,000 .1,20,000 रूपए तक की औसत आमदनी होती है। च्यूरा के पके हुए फलों, जो भूरे तथा हल्के पीले रंग वाले होते हैं, को हाथ से अथवा बांस के डंडे से तोड़ा जाता हैद्य इन फलों को 8.12 दिनों तक छायेदार स्थान पर रखकर सुखाया जाता है। प्रतिवर्ष औसतन 100.250 किलोग्राम प्रति पेड़ की दर से उपज प्राप्त होता है। उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। यह अपार संभावनाओं वाला एक बहूउद्देशीय पेड़ है जिसकी उपयोगिताओं के समुचित दोहन किए जाने की आवश्यकता है।
स्रोत- राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय, भारत सरकार