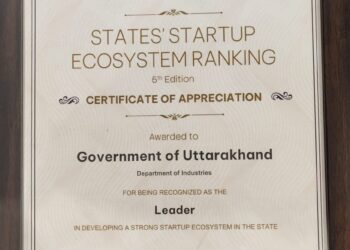डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
एक जमाने में पहाड़ के गांवों में परंपरागत धारे व नौलों का खास प्रचलन था। ग्रामीण पानी के लिए इन्हीं पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज पानी सूख जाने से अनेक धारे व नौले खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कई देखरेख के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कहीं-कहीं ऐसे नौले भी हैं जो गांवों में पेयजल योजनाएं बन जाने से प्रचलन में नहीं हैं।अस्सी के दशक से पूर्व यहां बाजार से लगे चांदीखेत गांव में तीन धारे व दो पारंपरिक नौले थे, जो पानी से लबालब भरे रहते थे। संपूर्ण गांव व बाजार की पेयजल आपूर्ति इन्हीं से होती थी। यहां तक कि इन धारों के पानी को सिंचाई के उपयोग में भी लाया जाता रहा, लेकिन अस्सी के दशक के बाद धारे व नौले सूखने लगे तथा वर्ष 1985 के आसपास दो धारे व दो नौले पूरी तरह सूख गए। वर्तमान में एक नौला तो खंडहर में तब्दील हो चुका है। जबकि दूसरे का आंशिक रूप से उपयोग हो रहा है। बांस का पुराना धारा भी सूखने के कगार पर है। इसमें इतना कम पानी रह गया है कि बमुश्किल आधे घंटे में एक बाल्टी भर पाती है। ऐसे में धारे नौलों का अस्तित्व खतरे में है।विज्ञान की नज़र से देखें तो नौले-धारे भूजल का एक रूप है जो प्रायः उच्च हिम क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से या वर्षा जल से रिचार्ज होते हैं। नौले- धारों में पानी आमतौर पर वर्षा द्वारा उत्पन्न जल को मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है और अंतर्निहित इन्ही संरचना को हम पहाड़ी नौले- धारों के रूप में देखते हैं। भूमि की आंतरिक संरचना में अनेक जलभृत पाएं जाते हैं जिन्हें हम सरल भाषा में भूमिगत जल टैंक एवं इन केशिकाओं को हम प्राकृतिक पाइपलाइन के रूप में समझ सकते हैं। बचपन से आप सुनते आए हैं, बूंद बूंद से बनता है सागर। बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। हर बूंद होती है अनमोल उसे संचय करने से ही बनते हैं, तालाब और समंदर। बूंद भले जल की हो या कोई और चीज़ की, सब अनमोल है। हर बूंद की कीमत है, विद्वान और गुणी ही इस कीमत की पहचान सकते और समझ सकते हैं। जल को ही ले लीजिए, बरसात होती है तो बूंदे गिरती है, इन्हीं से तालाब भरते हैं। तालाब तब भरते हैं, जब इनकी कीमत को समझा जाता है। कीमत को समझने का अभिप्राय तालाब बनाए जाते हैं और उनमें पानी के बहाव को लाया जाता है, इसी से सालभर पीने, नहाने और अन्य कामों के साथ कृषि कार्यो के लिए उपयोग में लिया जाता है। आधुनिक जल व्यवस्था और पाइपलाइन के दौर में वो पुराने कुएं जो कभी गांवों और शहरों की प्यास बुझाया करते थे, आज गुमनामी की धूल में दबे पड़े हैं. कहीं अतिक्रमण की चपेट में, कहीं उपेक्षा की वजह से बेजान, इन कुओं की हालत आज ऐसी हो गई है कि नई पीढ़ी ने तो कुओं को देखा भी नहीं होगा लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये कुएं फिर से बोलें, फिर से जीवनदायिनी बनें. मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में पुराने कुओं के पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार बरसात से पहले इन ऐतिहासिक जलस्रोतों की सफाई और मरम्मत कर इन्हें फिर से उपयोगी बनाने जा रही है.उत्तराखंड की धरती पर प्राचीनकाल से ही कुएं जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं. वे सिर्फ पानी के स्रोत नहीं बल्कि इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है. गांवों से लेकर शहरों तक हर स्थान पर कुएं धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह रहे हैं. हालांकि समय के साथ पानी की आपूर्ति की व्यवस्था बदलने से इनका उपयोग कम होता गया, जिससे कई कुएं उपेक्षित या अतिक्रमण का शिकार हो गए. अब उत्तराखंड सरकार ने इन कुओं की सुध लेने का फैसला किया है.मुख्यमंत्री ने दशकों पुराने कुओं के जीर्णोद्धार के लिए व्यापक सत्यापन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके बाद इन कुओं को फिर से साफ किया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी ताकि उन्हें फिर से उपयोग में लाया जा सके. सरकार ने बरसात से पहले इन कुओं की सफाई का भी निर्णय लिया है. यह अभियान मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कुओं की सफाई और रखरखाव किया जाएगा. बूंद-बूंद से घड़ा भरता है’ लेकिन अगर घड़ा ही गायब हो जाए तो पानी का क्या होगा? बूंद-बूंद का संचय ही सागर का रहस्य है। सागर या समंदर में जल को संचित किए जाने की शक्ति होती है। यह शक्ति उस जल को अपनी ओर खींचती है, जिसका संचय उचित तरीके से नहीं किया गया है। नदियों का बहता जल अपनी आखिरी मंजिल सागर में जा गिरता है। खेतों का बहता पानी नदी नाले में बह जाता है या फिर धरती की गहराई में समा जाता है। उचित व्यवस्था नहीं होने पर यह वाष्प बन उड़ जाता है। बिन संचय के इसकी कीमत सम्भव नहीं है। संचय तो बूंद-बूंद से ही होता है। जहां बूंद-बूंद का संचय नहीं होता वो ऊंची कीमत दे दूर से जल मंगवाते है। ऐसे ही धन का संचय भी बूंद-बूंद (रुपया-रुपया, पैसा-पैसा) से ही होता है। जिस बूंद का संचय नहीं किया गया वो आसपास के बड़े स्त्रोत (सेठ-साहूकार) की तिजोरी में उनके संचय के साथ जा मिलेगी। रुपये का बहाव भी जल की भांति ही है। दोनों में समानता है बिन संचय के ऐसी जगह जा गिरना जहां संचय सम्भव है। बुजुर्ग भी कहते हैं ‘रुपया, रुपये को खिंचता है’। रुपये में चुंबक की तरफ (सेठ-साहूकार) खिंचे जाने की शक्ति है, अधिक धन में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो आसपास की छोटी रकम को अपनी और खिंचता है। लेकिन छोटी रकम को मजबूती से पकड़ा रखा जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण व्यर्थ हो जाता है।संचय करने के लिए हर बूंद को उस तरफ बहाना होगा जहां भारी भरकम संचय करने वाली शक्ति की तरफ रुख ना हो। बहाव का रास्ता रोक उसकी दिशा में परिवर्तन कर अपने स्त्रोत की तरफ बहाव करना होगा। ऐसा रुपये में भी लागू होता है, उसके बहाव (खर्च) के रास्ते को समझ उस तरफ का बहाव रोकना होगा। किसी समय प्लस पोलियो अभियान भारत में जोर-शोर से चलता था। हर महीने घर-घर 0-5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाने का कार्य घर-घर पहुंच सरकारी कर्मचारी किया करते थे। उनके पास एक थैला होता था, प्लस पोलियो अभियान का, जिस पर लिखा हुआ होता था ‘दो बूंद जिंदगी की’। हालांकि वह टैग लाइन थी, प्लस पोलियो अभियान कि लेकिन जिंदगी की सच्चाई में यह कई जगह खरी उतरती है। जिंदगी की सच्चाई है, दो बूंद। बूंद-बूंद से सागर बनता है, इसी सागर से जल की आवश्यकता पूरी होती है। ऐसे ही व्यक्ति अपनी कुल आय से दो बूँद यानी थोड़ी से बचत करे तो यह उसे जिंदगी दे सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति या हारी-बीमारी में यह दो बूंद यानी अल्प बचत उसे साँसे देने में कामयाब हो सकती है। इस देश में प्रतिवर्ष हज़ारों नहीं बल्कि लाखो लोग ईलाज के अभाव में अपनी साँसे खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में ईलाज नहीं है, ईलाज है। लेकिन ईलाज के लिए रकम की आवश्यकता होती है, इस रकम के अभाव में ईलाज नहीं करा सकते हैं। अगर अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत के रुप में जमा करते जाए तो आसानी से ईलाज करा सकते हैं और अपनी साँस की डोर थमने से रोक सकते हैं। यानी समन्वित प्रयास से ही हम पानी जैसे बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण व संवर्धन कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में हमें महात्मा गाँधी की सीख याद रखनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि प्रकृति मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परन्तु लालच की नहीं। उत्तराखंड को इस गर्मी एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा. हालांकि प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, फिर भी नागरिकों की भूमिका भी अहम होगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों से अपने नौलों और धारों को संरक्षित करने की अपील की थी. मुख्यमंत्री ने इस अभियान को लेकर कहा कि कुएं हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा रहे हैं. हमारा प्रयास है कि इन पुराने कुओं को फिर से जीवित किया जाए ताकि जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिले और स्वच्छ जल के प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित किया जा सके. *लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*