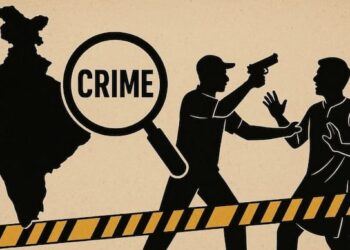डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
कटहल एक उष्णकटिबंधीय फल है जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। यह एक पेड़ पर उगने वाला सबसे बड़ा फल है और इसका एक खास स्वाद और बनावट है। भारत में कटहल की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है और यह देश के कई राज्यों में उगाया जाता है।हमारे देश में इस समय लगभग 11 प्रतिशत जनसंख्या डायबिटीज और लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या प्री डायबिटिक है। ऐसे में कटहल का सेवन करने की भी सलाह दी जाती है। वजह है कटहल के अंदर डायबिटीज रोग को प्रबंधित करने की क्षमता। जैसे -जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं कटहल के प्रोडक्ट का उपयोग डायबिटीज प्रबंधन में कर रहे हैं।कटहल उष्णकटिबंधीय जलवायु में 25 से 35°C (77-95°F) की तापमान सीमा के साथ पनपता है। इसके लिए हर साल 1500-2500 मिमी की अच्छी तरह से वितरित बारिश की ज़रूरत होती है। इसे तटीय क्षेत्रों, मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। एक पेड़ से 100 क्विंटल से अधिक कटहल की पैदावार हो सकती है तो आपको असंभव लगेगा. लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के गौलापार के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा ने यह कर दिखाया है. कटहल उत्पादन अब नरेंद्र सिंह की आर्थिकी का साधन बन गया है और उनके कटहल की मार्केट में भारी मांग रहती है. नरेंद्र मेहरा का कहना है कि किसानों के लिए कटहल की खेती को काफी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इससे सालों साल मोटी कमाई हो सकती है. कटहल का पौधा लगाने के बाद किसानों को इसका 2 से 4 साल तक रखरखाव और मेंटेनेंस करना होता है. जिसके बाद फल आना शुरू हो जाता है और अच्छी कमाई होती है. इसके लिए ना तो किसानों को दवाई की आवश्यकता होती है और ना ही किसी मेंटेनेंस की. साथ ही मौसम परिवर्तन या फिर आंधी तूफान का भी कोई असर नहीं होता है. उत्तराखंड के अनेक युवा आज कृषि से संबंधित स्वरोजगार में काफी अच्छे स्तर पर कार्य कर रहे हैं । इनमें ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप में कुछ नया रिकॉर्ड बना कर सभी के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हल्द्वानी के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा की ,जिसने कृषि क्षेत्र में एक और नयी उपलब्धि हासिल कर ली है आम तौर पर घर आए मेहमान को कुछ न कुछ देने का रिवाज है। हर कोई अपनी सामथ्र्य के अनुसार जाते समय मेहमान को मान-सम्मान स्वरूप भेंट देता है। अब समय जैविक उत्पादों का है। लिहाजा एक किसान ने घर आए मेहमान को उपहार स्वरूप जैविक उत्पाद देना शुरू कर दिया है। उसका मकसद जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों को जैविक खान-पान के लिए प्रेरित करना है। नरेंद्र सिंह मेहरा का जन्म 1959 में उत्तराखंड के नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कृषि गांव देवला मल्ला में हुआ था। हालाँकि उनका परिवार खेती करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वे एक अलग रास्ता अपनाएँगे। मेहरा ने भूगोल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उसके बाद कला में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए) और पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा किया। हालाँकि, अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद, उनका दिल अपनी मातृभूमि की मिट्टी से जुड़ा रहा।1984 में, सबको चौंकाते हुए, नरेंद्र अपने गांव लौट आए और पूर्णकालिक किसान बन गए। शुरुआत में, ज़्यादातर किसानों की तरह, उन्होंने पैदावार बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। लेकिन समय के साथ, उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता, फसल की पैदावार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने मुनाफ़े में नाटकीय गिरावट देखी। तब उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया – जो परंपरा और स्थिरता पर आधारित था। नरेंद्र हाल ही में कृषि जागरण की पहल, “ग्लोबल फ़ार्मर बिज़नेस नेटवर्क” का हिस्सा बने, जिसने अपने काम को एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया जो पूरे भारत से टिकाऊ कृषि उद्यमिता मॉडल को प्रदर्शित करता है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद नरेंद्र अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं और खेती-किसानी के प्रति समर्पित हैं। वे गांवों और कृषि मेलों में जाकर युवा किसानों को पारंपरिक ज्ञान, देशी बीज और रसायन मुक्त तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।जब बच्चों से किसान का चित्र बनाने को कहा जाता है, तो वे आम तौर पर फटे-पुराने कपड़े पहने एक उदास आदमी का चित्र बनाते हैं। मैं उस चित्र को बदलना चाहता हूँ। वह घोषणा करता है, “मैं चाहता हूँ कि हमारे किसानों को गर्वित, सफल और सम्मानित लोगों के रूप में देखा जाए।नरेंद्र सिंह मेहरा की यात्रा कृषि में जुनून, नवाचार और संधारणीय प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक, जलवायु-अनुकूल समाधानों के साथ मिलाकर, उन्होंने न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की है, बल्कि भारतीय किसानों के लिए अधिक संधारणीय, लाभदायक भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उनका काम उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है जो कृषि पद्धतियों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि दृढ़ता और सही ज्ञान के साथ, किसान प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं और एक हरियाली भरे, अधिक समृद्ध कल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के गौलापार के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा ने यह कर दिखाया है. कटहल उत्पादन अब नरेंद्र सिंह की आर्थिकी का साधन बन गया है और उनके कटहल की मार्केट में भारी मांग रहती है. किसानों के लिए कटहल की खेती को काफी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इससे सालों साल मोटी कमाई हो सकती है. कटहल का पौधा लगाने के बाद किसानों को इसका 2 से 4 साल तक रखरखाव और मेंटेनेंस करना होता है. जिसके बाद फल आना शुरू हो जाता है और अच्छी कमाई होती है. इसके लिए ना तो किसानों को दवाई की आवश्यकता होती है और ना ही किसी मेंटेनेंस की. साथ ही मौसम परिवर्तन या फिर आंधी तूफान का भी कोई असर नहीं होता है. कटहल का पौधा लगने के लगभग 5 सालों बाद फल देना शुरू कर देता है. शुरुआत में इसका पौधा 200 से 300 किलोग्राम तक उत्पादन देता है. लेकिन 10 वर्ष पुराना होने के बाद उसके फल देने की क्षमता लगातार बढ़ती जाती है और इसका एक पेड़ लगभग 500 से 600 किलो तक फल का उत्पादन कर सकता है. कटहल एक बहुमुखी फल है जिसके कई उपयोग हैं। पके फल को ताजा खाया जा सकता है या विभिन्न पाक तैयारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे डेसर्ट, करी और जैम। कच्चे या हरे कटहल का उपयोग अक्सर स्वादिष्ट व्यंजनों में सब्जी के रूप में किया जाता है और इसकी बनावट के कारण यह मांस के विकल्प के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। कटहल के बीज भी खाने योग्य होते हैं और इन्हें भूना या उबाला जा सकता है।भारत में कटहल की खेती कई किसानों के लिए आजीविका के मौके देती है और देश की कृषि विविधता में योगदान करती है। फल का पोषण मूल्य और बहुमुखी प्रतिभा इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ती माँग के साथ एक मूल्यवान फसल बनाती है। दरअसल, कटहल की खेती के प्रति लोगों का रुझान इस लिहाज से भी बढ़ा है कि इसके पौधों को जंगली जानवर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जबकि सब्जी की फसल एवं दूसरे खाने वाले फलों के पेड़ों को नीलगाय एवं सूअर आसानी से क्षति पहुंचा देते है। सभी दृष्टिकोण से कटहल का पेड़ लगाना आमदनी की दृष्टिकोण से किसानों के लिए एक अच्छा जरिया बन गया है। नरेंद्र मेहरा का यह प्रयास किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इससे न केवल उनकी इनपुट लागत कम होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है. जैविक खाद के उपयोग से फसलों की पैदावार भी अधिक होती है और खेती में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है. नरेंद्र मेहरा की यह पहल आने वाले समय में जैविक खेती को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी. यदि बाकी किसान भी इस तकनीक को अपनाते हैं, तो इससे खेती की लागत कम होगी, मिट्टी उपजाऊ बनेगी, और पर्यावरण संतुलित रहेगा. उनका यह प्रयास साबित करता है कि यदि सही तकनीक और जागरूकता के साथ खेती की जाए, तो यह न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकती है. नरेंद्र मेहरा जैविक खेती में एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जो किसानों को नए और टिकाऊ तरीकों की ओर प्रेरित कर रहे हैं. नरेंद्र सिंह मेहरा का जैविक खेती में योगदान न केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित है बल्कि यह उनके समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। उनके नवाचार, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, और किसानों को प्रेरित करने की कोशिशों ने उन्हें जैविक में एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया है। उनका प्रयास एक सच्ची मिसाल है कि खेती केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सेवा है जो समाज को पोषित करती है और पर्यावरण की रक्षा करती है। उनकी इस यात्रा ने साबित किया है कि जैविक खेती में न केवल आर्थिक लाभ है बल्कि यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामुदायिक उन्नति का सशक्त माध्यम भी है। सिस्टम के बजाय समुदायिक भागीदारी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। कई राज्यों में पके हुए कटहल को फल के रूप में लोग खाते हैं. विदेशों में भी अब कटहल की अच्छी खासी डिमांड रहने लगी है. ऐसे में अगर किसान कटहल की खेती करें तो नकदी फसल के तौर पर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*