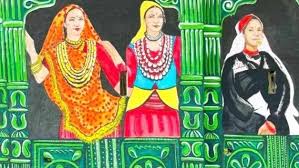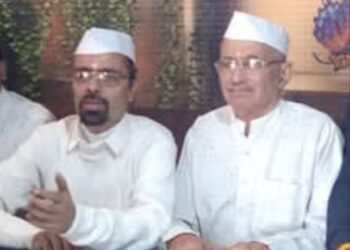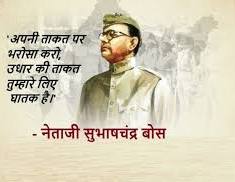डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, भारत का एक ऐसा राज्य है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का गहरा संबंध प्रकृति और उसके रहस्यमय रूपों से जुड़ा हुआ है। इस प्रदेश में प्रकृति की सुंदरता के साथ-साथ उसकी भयावहता भी एक साथ पाई जाती है। यहीं से उत्तराखंड के लोक देवताओं की उत्पत्ति हुई है। ये देवता न केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी अपनी संस्कृति, जमीन और प्रकृति पर गर्व करने वाले पहाड़ के लोग आज विकास और रोजगार के नाम पर अपनी ही पहचान का सौदा कर रहे हैं। शहरों से आने वाले धनाड्य लोग, रिसॉर्ट और होटल खड़े करने के लिए पहाड़ी जमीन खरीद रहे हैं। इसके बदले में स्थानीय लोग कुछ पैसों के लालच में अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ रहे हैं और धीरे-धीरे अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं।स्थानीयों का कहना है कि जो लोग कभी इन पहाड़ों के मालिक थे, अब उन्हीं के नौकर बनते जा रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा भी अब साफ दिखने लगा है आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाज़ा पहाड़ के लोग ही भुगत रहे हैं।पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई और पहाड़ों की खुदाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाले समय में गांव-गांव खाली हो जाएंगे, जलस्रोत सूख जाएंगे और पहाड़ केवल कंक्रीट के जंगल में बदल जाएंगे।शहरों में रह चुके लोग अब शांति के नाम पर पहाड़ों में बसने लगे हैं, लेकिन वे यहां भी अपनी शहरी आदतें और ढांचा लेकर आ रहे हैंजिससे न केवल स्थानीय संस्कृति बल्कि पूरा पर्यावरण खतरे में है। अब भी वक्त है अपनी भूमि, अपनी धरोहर और अपनी पहचान को बचाने का।वरना, कुदरत के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, और जब पहाड़ ही नहीं बचेंगे, तब इस पछतावे का कोई मतलब नहीं होगा। उत्तराखंड की पहचान उसकी लोकसंस्कृति, परंपराओं और लोकगीतों में बसती है। जागर, पांडव नृत्य, बग्वाल और रामलीला जैसे सांस्कृतिक आयोजन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि इस भूमि के गौरवशाली अतीत का जीवंत दस्तावेज हैं। यहां के मंदिर—केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, नैनी देवी—सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं।गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाएं केवल बोलियां नहीं, बल्कि इस राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, इन पर भी बाहरी प्रभाव और आधुनिकता का ऐसा दबाव बढ़ रहा है कि नई पीढ़ी अपनी ही भाषा से दूर होती जा रही है। उत्तराखंड आज एक नए संकट से जूझ रहा है—बाहरी पूंजीवादी ताकतों का अतिक्रमण। कुछ वर्षों से यहां की भूमि को केवल एक “रियल एस्टेट हब” के रूप में देखा जाने लगा है। बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यापारी यहां की जमीनें खरीद रहे हैं, उन्हें महंगे रिसॉर्ट्स और होटलों में बदल रहे हैं। यह न केवल पारंपरिक जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को उनके ही गांवों से विस्थापित कर रहा है।जनसंख्या संतुलन में अनियंत्रित बदलाव केवल सांस्कृतिक संकट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। चीन और नेपाल की सीमाओं से सटे इस राज्य में यदि बाहरी लोगों की अनियंत्रित बसावट होती रही, तो यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन रहा है। पारंपरिक कृषि प्रणाली यहां की जलवायु और पारिस्थितिकी के अनुरूप विकसित हुई है। मंडुवा, झिंगोरा, चौलाई, लाल चावल जैसे मोटे अनाज न केवल पोषण का स्रोत हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में भी सक्षम हैं।लेकिन हाल के वर्षों में कृषि को दरकिनार किया जा रहा है। पहाड़ों से पलायन बढ़ रहा है, खेत बंजर होते जा रहे हैं, और बाहरी प्रभावों के कारण पारंपरिक खेती पीछे छूट रही है। सरकारी नीतियों को इस ओर ध्यान देना होगा कि कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, किसानों को नए अवसर दिए जाएं, और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। पहाड़ों में पशुपालन एक अहम भूमिका निभाता है। बद्री गाय जैसी देशी नस्लें यहां की जैव विविधता और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन इसे संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है। आधुनिक डेयरी फार्मिंग, सहकारी दुग्ध समितियों और जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर इसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह उत्तराखंड की आत्मा को ही नष्ट कर दे। अनियंत्रित शहरीकरण और जंगलों की कटाई से राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। यदि यही हाल रहा, तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा उत्तराखंड मिलेगा, जहां न तो जैव विविधता बचेगी और न ही यहां की पारंपरिक पहचान।राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, पहाड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, और पर्यटन को इस तरह विकसित किया जाए कि यह स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। उत्तराखंड केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, यह उन लोगों की मातृभूमि है, जिन्होंने इसे अपने खून-पसीने से सींचा है। यहां के लोग अपने जंगलों, नदियों, पहाड़ों और संस्कृति को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे। यदि आवश्यकता पड़ी, तो वे फिर से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे।यह राज्य उन सभी का स्वागत करता है, जो इसकी पहचान और संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उत्तराखंड केवल एक व्यापारिक अवसर नहीं, बल्कि एक विरासत है। यह केवल कुछ पूंजीपतियों की जागीर नहीं, बल्कि उन सभी की धरोहर है, जो इसकी अस्मिता को संजोए रखना चाहते हैं।उत्तराखंड संघर्ष से बना है, और यदि इसे बचाने के लिए एक नई लड़ाई लड़नी पड़ी, तो यह भूमि एक बार फिर उसी साहस और आत्मसम्मान के साथ खड़ी होगी, जैसा उसने सदियों से किया है। उत्तराखंड के लोक देवताओं का स्थान न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन देवताओं की पूजा पद्धतियाँ सरल और आस्था से भरी होती हैं, जो इस प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। इन लोक देवताओं के प्रभाव के कारण यह प्रदेश “देवभूमि” के रूप में प्रसिद्ध है।समय के साथ, भले ही आधुनिकता और शिक्षा ने इन देवताओं के प्रति आस्था में कमी की हो, फिर भी जब कोई बड़ा संकट सामने आता है, तो उत्तराखंड के लोग इन लोक देवताओं की शरण में जाते हैं। यह दर्शाता है कि उत्तराखंड की देवभावना और लोक देवता की पूजा आज भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। । वैदिक पाठशाला का मुख्य उद्देश्य हमारी अति प्राचीन वैदिक पद्वति से ज्ञान की परंपरा का पुनर्उत्थान एवं स्थायित्व देना है। हमे हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य धर्मों के धर्मावलम्बी अपने धर्मो के अनुसार वेशभूष धारण कर अपने धर्म का अनुसरण करते है हमे भी गौरवान्वित अनुभव करते हुए अपने धर्मानुसार वेशभूष एवम आचरण का वरण करना चाहिए। तभी हमारी भावी पीढ़ी भी इससे सिख लेकर उसका अनुसरण करेगी। हमारे धर्मग्रंथों में हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है पाठशाला में उसी वैभवशाली संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। सर्वब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पं संजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्कृत शिक्षा पर जितना प्रकाश डाला जाए वह कम है, पौराणिक एवं धार्मिक चेतना को जगाने वाली संस्कृत भाषा अत्यंत सरल हैं। हमारे पूर्वज एवं वेद ग्रंथों में देखा जाए तो देश का प्रथम विषय संस्कृत ही है। जो की हमारे ऋषि मुनियो द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं एवं वेदों में मंत्रोधाार दर्शाए गए हैं वह सभी संस्कृत लिपि में दर्शाए गए हैं। पहले के राजा, महाराजा एवं वेद गुरु द्वारा शुद्घ संस्कृत की बोली बोली जाती थी। इसलिए अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने के लिए हमें संस्कृत ऐसे विषय को उधा स्तर पर ले जाने हेतु इस ज्ञान का प्रचार- प्रसार बहुत जरूरी है जो कि नगर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस विषय पर विशेष रूप से ज्ञान देना जरूरी है
*लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*