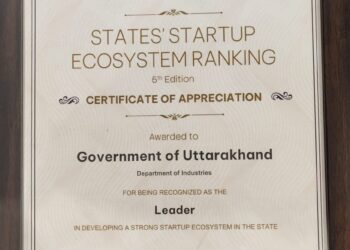डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखण्ड के बहुमूल्य उत्पादों की श्रंखला में एक और महत्वपूर्ण उत्पाद जिसको शायद ही कोई ना जानता हो। उत्तराखण्ड की पारम्परिक सब्जी पहाड़ी छेमी जिसको प्रदेश भर में सामान्यतः छेमी के नाम से ही जाना जाता है। छेमी का वैज्ञानिक नाम Dolichos lablab जिसका Fabaceae कुल के अन्तर्गत वानस्पतिक अध्ययन किया जाता है। छेमी को अनेकों वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है जो कि इसके ही प्रायः हैं। इतिहासकारों के अनुसार छेमी को सबसे प्राचीन, लगभग 300 वर्ष पूर्व उगाई जाने वाली सब्जी के रूप में भी जाना जाता है। इसका अस्तित्व लगभग आठवीं शताब्दी से माना जाता है। पूरे विश्व भर में छेमी की लगभग 60 प्रजातियां उगायी जाती हैं जो कि सबसे अधिक एशिया तथा अफ्रीका में उगायी जाती है।
भारत के अलावा छेमी को मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, चीन, ईराक, केनिया, सूडान, इथोपिया, नाईजीरिया, मध्य तथा पूर्वी अमेरिका आदि देशो में भी उगाया जाता है। छेमी में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के कारण इसे एशिया तथा अफ्रीका देशो में सब्जी के रूप में उपयोग हेतु उगाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका तथा अन्य विकसित देशो में इसे केवल घरेलू सजावट के लिये ही उगाया जाता है। छेमी को अन्य भाषाओ में अलग.अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि लबलाव.अरेबी, राजाशिम्बि, बंगाली, बैन डाउ, चाइनीज, डोलिचोस लबलाव.अंग्रेजी, डोलिक्यूडी इजिप्ट.फ्रेंच, एजिस्टचे फसेल .जर्मन, लोबिजा, रसियन, राज सिमी, नेपाली तथा फिजी मामे जापानीज आदि। समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊँचाई तक उगाई जाने वाली छेमी की फसल को भारत के कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में इसको घरेलू सब्जी उपयोग के लिये ही उगाया जाता है। उत्तराखण्ड में छेमी का उत्पादन सीमित मात्रा में किया जाता है तथा इसे स्थानीय सब्जी के रूप में बहुतायत पसंद किया जाता है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में छेमी का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही कर क्षेत्र के स्थानीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। हरी सब्जी के रूप में उपयोग की जाने वाली छेमी के रासायनिक विश्लेषण के आधार पर इसमें सुगर, एल्कोहल, फीनोल्स, स्टेरोइड्स, इसेंसियल ऑयल्स, एल्केलॉइड्स, टेनिन्स, फलेवोनॉइड्स, सेपोनिन्स, काउमेरिन्स, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स तथा एथनानोइड्स आदि सामान्यतः पाये जाते हैं।
वर्श 2000 में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार छेमी से एक डोलिचिन नामक रसायन आयसोलेट किया गया जिसे फूसारियम ऑक्सिसपोरमए राइजोक्टोनिया सोलानी तथा कोपरिनस कॉमेट्स नामक कवक (Fungi) के सापेक्ष प्रभावी पाया गया। इसके अलावा छेमी में प्रोटीन 2.95 ग्राम, वसा 0.27 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 9.2 ग्राम तथा विटामिन्स की अच्छी मात्रा पायी जाती है जैसे विटामिन बी1. 0.056 मिग्रा0, बी2. 0.088 मिग्रा, बी3. 0.48 मिग्रा0, बी 9.47 माइक्रो ग्राम एवं विटामिन सी. 5.1 मिग्रा0 प्रति 100 ग्राम तक पाये पर्वतीय क्षेत्रों में छेमी का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही कर क्षेत्र के स्थानीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। हरी सब्जी के रूप में उपयोग की जाने वाली छेमी के रासायनिक विश्लेषण के आधार पर इसमें सुगरए एल्कोहलए फीनोल्सए स्टेरोइड्सए इसेंसियल ऑयल्स, एल्केलॉइड्स, टेनिन्स, फलेवोनॉइड्स, सेपोनिन्स, काउमेरिन्स, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स तथा एथनानोइड्स आदि सामान्यतः पाये जाते हैं। भारत के अलावा पूर्व अफ्रीका में छेमी को भोजन में उपयोग हेतु अच्छा उत्पादित किया जाता है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक द्वारा लगभग 18000 टन उत्पादन 85000 हेक्टेयर भूमि पर किया जाता है। छेमी राजमा उत्तराखंड में राजमा को छेमी के नाम जाना जाता है। हर्षिल, चकराता, जोशीमठ और मुनस्यारी में होने वाली राजमा पूरे देश में सर्वोत्तम किस्म की मानी जाती है। पहाड़ की राजमा आसानी से पकने वाली और स्वाद में उत्तम होती है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी कीमत 190 रुपये प्रति किग्रा से 220 रुपये प्रति किग्रा है। उत्तराखंडी दालें जैविक होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद लाभदायी हैं।
इनकी खेती गढ़वाल.कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में की जाती है। हालांकि अब कई संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से इन्हें बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। राजमा को उत्तराखंड में छेमी के नाम से जाना जाता है। हर्षिल, जोशीमठ, चकराता एवं मुन्स्यारी की राजमा प्रसिद्ध है लेकिन पूरे देश में चकराता राजमा सर्वोतम मानी जाती है। हालांकि बाजार में जम्मू की राजमा की ज्यादा पहचान है। सभी तरह की पहाड़ी राजमा की दाल आसानी से गलने वाली व स्वाद में उत्तम होती है। पौष्टिकता में भरपूर राजमा प्रोटीन व रेशे का बड़ा स्रोत है। राजमा की तासीर ठण्ड मानी जाती है इस लिए लहसून, प्याज एवं गर्म मसाले इस्तेमाल करते हैं या एनी दाल के साथ खाते हैं, जिससे काश्तकारों को इनका अच्छा मूल्य मिल सके और लोग पारंपरिक खेती के प्रति भी आकर्षित हों। उपरोक्त सभी विशेषताओं को देखते हुये उत्तराखण्ड में छेमी के सीमित उत्पादन को बढावा देने के साथ.साथ इसमें प्रोटीन तथा पोटेशियम के अच्छे प्राकृतिक स्रोत को देखते हुये व्यवसायिक तथा स्वास्थ्य लाभ हेतु उत्पादन किया जा सकता है जो राज्य में आर्थिकी का अच्छा स्रोत बन सकता है। जिससे पर्यावरण तथा