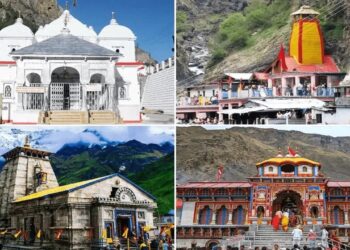डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर
करता है और बच्चों का भविष्य उनकी स्कूली शिक्षा पर टिका
होता है। स्कूल केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने के केंद्र नहीं हैं,
बल्कि वे चरित्र-निर्माण, सामाजिक कौशल, अनुशासन और
आत्मविश्वास की पहली पाठशाला होते हैं। यह वह पवित्र स्थान
है जहां एक बच्चा कल का जिम्मेदार नागरिक बनने की तैयारी
करता है। एक मजबूत स्कूली शिक्षा प्रणाली एक व्यक्ति को
अकादमिक रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ उसे जीवन की
चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। संक्षेप में,
स्कूल एक उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है, लेकिन जब यह
आधारशिला ही जर्जर और असुरक्षित हो, तो उस पर एक
मजबूत भविष्य की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? राजस्थान
में एक हृदय-विदारक घटना हुई , जहां एक सरकारी स्कूल की
छत गिरने से सात बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। यह घटना कोई
अकेली या अप्रत्याशित दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह देशभर में
सरकारी स्कूलों की प्रणालीगत उपेक्षा और जर्जर हालत का एक
क्रूर प्रतीक है। यह उजागर करता है कि हमारे बच्चे हर दिन
अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने
की कोशिश कर रहे हैं। यह समस्या किसी एक राज्य तक सीमित
नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी संकट बन चुकी है।राजस्थान में
अनुमानित करीब 8,000 स्कूल जर्जर हालत में हैं। ओडिशा में
करीब 12 हजार, पश्चिम बंगाल में करीब 4000, गुजरात में
करीब 3000 तथा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में प्रत्येक
में करीब 2500 सरकारी स्कूल जीर्ण-शीर्ण भवनों में चल रहे हैं।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लाखों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढऩे को
विवश हैं, जहां न तो पर्याप्त बेंच हैं, न पीने का साफ पानी, न ही
शौचालय और चारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाएं। बारिश के
मौसम में छतों का टपकना और दीवारों में सीलन आना एक आम
बात है, जो कभी भी राजस्थान जैसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले
सकती है। सरकारी स्कूलों के इस दयनीय स्थिति में पहुंचने के
पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई जटिल और आपस में जुड़े
हुए कारक जिम्मेदार हैं- स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत के
लिए बजट का आवंटन अक्सर अपर्याप्त होता है। शिक्षा पर सकल
घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक निश्चित हिस्सा खर्च करने की
सिफारिशों के बावजूद, वास्तविक आवंटन कम रहता है। जो
बजट आवंटित होता भी है, वह नौकरशाही की लालफीताशाही
और देरी के कारण समय पर स्कूलों तक नहीं पहुंच पाता।
सरकारों का ध्यान अक्सर नए स्कूल खोलने जैसी राजनीतिक
रूप से आकर्षक योजनाओं पर अधिक होता है, जबकि मौजूदा
हजारों स्कूलों के रखरखाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
मरम्मत और निर्माण के लिए आवंटित धन में भ्रष्टाचार एक
दीमक की तरह है, जो पूरे तंत्र को खोखला कर रहा है। घटिया
सामग्री का उपयोग और अधूरे काम के कारण समस्या जस की
तस बनी रहती है।स्कूल भवनों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए
जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की कोई स्पष्ट जवाबदेही
तय नहीं होती। हादसे होने के बाद जांच समितियां बनती हैं,
लेकिन निवारक उपायों, यानी नियमित निरीक्षण और निगरानी
पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विशेषकर दूर-दराज के ग्रामीण
क्षेत्रों में निगरानी तंत्र लगभग न के बराबर है। राष्ट्रीय शिक्षा
नीति (एनईपी) 2020 स्कूलों के बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर
तो देती है, लेकिन यह एक नीतिगत ढांचा है, न कि बजटीय
प्रावधान। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें वार्षिक बजट में इन
नीतियों को लागू करने के लिए ठोस वित्तीय आवंटन और एक
मजबूत कार्यान्वयन योजना नहीं बनातीं, तब तक ये नीतियां
कागजों तक ही सीमित रहेंगी। इस गंभीर समस्या के समाधान
के लिए 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक
और दूरदर्शी फैसला सुनाया था। न्यायालय ने आदेश दिया कि
उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों,
जनप्रतिनिधियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए अपने
बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया
जाए। इस आदेश का तर्क सीधा और शक्तिशाली था- जब
प्रभावशाली और निर्णय लेने वाले लोगों के बच्चे इन स्कूलों में
पढ़ेंगे, तो वे स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए व्यक्तिगत रूप से
प्रेरित होंगे और व्यवस्था पर दबाव डालेंगे। हालांकि, मजबूत
इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह आदेश धरातल पर नहीं उतर
पाया। यह इस बात का उदाहरण है कि केवल न्यायिक आदेश ही
पर्याप्त नहीं होता, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक
सहयोग और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती
है।देश में सरकारी स्कूलों का संकट केवल कुछ इमारतों के गिरने
का नहीं, बल्कि यह व्यवस्थागत उदासीनता, भ्रष्टाचार और
जवाबदेही की कमी का संकट है। यह हमारे देश के भविष्य,
यानी हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनके शिक्षा के अधिकार से
सीधे तौर पर जुड़ा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए इन
ठोस कदमों की तत्काल आवश्यकता है- स्कूलों के रखरखाव के
लिए एक अलग, पर्याप्त और गैर-व्यपगत (नॉन लैप्सेबल) बजट
का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसके खर्च का पूरा हिसाब
ऑनलाइन उपलब्ध हो। हर स्कूल भवन का एक स्वतंत्र एजेंसी
द्वारा हर दो साल में अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराया जाना
चाहिए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्कूल
के बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों (जैसे खंड
शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी) और ठेकेदारों की
जवाबदेही तय की जाए। लापरवाही के मामलों में सख्त
दंडात्मक कार्रवाई हो। स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिक
वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं ताकि वे स्थानीय
स्तर पर छोटी-मोटी मरम्मत का काम तुरंत करा सकें।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे प्रगतिशील आदेशों को लागू
करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना होगा।
जब तक नीति-निर्माताओं के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब
तक वास्तविक सुधार की उम्मीद करना कठिन है। अंतत:, जब
तक हम स्कूलों को केवल ईंट-गारे की इमारत न समझकर, उन्हें
राष्ट्र-निर्माण की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई नहीं मानेंगे, तब तक
ऐसी दुखद घटनाओं की आशंका बनी रहेगी और हम अपने बच्चों
के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। लगभग डेढ़ दशक
पहले, जब इंटरनेट के कारण नौकरियों के नुकसान को लेकर
बहस ज़ोर पकड़ रही थी, मैकिन्से की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ
कि इंटरनेट ने जितनी नौकरियाँ नष्ट कीं, उसके मुकाबले उसने
वास्तव में 2.4 नौकरियाँ पैदा कीं। यह इस तथ्य के बावजूद था
कि उस समय अधिकांश पेशेवरों को स्कूलों में औपचारिक
इंटरनेट शिक्षा नहीं मिली थी।हालाँकि इंटरनेट निस्संदेह एक
विध्वंसक था, लेकिन जिन लोगों ने पुनः कौशल प्राप्त किया,
उन्होंने न केवल अपनी क्षमता को अधिकतम किया, बल्कि अपने
करियर को "भविष्य-सुरक्षित" भी बनाया। अब, दुनिया एक ऐसे
ही चौराहे पर खड़ी है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग
नए विध्वंसक की भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि, इस बार,
हमारे पास पीछे मुड़कर देखने का लाभ है।इतिहास निस्संदेह
खुद को दोहरा रहा है, लेकिन हमें अपनी पिछली गलतियों को
दोहराने से बचना चाहिए। इस बार, हमें अपनी शिक्षा को
"भविष्य-सुरक्षित" बनाने की ज़रूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए
कि छात्र धारा के विरुद्ध तैरने के बजाय उसके साथ तैरना सीखें।
आज, यह एआई है; कल, यह कुछ और होगा। लेकिन अगर हम
यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे छात्र व्यावसायिक कौशल को
तकनीक के साथ एकीकृत करने की कला में पारंगत हैं, तो वे
चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो, आसानी से आगे बढ़ेंगे।
अनिश्चित भविष्य के लिए योजना बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता
है, लेकिन इस चुनौती से पार पाने का सबसे आसान तरीका है
हमेशा सतर्क रहना। बुद्धि – अज्ञानता नहीं – आनंद है, और छात्रों
को इस बुद्धि को विकसित करने में मदद करने के लिए, संस्थानों
को बाज़ार की नब्ज़ पकड़ने के लिए अपनी आँखें और कान खुले
रखने चाहिए: दुनिया किस ओर जा रही है, कौन सी तकनीकें
यहाँ टिकने वाली हैं, किन भविष्यवादी रुझानों पर दांव लगाना
है, और किन बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहना है।छात्रों को
उभरती वैश्विक समस्याओं से परिचित कराने से उन्हें नए
समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके
अलावा, उन्हें बदलावों और चुनौतियों के साथ सहज होना
सिखाया जाना चाहिए। ऐसा उन्हें अपने आसपास के परिवेश से
परे हो रहे विकास से अवगत रखकर किया जा सकता है। नई
चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार मानसिकता छात्रों को
उद्योग जगत के लिए तैयार होने में मदद कर सकती है। लक्ष्य
केवल ज्ञान के उपभोक्ता से आगे बढ़कर समाधान के निर्माता
बनना है। निश्चित रूप से, छात्रों को उन नौकरियों के लिए तैयार
करना जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं, अब केवल सैद्धांतिक अभ्यास
नहीं रह गया है – यह समय की माँग है। यह हमें एक लाख टके
के सवाल पर लाता है: हम इसे कैसे हासिल करें? यहाँ बताया
गया है कि शिक्षक, संस्थान और नीति-निर्माता छात्रों को
अनजानी नौकरियों के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। वर्तमान में
जियो – यह जीवन का एक ऐसा पाठ है जो कई लोग सिखाते हैं।
लेकिन व्यावहारिक रूप से, भविष्य पर नज़र रखना वर्तमान को
सुरक्षित रखने का एक व्यावहारिक तरीका है। यह और भी
प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि काम का भविष्य अभी अज्ञात क्षेत्र
है।महत्वपूर्ण बात यह है कि दूरदर्शी, लचीले और सामाजिक व
तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखें। बिज़नेस स्कूल
छात्रों को अनुकूलनशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने पर
ध्यान केंद्रित करके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण
प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।संक्षेप में,
भविष्य-सुरक्षित शिक्षा का अर्थ केवल नौकरियों के लिए तैयारी
करना नहीं है; इसका अर्थ है छात्रों को भविष्य को आकार देने के
लिए सशक्त बनाना। अनिश्चित समय में, स्कूलों को
"परामर्शदाता" दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। छात्रों को उद्यमिता
की गतिशील दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए,
शैक्षणिक संस्थानों को उन्हें सूचित करियर निर्णयों की दिशा में
मार्गदर्शन करने के लिए मज़बूत सलाहकार सेवाएँ प्रदान करनी
चाहिए। परामर्शदाताओं और मार्गदर्शकों की एक समर्पित टीम
छात्रों को मौजूदा और उभरते अवसरों, दोनों के बारे में जागरूक
कर सकती है, साथ ही उन्हें उन भूमिकाओं के लिए तैयार कर
सकती है जिनकी अभी तक कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है। *लेखक*
*विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में*
*कार्यरत हैं।*