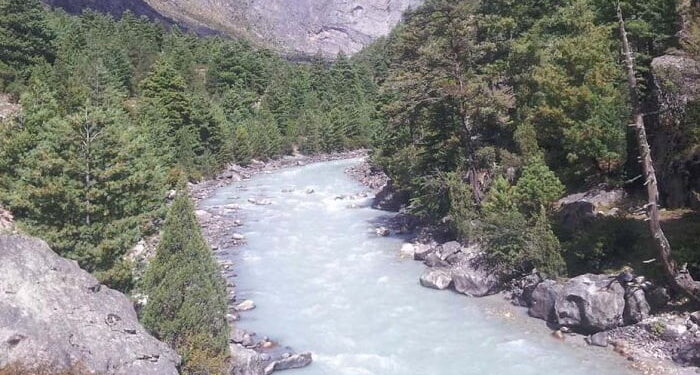डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
एशिया के वाटर हाऊस हिमालय में भी जल संकट खडा हो गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आंकड़े जारी किए थे, उसमें ये डराने वाली तस्वीर पेश की गई थी कि भविष्य में देश के सामने बडा जलसंकट खडा होने जा रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा। दर्जनों नदियों का उदगम क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड धीरे.धीरे गंभीर पेयजल संकट की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के अर्बन एरिया के ही आंकडे अगर उठकर देखें तो मांग के अनुरूप प्रतिदिन 13 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी की कमी बनी हुई है। पहाडों में अल्मोड़ा तो मैदान में ऊधमसिंह नगर सबसे अधिक जल संकट से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में 917 छोटे.बड़े ग्लेशियरों से दर्जनों बारहमासा बहने वाली नदियां निकलती हैं, जो देश के कई राज्यों को भी पीने का पानी देती हैं, लेकिन खुद उत्तराखंड पानी के संकट से जूझ रहा है। उत्तराखंड के अर्बन एरिया के 92 छोटे.बडे़ शहरों को प्रतिदिन 701 मिलियन लीटरर्स पानी चाहिए होता है, लेकिन इन शहरों को कुल 567 मिलियन लीटर पानी ही मिल पाता है। यानि की प्रतिदिन के हिसाब से 133 मिलियन लीटर पानी की कमी बनी हुई है। एक मिलियन लीटर का मतलब होता है दस लाख लीटर पानी। मांग के अनुरूप करीब 13 करोड़ लीटर पानी और चाहिए, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसने गर्मियों के मददेनजर जलसंस्थान की चिंता बढ़ा दी है।
मैदान से ऊधमसिंह नगर और पहाड़ से अल्मोड़ा में सबसे अधिक जल संकट है। ऊधमसिंह नगर में प्रतिदिन 27 मिलियन लीटर पानी की जगह दस मिलियन लीटर पानी ही मिल पा रहा है, हालांकि जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग का कहना है कि यहां हैंडपंप और टयूबवेल अधिक होने के कारण अधिकांश आपूर्ति इनसे हो जाती है। अल्मोडा में प्रतिदिन 21 मिलियन लीटर पानी की मांग के अनुरूप महज आठ मिलियन लीटर पानी ही मिल पा रहा है। ठीक इसी तरह देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, पिथौरागढ़ में भी मांग के अनुरूप पानी उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत लक्सर, सतपुली, कोटद्वार, झबरेडा, स्वर्गाश्रम, श्रीनगर, डोईवाला, ऋषिकेश ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। जल संकट से निपटने के लिए विभाग चालू योजनाओं को अपग्रेड करने की भी योजना बना रहा है, लेकिन ये अभी प्रस्ताव तक ही सीमित हैं।
बहरहाल, सूखते जल स्रोत, अंडरग्राऊंड वाटर का गिरता स्तर भविष्य में गहराते जल संकट की चेतावनी दे रहा है। पेयजल संकट से निपटने के लिए रेन वॉटर हारवेस्टिंग बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों की मानें तो हिमालय में हो रहे वनों के कटान और वन प्रबंधन बेहतर ना होने के कारण ना सिर्फ उत्तराखंड में ही जल प्रबंधन की स्थिति नाजुक है, बल्कि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल तक हुआ है, कि भविष्य के लिए जलसंकट बड़ी समस्या है। उन्होंने बताया कि कई विभाग इसके लिए कार्य तो करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कार्य नहीं होने से सकारात्मक परिणाम नहीं आते। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा तो फिर अच्छे परिणाम सामने आएंगे। देश के पर्वतीय राज्यों में शहरीकरण के साथ ही भूमिगत खनिज पदार्थों के लिये खनन, फैक्टरी, बाँध के निर्माण जैसी गतिविधियों से क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना के महत्त्वपूर्ण घटकों को अपूरणीय क्षति हुई है।
इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों में वृद्धि से प्राकृतिक जल के स्रोतों को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही खनन के कारण भू.स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ जाने से जल के संचयन में भी कमी आई है, जिसने जल संकट की समस्या को और बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर असर भी दिख रहा है। 2016 में 67 फीसदी, 2017 में 52 फीसदी और 2018 में 66 फीसदी बारिश रिकार्ड हुई है। गंगा नदी में हुए शोध के आकड़ों को देखें तो देवप्रयाग में गंगा नदी में 30 प्रतिशत जल ग्लेशियर और 70 प्रतिशत जल जंगलों, बुग्यालों, छोटी नदियों और जलधाराओं से आता है। अब सर्दियों के समय में बर्फबारी कम हो रही है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए हर साल करोड़ों की धनराशि पानी की तरह बहाई जाती है। अब सभी विभागों को एकजुट कर एक समूह बनाया गया है, तो साफ है आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। विशेषज्ञों की राय और विभागों के बीच समन्वय बनाया गया तो भविष्य में प्राकृतिक जलस्रोत फिर से रिचार्ज हो सकते हैं। वन विभाग के पास धनराशि कम है, जिसमें वर्षाजल संरक्षण पर कार्य किया जाना है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत खासतौर पर वन क्षेत्रों में स्थित जलधाराएं और झरने सूख रहे हैं और पिछले 150 वर्षो में करीब 60 प्रतिशत तक प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। वर्षाजल संरक्षण पर कार्य किया जाना है। इसी तरह सिंचाई विभाग, पेयजल, ग्राम्या सहित कई विभाग जल संरक्षण पर कार्य कर रहे है। ताकि भविष्य में ये किसी क्षेत्र से विलुप्त भी हो गई तो इन्हें फिर से जल स्रोत वहां सूख रहे जल स्रोत लौटाया जा सके।
पानी की कमी के कारण सूखा और वनाग्नि जैसे प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों के अतिरिक्त यह समस्या भविष्य में क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिये अपूरणीय क्षति का कारण बन सकती है। पानी की कमी के कारण सूखा और वनाग्नि जैसे प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों के अतिरिक्त यह समस्या भविष्य में क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिये अपूरणीय क्षति का कारण है। उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर.प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग पृथक रूप से अस्तित्व में था। उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्रों की भूमिगत जल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति इस विभाग द्वारा की जाती थी। इसके लिए मैदानी क्षेत्रों में कई भू.जलस्तर मापक यन्त्र-स्थल तथा वर्षा जल मापक यन्त्र-स्थल स्थापित है, जिनसे आंकड़े एकत्रित कर उपयोग किये जाते हैं। उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आने के बाद इस कार्य हेतु कोई संस्था-विभाग नहीं रह गया था तथा उत्तर प्रदेश द्वारा भी उत्तरांचल क्षेत्र में भूगर्भ जल सम्बन्धी कार्य छोड़ दिया गया है, जिस कारण भूमिगत जल सम्बन्धी आंकडे वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
वैसे भी उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित स्थल अच्छे आंकड़ों के लिए प्र्याप्त नहीं थे, जिसके लिए अतिरिक्त स्टेशन लगाये जाने एवं कर्मचारी लगाये जाने की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड के मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जहां पर नदी नालों एवं श्रोतों के श्राव लगातार कम होते जा रहे हैं, के आंकड़े एकत्र करने के बारे में पूर्व में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। समय आ गया है कि उन क्षेत्रों के जलश्राव के हास्र के कारणों को ज्ञात किया जाये। जगह.जगह पर श्रोतों को चिन्हित कर उसके श्राव का मापन किया जाये तथा तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष कर पहुंचा जाये। नदी नालों पर पेड़ झाडियों से पानी को कृत्रिम रूप से रोकने तथा चाल खाल को संरक्षित करने की जानकारी जनता को बखूबी थी। वर्तमान में यह प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। चाल खाल नष्ट होते जा रहे हैं। नदी नालों के बहाव को जगह.जगह पर रोककर त्मबींतहम करने की कोई व्यवस्था नहीं रह गयी थी। वर्षाजल संरक्षण पर कार्य किया जाना ऐसे में यह आवश्यक है।