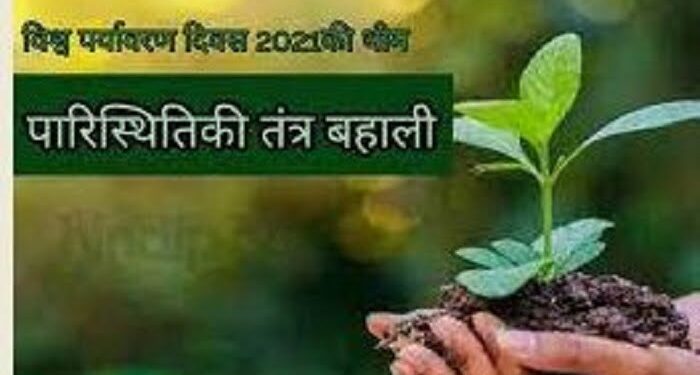डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
पर्यावरण के असंतुलन से सम्पूर्ण विश्व आपदाओं से घिरा हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि इसका मुख्य कारण विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, जिसके फलस्वरूप विकसित व विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण की बढ़ोत्तरी हुयी और पृथ्वी के अवयवों का विशेषकर.हाइड्रोकार्बन का अनियमित दोहन हुआ है। वही दूसरी तरफ वाहनों की आवश्यकता में कई गुना वृद्धि से पर्यावरण में कार्बन के उत्सर्जन व अन्य नुकसानदायक गैसों की मात्रा में निर्धारित सीमा से कई गुना वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है। जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि और पर्यावरण असंतुलन के कारण सम्पूर्ण विश्व आपदाओं से घिरा हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में, 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गयी थी। उसके दो.साल बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक पृथ्वी विषय पर आयोजित किया गया था। इसी दिन यह भी निर्धारित किया गया कि 5. जून 1974 से प्रतिवर्ष समारोह आयोजित किए जाये और फिर 1987 में यह निर्णय लिया गया कि गतिविधियों को बढाने के लिये विभिन्न देशों को इसकी मेजबानी के लिये मौका दिया जाय। पिछले दशकों में तापमान में भी 2.3 डिग्री सेन्टीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है। इससे ग्लेसियर व आइसलैण्ड व आर्कटिक समुद्र में अत्यधिक पिघलाव हो रहा है। प्रत्येक दशक में ग्लेसियर में 12.5 प्रतिशत की कमी आ रही है तथा समुद्र की सतह में निरन्तर 2.54 मिमी प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी हो रही है। उपरोक्त कारणों से जलवायु में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है तथा विश्व में अप्रत्याशित आपदाएँ भी घटित हो रही हैं। जिसका आकलन करना असम्भव हो रहा है कि विश्व में कब, कहाँ व क्या घटित होगा। इन आपदाओं से कही अतिवृष्टि से अधिक जानमाल का नुकसान, कही अति ओलावृष्टि व कही सूखे की मार से जन.जीवन को भारी नुकसान हो रहा है।
प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, अधिक जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, स्थायी अपशिष्ट उत्पन्न करना, अपशिष्ट निपटान, वनों की कटाई, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, महासागर अम्लीकरण, नाइट्रोजन चक्र, ओजोन परत का क्षरण, अम्ल वर्षा, जल प्रदूषण, ओवरफिशिंग, शहरी फैलाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे और जेनेटिक इंजीनियरिंग।
आज सम्पूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान की विभीषिका से ग्रसित है। उत्तरी धु्रव के तेजी से पिघलने के कारण जहां समुद्र की सतह में बढ़ोत्तरी हो रही है, वही अटलांटिक महासागर की छोर जो कनाडा, उत्तरी.पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी.उत्तरी संयुक्त राष्ट्र के देशों फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में समुद्री तूफान, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि से दिसम्बर माह से अप्रैल तक जनजीवन अस्त.व्यस्त हो रहा है। पिछले वर्ष से सम्पूर्ण विश्व कोविड.19 की महामारी से जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था भी पूर्णरूप से चरमरा गयी है। अभी तक विश्व में 17.25 करोड लोग संक्रमित हुये, 37.1 लाख लोगो की मृत्यु हो चुकी है और उनमें से 15.51 करोड लोग स्वस्थ हुये। विकास का पहिया रूक गया है। इस स्थिति से जब विश्व के समस्त विकसित व विकाशसील देश गुजर रहे हैं तो भारतवर्ष व अन्य विकाशसील देशों की स्थिति कोरोना, तूफानों, ग्लेशियर के गिरने और अतिवृष्टि, सूखा आदि से हालात बत्तर हो रहे हैं। आनेवाले समय में बच्चों का क्या भविष्य होगा, यह भी एक चिंतनीय विषय है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विश्व मानव को पर्यावरण सुरक्षा हेतु कारगर उपाय तत्काल ढूढ़ने व उसे तत्परता से लागू करने की आवश्यता है, जिससे वर्तमान में हो रही अप्रत्याशित घटनाओं में कमी लायी जा सके और आने वाली पीढ़ी को भी राहत मिल सके।
भारतवर्ष व अन्य विकाशसील देशो की स्थिति कोरोना, तूफानों, ग्लेसिअर के गिरने और अतिवृष्टि, सूखा आदि से बत से बत्तर हो रही है। आनेवाले समय में बच्चो का क्या भविष्य होगा, यह भी एक चिंतनीय विषय है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विश्व मानव को पर्यावरण सुरक्षा हेतु कारगर उपाय तत्काल ढूढ़ने व उसे तत्परता से लागू करने की आवश्यता है, जिससे वर्तमान में हो रही अप्रत्याशित घटनाओं में कमी लायी जा सके और आने वाली पीढ़ी को भी राहत मिल सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वर्तमान में कारगर उपाय न किये गये तो वर्ष 2040 तक हाइड्रोकार्बन जिसका पृथ्वी से दोहन हो रहा है। लगभग समाप्त के कगार पर होगा व उत्तरी धु्रव पर बर्फ के तीव्रता से पिघलने के कारण नाम.मात्र ही बर्फ मौजूद रहेगी तथा विश्व के सभी पर्वतीय श्रृंखलाओं में जहां ग्लेसियर हैं, समाप्त हो जायेंगे, जिससे समुद्र की सतह में लगभग 13 से 14 फीट पानी की बढ़ोत्तरी होना सम्भव है तथा 2015 के वर्तमान शोध के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन होना निश्चित है एवं पृथ्वी की गति में भी कमी आना सम्भव हैए जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना होने से नकारा नहीं जा सकता है।
पारिस्थितिकी तंत्र बहाली जैव विविधता संरक्षण के बिना असंभव है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र इसके बिना ठीक से काम नहीं कर सकते। उसने कहा कि भले ही हमारे जीवन में इलेक्ट्रानिक्स का उपयोग काफी बढ़ गया है लेकिन ई.कचरा प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अभी तक पूरा ध्यान नहीं मिला है और इलेक्ट्रानिक्स के उपयोगकर्ता इस कचरे के खतरों के बारे में नहीं जानते हैं। निदेशक ने इस अवसर पर कहा कि पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने के लिए आगे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनस्र्थापित करने में मदद करने के लिए पानी की बचत करने, ऊर्जा के अक्षय रूपों में स्थानांतरित करने के लिए सरल चीजों को अपनाने के लिए आसान चीजों को अपनाने के लिए कहा। 700 साल पुराना यह ग्लेशियर आइसलैंड देश के सबसे प्राचीन ग्लेशियरों में से एक था 2014 में इस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह पूरी तरह पिघल चुका था। 50 साल से ग्लेशियर के फोटो ले रहे पर्यावरणविद सायमीनी हावे ने पहली बार ओकजोकुल की पिघली बर्फ पर चेताया था। भारत में हिमालय में ग्लेशियर इतनी तेजी से पीछे हट रहे हैं कि शोधकर्ताओं का मानना है कि अधिकांश मध्य और पूर्वी हिमालयी ग्लेशियर 2035 तक गायब हो सकते हैं।
पृथ्वी की सेहत के तुलना में दुनिया में छोटे आर्थिक लाभों को प्राथमिकता दी जा रही है। उसका कहना है कि सरकारों, व्यापारियों और नागरिकों सहित पूरे समाज को शहरी क्षेत्रों फिर से जंगल बनाने के साथ घास के मैदानों, सवाना, समुद्री इलाकों को फिर से बहाल करना होगा। मानवीय गतिविधियों और हिमालयी जैव.संपदा के संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता बढ़ रही है। इसीलिए, हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन बेहद जरूरी हो गया है। उत्तराखण्ड के रूप में अलग राज्य बनने के बाद इसमें और बढ़ोत्तरी हुई। इसे नकारा नहीं जा सकता। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण काम यह हुआ कि पर्यावरण का सवाल पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया। यानी उसको पूरी तरह नजरअन्दाज कर दिया गया। असलियत में वर्तमान में सरकारों का एकमात्र लक्ष्य विकास होकर रह गया है, पर्यावरण संरक्षण नाम का शब्द तो उनके शब्दकोश में अब है ही नहीं। वह तो विकास का सबसे बड़ा उनकी दृष्टि में नदी का मानव जीवन और औद्योगिक हित में दोहन ही उसका सही मायने में उपयोग है अन्यथा नहीं यानी फिर तो वह निरर्थक है। उस स्थिति में जबकि यह पूरा.का.पूरा क्षेत्र भूकम्प के लिहाज से अति संवेदनशील है। तात्पर्य यह कि सिस्मिक जोन पाँच में होने के कारण इस क्षेत्र में भूकम्प का हमेशा खतरा बना ही रहता है। फिर जल.विद्युत परियोजनाओं की खातिर सुरंग बनाने हेतु किये जाने वाले विस्फोट के परिणामस्वरूप वहाँ रहने.बसने वालों के घर तो तबाह होते ही हैंए वहाँ के जल स्रोत भी खतरे में पड़ जाते हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों और वनों को यदि समय रहते नहीं बचाया गया तो इसका दुष्प्रभाव पूरे देश पर पड़े बिना नहीं रहेगा। यदि हिमालय बचेगा, तभी नदियाँ बचेंगी और तभी इस क्षेत्र में रहने.बसने वाली आबादी का जीवन भी सुरक्षित रह पाएगा। असलियत यह है कि विकास के ढेरों दावों के बावजूद अभी भी हिमालय क्षेत्र में रहने वाली तकरीब 80 फीसदी आबादी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। उनके जीवन में आज भी सुधार नहीं आ पाया है जिसकी वजह से वह पलायन को विवश हैं।