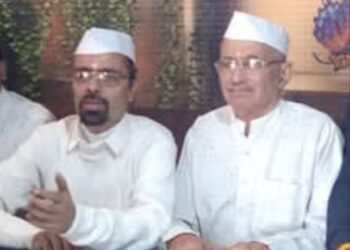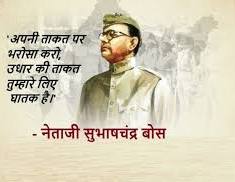डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी जनपदों में कृषि और बागवानी से जुड़े काश्तकारों की अलग ही परेशानी हैं। उन्नत किस्म के बीज और उत्तम क्वालिटी की दवा न मिलने से यहां काश्तकार परेशान हैं। लेकिन, इससे बड़ी परेशानी गांव से निकटवर्ती मंडी और बाजार तक तैयार फसल पहुंचाने की है। इसके अलावा पहाड़ में अधिकांश काश्तकार छोटी जोत वाले हैं। इसी कारण सामूहिक खेती और चकबंदी की वकालत भी काश्तकार लंबे समय से करते आ रहे हैं। राज्य बनने के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के लिए पहाड़ में मंडी नहीं बन पाई। कुमाऊं के पांच पर्वतीय जिलों में बड़ी मात्रा में फल, सब्जियों का उत्पादन होता है।पहाड़ में मंडी न होने से किसान फसल ढोकर हल्द्वानी, दिल्ली मंडी में बेचने जाते हैं। यहां बिचौलिए किसानों से कम दाम में फसल खरीदते हैं। ऐसे में कई बार किसानों की लागत तक नहीं निकल पाती है। राज्य बनने के बाद पांचवीं बार पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसके बावजूद किसानों के लिए मंडी बनाने का मुद्दा कहीं नजर नहीं आता है। कुमाऊं में ज्यादातर किसान पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाके से हैं।कुमाऊं के पांच पर्वतीय जिलों में सेब, नाशपाती, खुमानी, आडू, पुलम, अखरोट, आम, लीची के साथ सब्जियों का भी उत्पादन होता है। इसमें सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता है। आंकड़ों के अनुसार कुमाऊं में 48695.96 हेक्टेयर भूमि में फलों का उत्पादन किया जाता है जिससे करीब 444,569.89 मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है। कभी प्राकृतिक सुंदरता, स्वस्थ्य वातावरण भरे-पुरे जंगल और पहाड़ी खेती के लिए देश विदेश में विख्यात उत्तराखंड धीरे-धीरे अपनी पहचान खो रहा है। विकास की अंधी दौड़ ने लोगों की सोच और रहन सहन का तरीका बदल दिया है। इसका सीधा प्रभाव क्षेत्र की संरचना में नज़र आ रहा है। अब यहां जंगलों और प्राकृतिक रूप से निर्मित मकानों की जगह कंक्रीट के घर ने ले ली है। बड़े बड़े पांच सितारा होटल बनाने और अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालच ने लोगों को खेती किसानी से दूर कर दिया है। परिणामस्वरूप राज्य में खेती के लिए भूमि सिकुड़ती जा रही है। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है. चाहे वह बढ़ता तापमान हो, उत्पादन की मात्रा में गिरावट की बात हो, जल स्तर में गिरावट हो या फिर ग्लेशियरों के पिघलने इत्यादि सभी जगह देखने को मिल रहे हैं. जलवायु में होने वाले बदलावों ने सबसे अधिक कृषक वर्ग को प्रभावित किया है. चाहे वह मैदानी क्षेत्र के हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र के किसान. मैदानी क्षेत्र में फिर भी आजीविका के कई विकल्प मौजूद हैं. यदि कृषि में नुकसान हो रहा हो तो अन्य कार्य के माध्यम से आय की जा सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का खामियाजा हर हाल में कृषकों को ही उठाना पड़ रहा है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के पास आय के दूसरे श्रोत नहीं हैं. वहीं प्राकृतिक कहर और जंगली जानवरों के नुकसान ने कृषकों को खेती से विमुक्त होने के लिए विवश कर दिया है. अब किसान या तो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं या फिर मामूली तनख्वाह पर कहीं काम कर रहे हैं. सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है लेकिन भीमताल, रामगढ़, ओखलकांडा, धारी और बेतालघाट के पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक मंडी की स्थापना न होने से काश्तकार अपनी फसलों व फलों को बिचौलियों के माध्यम से हल्द्वानी मंडी में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।कृषि मंत्री धारी या ओखलकांडा के मध्य मंडी खोलने की घोषणा काफी पहले कर चुके हैं लेकिन उद्यान विभाग को अब तक भूमि नहीं मिली है। अफसोस है कि मंडी खुलने का सपना धरातल पर नहीं उतर सका है। काफल तो उत्तराखंड का राजकीय फल ही है, जो मीठा, खट्टा और रसीला होता है. और उसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और अनेक विटामिन भी होते हैं । देवभूमि के पहाड़ों पर तिमला, मेलू, अमेज, दाडि़म, करौंदा, तूंग, जंगली आंवला, खुबानी, हिसर, किनगोड़ जैसे अनेक अन्य जंगली फल भी पाए जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद होते हैं। मगर यह क्या ? चंबा, टिहरी और काना ताल के बाजारों में कहीं भी कोई स्थानीय फल ढूंढे से भी नहीं मिला । वहां के बाजार भी उन्हीं आमों, लीची, आड़ू और सेब से भरे पड़े थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अथवा दिल्ली की आजाद पुर सब्जी मंडी से वहां पहुंचे थे । बेशक सवाल छोटा सा था मगर मैं उसमें अटक गया कि पहाड़ का फल जब पहाड़ पर ही नहीं मिलता तो बाकी देश के बाशिंदे उनका सेवन कैसे करेंगे ? ऐसे में इन नायाब फलों के निर्यात की बात तो सोची भी कैसे जा सकती है ?स्थानीय लोगों से जब इस विषय में बात की तो पता चला कि सेब, माल्टा, आड़ू और खुबानी जैसे पारंपरिक फलों को छोड़ कर अन्य स्थानीय फलों की वहां खेती ही नहीं की जाती और प्राकृतिक रूप से जो फल जितना भी उपलब्ध होता है, उसे ही स्थानीय लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इन बेहतरीन फलों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए आज तक कोई प्रयास न तो सरकार ने किया है और न ही काश्तकारों ने । ले देकर बुरांश के फूल का रस जरूर बोतलों में बंद कर पर्यटकों को बेचा जाने लगा है मगर बुरांश का फल तो अभी भी बाजार तक नहीं पहुंचा । जबकि यह फल भी स्वादिष्ट होने के साथ साथ अनेक बीमारियों के इलाज में भी उपयोगी होता है। दुनिया जानती है कि उत्तराखंड के अधिकांश फल जैविक रूप से उगाए जाते हैं और इन फलों के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव-विविधता को बनाए रखने में भी मदद करते हैं । काफल, हिसालू, और बेड़ू जैसे फल तो स्थानीन संस्कृति, लोकगीतों और लोककथाओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ।पहाड़ से लौट कर पड़ताल की तो पता चला कि साल 2016 से अब तक उत्तराखंड में फलों के लिए आरक्षित भूमि में 54 फीसदी की कमी आई है और इसी के चलते फलों का उत्पादन भी 60 फीसदी घट गया है। वर्ष 2016 में 4551 मीट्रिक टन फलों का यहां से निर्यात होता था जो अब घटते घटते मात्र 1192 मीट्रिक टन ही रह गया है। हैरानी की बात नहीं है कि उत्तम क्वालिटी के फलों का उत्पादन करने के बावजूद राज्य से अब मात्र 4 करोड़ 68 लाख का ही निर्यात होता है ? इन फलों में भी केवल वही फल हैं जो हमें आमतौर पर अपने गली मोहल्ले में भी मिल जाते हैं। केवल पहाड़ पर ही मिलने वाले फल सिरे से गायब हैं जाहिर है कि राज्य सरकार का इस ओर कतई ध्यान नहीं है और यही कारण है कि किसान फलों की बागवानी को लेकर उदासीन हो रहे हैं। कई बार घोषणा के बावजूद राज्य में काश्तकारों को ओला वृष्टि जैसी आपदाओं से निपटने को सब्सिडी नहीं दी जा रही और किसानों को मंडियों से जोड़ने को कोई महत्वपूर्ण पहल भी अब तक नहीं की गई । ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी राज्य सरकार का ध्यान नहीं है तो फिर उसका ध्यान कहां है .! *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*