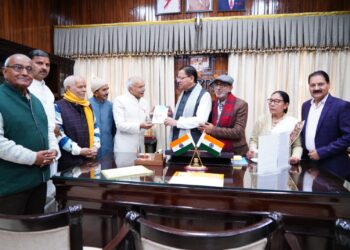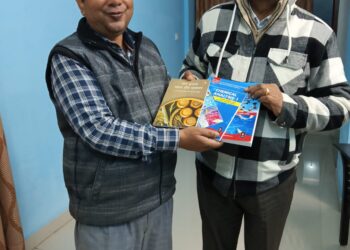डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत का भाल कहा जाने वाला हिमालय देश के
करीब 65 हिस्से को पानी उपलब्ध कराता है। गंगा-यमुना जैसी सदानीरा
नदियां यहीं से निकलती हैं। साथ ही हिमालय जड़ी-बूटियों का विपुल भंडार है।
हवा, पानी और मिट्टी के मामले में अहम भागीदारी निभाने के बावजूद हिमालय
के मिजाज को समझने और उसके संरक्षण को अभी तक ठोस और प्रभावी कदम
नहीं उठाए जा सके हैं। वह भी तब जबकि समूचा हिमालय प्रकृति सम्मत और
मानवजनित चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि, पिछले वर्षों में उत्तराखंड समेत
अन्य हिमालयी राज्यों ने थोड़ी बहुत पहल जरूर की है, लेकिन गैर हिमालयी
राज्यों का योगदान इसमें न के बराबर है। ऐसे में आवश्यक है कि देश के सभी
राज्य हिमालय की पीर को समझें और इसके संरक्षण में भागीदारी
निभाएं।भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 16.3 प्रतिशत हिस्से में जम्मू-
कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला है हिमालय। बदली परिस्थितियों में
यह हिमालयी क्षेत्र एक नहीं अनेक झंझावातों से जूझ रहा है। हिमालयी क्षेत्र में
निरंतर आ रही आपदाएं डराने लगी हैं और हिमालयी राज्य उत्तराखंड भी इससे
अछूता नहीं है।इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटना, भूस्खलन,
हिमस्खलन, नदियों का बढ़ता वेग जैसी आपदाएं उत्तराखंड पर निरंतर ही टूट
रही हैं। अन्य हिमालयी राज्यों की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। हिमालयी
क्षेत्र की नाजुक भूगर्भीय संरचना को नजरअंदाज कर बेतहाशा विकास कार्य किए
जा रहे हैं। नदियों और मौसमी नालों के किनारे निर्माण की वजह से अब तक
सैकड़ों घर ध्वस्त हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। इनसे सबक लेने
के बजाय सरकारें अब भी अनियोजित विकास पर जोर दे रही हैं। यह कहना है
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देहरादून के पूर्व अपर महानिदेशक का। हिमालयी
क्षेत्र की नाजुक भूगर्भीय संरचना को नजरअंदाज कर बेतहाशा विकास कार्य किए
जा रहे हैं। नदियों और मौसमी नालों के किनारे निर्माण की वजह से अब तक
सैकड़ों घर ध्वस्त हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। इनसे सबक लेने
के बजाय सरकारें अब भी अनियोजित विकास पर जोर दे रही हैं। यह कहना है
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देहरादून के पूर्व अपर महानिदेशक का। उत्तराखंड
का पूरा इलाका भूगर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील हिमालयी भूभाग में आता है।
चारधाम ऑलवेदर रोड जैसी परियोजनाएं इस बात का उदाहरण हैं कि यहां
योजनाओं को मंजूरी देने से पहले भू-वैज्ञानिकों से राय तक नहीं ली जाती।
उनका मानना है कि ढांचागत विकास कार्यों में भू-विज्ञान की अनदेखी सबसे
बड़ा खतरा है। अनियोजित शहरीकरण ने न सिर्फ पर्यावरणीय संकट बढ़ाया है
बल्कि सुरक्षित और उपयुक्त भूमि का चयन करना भी कठिन बना दिया है।
भविष्य में तीर्थयात्रा, पर्यटन और विकास की गतिविधियों पर इसका गंभीर
असर होगा। पहाड़ों पर मानव निर्मित संरचनाओं से प्राकृतिक जल धाराओं और
मौसमी नालों का बहाव अवरुद्ध हो जाता है। इससे पानी का प्रवाह बदल जाता
है। जलधारा से ढलान के आधार का कटाव, ढलान की सुरक्षा की कमी, जल
निकासी का अभाव, असुरक्षित व अनियोजित निर्माण और भारी व अनियंत्रित
ब्लास्टिंग ये सभी कारक पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और गंभीर भू-धंसाव के मुख्य
कारण हैं। धराली, हर्षिल, थराली, केदारनाथ, वर्णावत सहित पूरे उत्तराखंड में
इस प्रकार की आपदाओं के होने का मुख्य कारण यही अनदेखी रही है। भूस्खलन,
बाढ़, भूमि धंसाव और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान को नियंत्रित
करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। हिमालयी
राज्यों में राजमार्ग, रेलवे, जल विद्युत और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं
में सतत निर्माण के लिए व्यापक भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन
अनिवार्य है ताकि अनियोजित और अवैज्ञानिक क्रियान्वयन से पूरे क्षेत्र के
पारिस्थितिकीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क
की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में नदी की साइड कॉलम बनाकर
एलिवेटेड रोड का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। सड़कों का
चौड़ीकरण उस क्षेत्र की भूगर्भीय दशा का अध्ययन करते हुए किया जाना
चाहिए। अदालत ने हिमालयी राज्य की कई गंभीर चिंताओं को सूचीबद्ध किया
– जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जलविद्युत परियोजनाओं के "दृश्यमान"
और "चिंताजनक" प्रभाव, जिनसे कथित तौर पर पानी की कमी और भूस्खलन
हो रहा है; अनियंत्रित पर्यटन पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है और
संसाधनों पर दबाव डाल रहा है; और बढ़ती संख्या में पर्यटकों को समायोजित
करने के लिए चार-लेन सड़कों, सुरंगों और बहुमंजिला इमारतों का निरंतर
निर्माण. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास
रहने वाले समुदायों के संघर्षों को उजागर किया, जो पानी की कमी, भूस्खलन
और यहां तक कि अपने घरों के पास संरचनात्मक दरारों से जूझ रहे हैं. जजों ने
"अनुबंध में अनिवार्य" न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखने में विफलता की ओर
इशारा किया. पर्वतीय क्षेत्र में तापमान में कई डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान
है, जिससे अधिक ग्लेशियर पिघलेंगे, जो शुरुआत में नदी के प्रवाह को बढ़ाता है
और बड़े पैमाने पर मौसमी बाढ़ का कारण बनता है, जिसके बाद शुष्क अवधि
आती है. हाल के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि साल 2100 तक, यह क्षेत्र –
उत्तराखंड सहित – अपने ग्लेशियरों का 70-99% तक खो सकता है. ग्लोबल
वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया द्वारा ऊर्जा की खपत और उत्पादन में बदलाव
करने से पहले, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को मजबूत करने के लिए स्थानीय
स्तर पर कई छोटे कदम उठाए जा सकते हैं. यह याद रखना जरूरी है कि अनोखा
हिमालयी परिदृश्य – जो खड़ी ढलानों और तेज ढालों से चिह्नित है –
स्वाभाविक रूप से मानव इंजीनियरिंग के लिए उपयुक्त नहीं है. ये परिदृश्य
गतिशील रूप से विविध हैं, जिनमें जलवायु चर, जल विज्ञान प्रक्रियाएं और जैव
विविधता जैसे गुण लगातार बदल रहे हैं.जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुरंग
जैसी भूमिगत संरचनाएं पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती हैं, जिसमें
यातायात के उत्सर्जन से निकलने वाले प्रदूषकों का जमाव भी शामिल है. लंबी
दूरी की सुरंगों में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और सीमित फैलाव के कारण
यह समस्या और भी विकट हो जाती है. रेल यातायात विद्युत परिवहन पर
निर्भर हो सकता है, लेकिन लगातार जमीनी कंपन पहाड़ी ढलानों को हमेशा के
लिए अस्थिर बना सकते हैं और जरा सी भी हलचल होने पर भूस्खलन का खतरा
पैदा कर सकते हैं. विस्फोट अक्सर चट्टानों की संरचनाओं को कमजोर कर देते हैं,
जिससे भूस्खलन का खतरा और बढ़ जाता है और बड़ी मात्रा में उत्खनन से
निकलने वाला कचरा निकलता है. सुरंग निर्माण के दौरान भूजल स्तर पर देखे
गए अपरिवर्तनीय प्रभाव चिंता का विषय हैं, क्योंकि उत्खनन से चट्टानों की
संरचनाओं में तनाव परिवर्तन और विकृति उत्पन्न होती है, जिससे भूस्खलन की
आशंका बढ़ जाती है. जोशीमठ और अन्य शहरों में देखा गया भू-धंसाव एक
चेतावनी है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आगे क्या हो सकता है.
हिमालय में बिगड़ती पर्यावरणीय स्थितियों पर चिंताएं विकास और स्थिरता के
लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की मांग करती हैं – एक ऐसा दृष्टिकोण जो
पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता दे, साथ ही
अपूरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करे.. यही नहीं, ग्लेशियरों का
निरंतर पिघलना, स्नो और ट्री लाइनों का ऊपर की तरफ खिसकना भी हिमालयी
क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। हिमालय की बिगड़ती सेहत के
कारणों की तह में जाएं तो इसके पीछे उसकी अनदेखी सबसे बड़ी वजह है।
असल में बेहद संवेदनशील वातावरण वाले हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण और
विकास के मध्य सामंजस्य का अभाव साफ देखा जा सकता है।इसके अलावा
हिमालयी क्षेत्र के गांवों से आजीविका के साधनों के अभाव में निरंतर पलायन हो
रहा है। सीमांत गांवों में ग्रामीणों की संख्या अंगुलियों में गिनने लायक रह गई
है। सूरतेहाल, हिमालय में नागरिक ही नहीं रहेंगे तो हिमालय का संरक्षण कौन
करेगा। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जाहिर है कि ऐसे प्रयासों की दरकार
है, जिससे हिमालय भी सुरक्षित रहे और यहां के निवासियों के हित भी। *लेखक*
*विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*