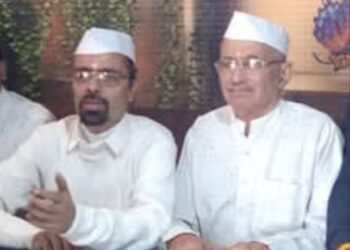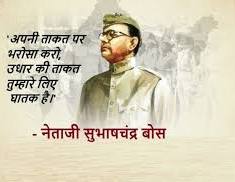डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड के चार धामों में से एक विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को रोपवे सुविधा मिलेगी. इसके लिए तैयारी तेजी से चल रही है. केंद्र सरकार ने केदारनाथ रोपवे परियोजना का टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है. लगभग 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इस परियोजना को देश की एक प्रमुख कंपनी को सौंपा गया है. कंपनी अगले पांच सालों में इस रोपवे का निर्माण करेगी और आने वाले 29 वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव भी करेगी. केदारनाथ में रोपवे का सर्वे से लेकर सभी धरातल के काम लगभग पूरे कर लिए हैं.पर्यटन मंत्री से मिली जानकारी के अनुसार, यह रोपवे परियोजना 12.9 किलोमीटर लंबी होगी, जो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक बनेगी. अभी जहां श्रद्धालुओं को 16 किमी की पैदल चढ़ाई में 8 से 9 घंटे लगते हैं, वहीं रोपवे तैयार होने के बाद यह दूरी केवल 35 से 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी. इस परियोजना में आधुनिक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो तारों के सहारे रोपवे को लाने और जाने में मदद करेगा.हर साल चारधाम यात्रा के दौरान करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं. बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा अक्सर बाधित रहती है. वर्तमान में लोग पैदल, खच्चरों और हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचते हैं. लेकिन रोपवे बन जाने के बाद यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यात्रियों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है. साथ ही लोगों का समय बचेगा.हालांकि, इस पूरे प्रोजेक्ट पर पर्यावरणविद चिंतित हैं. प्रसिद्ध पर्यावरणविद् ने इस परियोजना पर सवाल उठाए हैं.पहाड़ पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं के दबाव में है. ऐसे में मशीनों और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों से केदारनाथ क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को खतरा हो सकता है. उन्होंने चेताया कि पिछले वर्षों में उत्तराखंड ने कई आपदाएं देखी हैं. इसलिए पहाड़ों पर किसी तरह का बड़ा एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माणकार्य बिना पहाड़ों को काटे और तोड़े नहीं हो सकता है. अगर इसके बिना कुछ होता है तो, बात अलग है.पर्यटन मंत्री का कहना है कि रोपवे परियोजना से पर्यावरण को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होगा. मंत्री की मानें तो जो श्रद्धालु अभी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वो रोपवे का विकल्प चुनेंगे. इससे हेलीकॉप्टर की आवाजाही कम होगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा. यात्रियों को आरामदायक सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. मंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हेमकुंड साहिब तक भी रोपवे का निर्माण करेगी.उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सरकार वहां भक्तों के लिए बेहतर सुविधा जुटा रही है. केदारनाथ की चढ़ाई बेहद कठिन है. ऐसे में बहुत से लोग जा पाते हैं और बहुत से लोग नहीं जा पाते. केदारनाथ में इस प्रोजेक्ट की इसलिए भी जरूरत है, ताकि आसानी से श्रद्धालु धाम तक पहुंच सके. हम आगे ओर भी इस तरह के प्रोजेक्ट प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बनाने जा रहे हैं.: पर्यटन मंत्री का कहना है, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका प्रॉपर सर्वे होता है. कोई भी प्रोजेक्ट यूं ही तैयार नहीं होता है. हमारे प्रदेश में रेल मार्ग भी बन रहा है और जल्द तैयार हो जाएगा. सरकार बेहद शानदार तकनीक से सभी प्रोजेक्ट तैयार कर रही है. उत्तराखंड का मनसा देवी या सुरकंडा देवी रोप-वे प्रोजेक्ट भी सर्वे के बाद ही बने हैं. उनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी पहलुओं की देख-रेख के बाद ही काम शुरू होता है.उन्होंने कहा कि, साथ ही समय समय पर रोप-वे और पहाड़ों के हालात परखे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी का इससे रोजगार छिनेगा, बल्कि रोजगार बढ़ेगा. यात्रियों की संख्या अधिक आएगी, तो काम भी अधिक लोगों को मिलेगा. इसलिए ये कहना कि रोपवे से किसी का रोजगार खत्म हो जाएगा, गलत है. आज अगर 20 लाख भक्त आ रहे हैं, फिर हो सकता है 30 लाख या उससे कई अधिक आएं.पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ने दावा किया कि रोपवे की योजना यूपीए सरकार के समय ही बनाई गई थी. उनका कहना है कि हमारी (कांग्रेस) सोच यह थी कि सोनप्रयाग से सीधा रोपवे न बने, बल्कि बीच में गौरीकुंड जैसे धार्मिक स्थल पर एक स्टॉप रखा जाए. इससे स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और तीर्थ का पारंपरिक स्वरूप बना रहेगा. सीधा रोपवे बनना स्थानीय लोगों के साथ अन्याय होगा.हम पहले से ही कहते रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ इस लायक नहीं हैं कि उनमें इतने बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएं. लेकिन फिर भी पहाड़ों को लगातार खोदा और डायनामाइट से तोड़ा जा रहा है. जोशीमठ की घटना हाल ही का उदाहरण है. हर साल बारिश के दौरान केदारनाथ और आसपास की घटना एक चेतावनी है. सरकार टीटमेंट करे लेकिन भारी मशीनें का उपयोग और पहाड़ों को खोदना सही नहीं है. ये सभी पहाड़ बेहद नए हैं और उनमें काम करना सही नहीं है स्थानीय लोगों की उम्मीदेंअभी तक अधिकांश लोग पैदल या खच्चरों के सहारे धाम तक जाते हैं, जिससे यात्रा सीमित रहती है. लेकिन रोपवे शुरू होने पर अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे. जिससे रोजगार और पर्यटन दोनों को फायदा होगा.बहरहाल केदारनाथ रोपवे परियोजना, उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है. हालांकि, रोपवे से श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा आसान होगी, लेकिन पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी हैं. ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन कैसे बनाती है. उत्तराखंड, पेड़ों का अंधाधुंध कटान मौजूदा आपदा का सबसे बड़ा कारण है। सर्वाेच्च अदालत ने तब भी दखल दिया था जब गंगोत्री की भैरों घाटी में आल वेदर की भेंट चढ़ रहे देवदार और अन्य प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ों को बचाने के लिए इनके तनों पर राखियां/रक्षासूत्र बांधे जा रहे थे। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जियोलॉजिस्ट की एक कमेटी तक गठित की, लेकिन सरकारों के पास हर किस्म का तोड़ है। मनमुताबिक सड़क चौड़ी करने के लिए उसने सड़क को किलोमीटर के हिसाब से ऐसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिनके लिए एनजीटी मंजूरी की जरूरत ही नहीं होती। यही सब देखकर कमेटी से नामी जियोलॉजिस्ट को इस्तीफा देना पड़ा।पहाड़ों में सड़क बनें, पर कितनी चौड़ी बनें! होटल बनें, पर क्या भारी-भरकम निर्माण सामग्री के साथ इतने विराट बनें कि पूरी पहाड़ी खोदनी पड़ जाए ! बांध बनें, पर क्या रिजर्व-वायर का आयतन गुपचुप बढ़ा दिया जाए! तीर्थों को सुविधामय बनाने के लिए उनका विकास हो, पर सुरक्षित पर्यावरण के उसूलों का मखौल उड़ा दिया जाए! ये प्रश्न पहले हमें खुद से पूछने होंगे, मौसमी बदलाव के सैद्धांतिक अवयवों का नंबर इसके बाद आता है। आधुनिक और अंधाधुंध विकास का चश्मा लगाकर हिमालय और इसके संसाधनों पर लार टपकाने वाली सरकारें और उसके योजनाकारों की फौज यदि छटांग भर भी इस बात समझ सकती कि हिमालय के लिए किस तरह की योजनाओं का खाका खींचना है तो शायद हमें धराली और थराली जैसे विनाशों के लिए मौसमी परिवर्तन की आड़ न लेनी पड़ती। अफसोस कि क्षति के लिए हमारे निशाने पर सिर्फ आसमान है, जमीन पर पसरी मानवीय भूलें नहीं ! उत्तराखण्ड का रुद्रप्रयाग जिला संवेदनशीलता कह दृष्टि से एक नम्बर पर तथा टिहरी दूसरे नम्बर पर दिखाया गया है। प्रदेश के सभी 13 जिले संवेदनशील बताये गये हैं। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एनआइडीएम की रिपोर्ट में भूस्खलन जोनेशन मैपिंग का प्राथमिकता के आधार पर पालन, निर्माण कार्यों में विस्फोटों के प्रयोग पर रोक, सड़क निर्माण में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, ढलानों के स्थिरीकरण के ठोस प्रयास और ग्लेशियल लेक तथा नदी प्रवाह निगरानी का ठोस ढांचा तैयार करने की सिफारिश भी की गयी थी। अगर इन सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता तो पहाड़ इस तरह नहीं काटे जाते और केदारनाथ जैसे संवेदनशील स्थान पर सीमेंट कंकरीट का इतना बड़ा ढांचा भी खड़ा नहीे किया जाता हजामत की तैयारी न होती। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं*