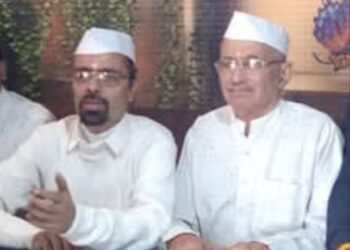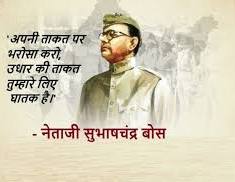डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों के दौरान भूकंप, बाढ़, ग्लेशियर टूटने,
भूस्खलन जैसी त्रासदी तबाही मचा चुकी है। लेकिन, यहां भौगोलिक
परिस्थितियों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के ढांचे को सुदृढ़ नहीं
किया गया। हां, पिछले 20 वर्षों के अंतराल में शासन स्तर पर इसको लेकर
चर्चाएं जरूर हुई हैं। दून में नदी-नालों के किनारों पर खड़ी सवा लाख से
अधिक आबादी, फ्लड प्लेन जोन में पसरी 129 मलिन बस्तियां और पर्यटन
के नाम पर घाटियों में हो रहा अंधाधुंध निर्माण ये सब मिलकर राजधानी
को किसी भी वक्त बड़े हादसे की ओर धकेल रहे हैं।रिस्पना-बिंदाल जैसी
नदियां लगातार उफान पर हैं, पहाड़ों से लेकर मैदान तक जमीन दरक रही
है और लगातार हो रही बारिश भी तबाही का सबब बन रही है। बावजूद
इसके, न तो नदी-नालों के मुहानों पर निर्माण रुक रहे हैं और न ही आपदा
को लेकर नीति नियंता ही गंभीर नजर आ रहे हैं।देहरादून में नगर निगम के
रिकार्ड बताते हैं कि शहर में 50 हजार से अधिक मकान नदी-नालों के
किनारे खड़े हैं। 2006 में किए गए सर्वे में 11 हजार अवैध निर्माण सामने
आए थे, लेकिन यह आंकड़ा अब बढ़कर 50 हजार पार कर चुका है। नगर
निगम सीमा का विस्तार होने के बाद जुड़े 72 गांवों में भी कई बस्तियां
नदियों के किनारे बसी हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है।हाईकोर्ट के आदेश
पर बिंदाल नदी किनारे 2016 के बाद बने 310 अवैध निर्माणों को
चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, अब तक पुनर्वास के नाम
पर सिर्फ काठबंगला बस्ती में 112 मकान ही तैयार हो पाए हैं। नगर
आयुक्त का कहना है कि आने वाले समय में और पुनर्वास योजनाएं लाई
जाएंगी, लेकिन मौजूदा प्रयास आबादी की तुलना में बेहद बौने नजर आते
हैं।तत्कालीन सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते बार-बार
अध्यादेशों के सहारे इन बस्तियों का अस्तित्व बचाए रखा। 2016 से पहले
बनी बस्तियां अध्यादेश के जरिए नियमित कर दी गईं, जबकि इसके बाद
हुए निर्माण अवैध माने गए। यही वजह है कि खतरे के बीच जी रही लाखों
की आबादी के लिए कोई ठोस पुनर्वास योजना धरातल पर उतर नहीं
पाई।राजधानी देहरादून की खूबसूरत घाटियां अब धीरे-धीरे आपदा की
गिरफ्त में आ रही हैं। सहस्रधारा, गुच्चू-पानी, मालदेवता, शिखर फाल और
किमाड़ी जैसे पर्यटन स्थल, जहां कभी प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य सैलानियों
को आकर्षित करता था, आज अतिवृष्टि और बादल फटने के बढ़ते खतरे के
लिए बदनाम हो रहे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि इन घाटीनुमा क्षेत्रों में
भौगोलिक स्थिति के कारण वैसे भी भारी बारिश का जोखिम रहता है,
लेकिन मौसम के बदलते पैटर्न ने घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों
बढ़ा दी है। चिंता की असली वजह है यहां पिछले कुछ वर्षों में हुआ अंधाधुंध
निर्माण।नदी-नालों के किनारों पर मकान, होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट और
होम-स्टे की कतारें खड़ी कर दी गई हैं।सहस्रधारा से लेकर मालदेवता तक,
हर जगह नदी के प्राकृतिक प्रवाह और चौड़ाई की अनदेखी की गई है।
नदियों का "गला घोंटने" जैसे हालात बन गए हैं। नतीजतन, बारिश या बाढ़
की स्थिति में जलप्रवाह का दबाव बढ़कर आसपास की बस्तियों, सड़कों और
पर्यटक ढांचों पर कहर ढा देता है।हर मानसून में इन घाटियों में सीमित क्षेत्र
में दर्ज की जाने वाली अतिवृष्टि अब बड़े पैमाने पर तबाही की वजह बनने
लगी है। पर्यटन के नाम पर हो रहे इस अनियंत्रित और बिना मानकों वाले
निर्माण से न सिर्फ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि आपदा का खतरा
भी कई गुना बढ़ गया है।परिणामस्वरूप, पहाड़ और मैदान दोनों जगहों पर
भूस्खलन और भूधंसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। नदियां भी लगातार
उफान पर हैं, जिससे नदी किनारे बसे क्षेत्रों में भूकटान (किनारों का कटाव)
और तेज हो गया है। रिस्पना, बिंदाल और सहस्रधारा जैसे इलाकों में तो
जमीन दलदल की तरह नरम हो चुकी है।पहाड़ी प्रदेश की राजधानी होने के
नाते पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल मानसून में टूट पड़ने वाली आफत को दून ने
न सिर्फ देखा, बल्कि सरकारी मशीनरी का केंद्र होने के नाते वहां की पीड़ा
पर मरहम लगाने में भी अहम भूमिका निभाई। इस बार भी धराली से
लेकर थराली और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर टूटी आपदा में दून से ही राहत एवं
बचाव कार्यों को धार मिली।किसे पता था कि पहाड़ की आपदाओं पर
आधार स्तंभ बना रहने वाला देहरादून स्वयं इस कदर चौतरफा आपदा का
शिकार हो जाएगा। अब तक देहरादून में वर्ष 2011 में कार्लीगाड़ में बादल
फटने की घटना के साथ ही सौंग और बांदल घाटी में भी बदल फटने से
तबाही मचती रही हैं। लेकिन, उन आपदाओं का क्षेत्र विशेष तक सीमित
होने से राहत और बचाव कार्यों की चुनौती उतनी बड़ी नहीं होती
थी।लेकिन, इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी भी दूनवासी को उम्मीद
नहीं थी। अब तो मानसून ढलान पर था और सरकारी मशीनरी ने तो
वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत भी शुरू कर दी थी। मानसून
को अगले साल तक के लिए अलविदा कहने की तैयारी थी। लेकिन, विदा
लेने से पहले मानसून ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि शहर का चेहरा ही
बदल गया।देहरादून शहर के बाहरी इलाकों का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा
है, जहां कुदरत के कहर के गहरे निशान मौजूद न हों। जगह-जगह तबाही के
निशान हैं, चेहरों पर आंसू और गम की गहरी छाप है। गहरे दर्द के साथ दून
पूछ रहा है कि प्रकृति ने आखिर उस पर ऐसा कहर क्यों बरपाया? स्वतंत्र
भारत में उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने साथ वर्ष 2000 में नवगठित
उत्तराखंड की राजधानी का ताज भी हासिल किया। लेकिन, 349 सालों के
अपने उतार-चढ़ाव के तमाम दौर में ऐसी आपदा नहीं देखी, जो सोमवार
की आधी रात को इस आधुनिक शहर पर टूटी। इन आपदाओं के समय
आमजन और सिस्टम चुपचाप विनाश को देखने के लिए विवश होता है। इन
सभी संरचनाओं को आपदा सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी करके
अनुमति दी गई है, जिससे जोखिम और बढ़ गया है।उत्तराखंड आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य के विभिन्न भागों में स्थित उन्नीस
हजार सरकारी इमारतें भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति
संवेदनशील हैं। दून अस्पताल सहित 50 प्रतिशत स्कूल और अस्पताल भवन
भी इसी श्रेणी में आते हैं।भूकंपीय सुरक्षा संबंधी नियमों का आकलन किए
बिना ही हजारों पुराने मकानों में खतरनाक तरीके से अधिक मंजिलें और
संरचनाएं जोड़ने की अनुमति दी जा रही है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो
रही है, खासकर तलहटी क्षेत्रों में।इसलिए राज्य सरकार को आपदा के प्रभावों
को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के नौ सूत्री एजेंडे पर काम करना चाहिए
और सभी नई संरचना योजनाओं को संरचनात्मक इंजीनियरों के माध्यम से
पारित करने और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बनाए जाने वाले
एक अलग शहरी विकास निगरानी सेल द्वारा उनकी मंजूरी लेने के लिए सख्त
नियम बनाने चाहिए।आपदाओं के कारणों और उनके प्रभाव को कम करने के
तरीकों को समझने के लिए स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जागरूक
करने पर शायद ही कोई ज़ोर दिया जाता है। एक ज़ोरदार अभियान की
ज़रूरत है और शहरी विकास एजेंसियों को अनिवार्य रूप से प्राधिकरण से
आपदा प्रबंधन सलाह लेनी चाहिए।उचित आपदा प्रबंधन को क्रियान्वित करने
में सबसे बड़ी चुनौती शहरी एजेंसियों में राजनीतिक स्वार्थों के चलते अंधाधुंध
अनुमति व्यवस्था से आती है। घनी आबादी वाले इलाकों में खतरनाक जगहों
पर स्थित इमारतें, संकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों में विशाल
मॉल, खेल के मैदानों पर विशाल कंक्रीट की संरचनाएं (देहरादून का प्रसिद्ध
परेड ग्राउंड ऐसी इमारतों की भेंट चढ़ गया है), आधे से ज़्यादा शहरों के पास
मास्टर प्लान नहीं हैं, प्रभावशाली अभिजात वर्ग का शहर के मुख्य इलाकों में
निवेश करने का दबदबा और आम नागरिकों के लिए सांस लेने की जगहों का
दम घुटना, और आर्द्रभूमि और नदी तटों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है।
योजनाकारों की अदूरदर्शिता के कारण देहरादून ने अपनी दो खूबसूरत नहरें –
पूर्वी और पश्चिमी – खो दीं। हमने हज़ारों लीची और आम के पेड़ खो दिए और
दस फुट चौड़ी सड़कों पर अब बहुमंजिला अपार्टमेंट बन गए हैं, जहाँ से प्रवेश
करना या बाहर निकलना मुश्किल है। स्कूलों को पीछे धकेल दिया गया है,
लेकिन सात सितारा होटल बन गए हैं जहाँ ट्रैफ़िक जाम अब निवासियों का
जीवन नरक बना रहा है।हमारे ज़्यादातर शहरों में जल निकासी का बुनियादी
ढाँचा नहीं है। इसके अलावा, प्राकृतिक भू-भाग और जल-भू-आकृति विज्ञान
की अज्ञानता शहरी बाढ़ को मानव-निर्मित आपदा बना देती है।जब कोई
आपदा आती है, तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और फिर राजनेताओं,
विशेषज्ञों, मीडियाकर्मियों का आना-जाना, किताबें और भारी-भरकम
रिपोर्ट तैयार करना आम बात हो जाती है। लेकिन क्या हम प्रधानमंत्री के
आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंत्र को अक्षरशः लागू करने के लिए एक
संवेदनशील दूरदर्शी जैसी सजगता दिखा सकते हैं? इसका कोई विकल्प नहीं
है। बहाली की कोशिश परवान चढ़ेग! *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के*
*जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*