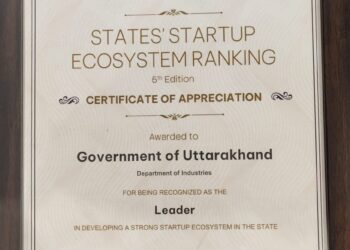डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला:
मध्य हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड का हस्तशिल्प सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। फिर चाहे वह काष्ठ शिल्प हो, ताम्र शिल्प अथवा ऊन से बने वस्त्र। सभी की खूब मांग रही है। हालांकि, बदलते वक्त की मार से यहां का हस्तशिल्प भी अछूता नहीं रहा है। हस्तशिल्पियों और बुनकरों को पूर्व में राज्याश्रय न मिलने का ही नतीजा रहा कि यह कला सिमटने लगी है।उत्तराखंड के पहाड़ों में हर घर की शान बढ़ाने वाली काष्ठ कला अब स्मृति चिन्हों तक सिमट गई है।
किसी जमाने में घर बनाने से लेकर घरेलू उपयोग में आने वाले लकड़ी के सामान में नक्काशी का प्रचलन था। लेकिन अब काष्ठ कला धीरे-धीरे लुप्त हो रही है।पहाड़ों में भी सीमेंट व कंकरीट के मकान बनने से गांवों में प्राचीन काष्ठ कला के नमूने देखने को मिलते हैं। मकान बनाने के लिए लकड़ी न मिलने से अब यह काष्ठ कला काम भी खत्म हो रहा है। इससे इस व्यवसाय से हस्तशिल्प भी आजीविका के लिए दूसरे साधन अपनाने को पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं।किसी जमाने में उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प में एक अलग पहचान थी। गांवों में पुराने मकानों के दरवाजों, खिड़कियों पर आज भी प्राचीन काष्ठ कला ने अपनी छाप छोड़ी है।
हस्तशिल्पियों के हाथों से लकड़ी पर उकेरी गई नक्काशी हर घर की शान होती थी। वहीं, लकड़ी से पाली, ठेकी, कुमैयां भदेल, नाली समेत अन्य प्रकार के बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता है।वर्तमान में काष्ठ कला से जुड़े परिवारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट हो गया है, जिससे वे अब दूसरे व्यवसाय को अपनाने के लिए पलायन करने को विवश हैं। काष्ठ कला के हस्तशिल्पियों का कहना है कि सरकार को इस प्राचीन हस्तशिल्प कला पर गंभीरता से ध्यान दिया देना चाहिए।
बढ़ती आधुनिकता के साथ लकड़ी से बने परम्परागत उत्पाद हमारे जीवन से दूर होते-होते अब लगभग लगभग समाप्त हो चुके हैं और उत्तराखण्ड में काष्ठशिल्पपूरी तरह बरबाद हो चुका है यह बात किसी से भी छिपी नहीं हैकठयूड़ी, पाल्ली, हड़प्या, ठेकी, बिंडो, पारो, नाली, मानो, बैगर, ढाड़ो, चाड़ी, कुमली लकड़ी से बनने वाले कुछ ऐसे बर्तन हैं जो एक समय उत्तराखंड के हर घर में मिलते थे. आज यह बर्तन हमारे घरों से ही नहीं हमारे शब्दकोश तक से गायब हो चुके हैं.घरो की चौखट पर बनने वाले देवी-देवता, पेड़-पौधे, जानवरों, फूलों, यक्ष-यक्षिणियों के मोटिफ हमेशा-हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं.गेठी और सानन की लकड़ी से बनने वाले यह लकड़ी के बर्तन उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड की हर रसोई में देखने को मिल जाते थे. अब ये बर्तन ढूंढने पर ही मिलेंगे. सालन और गेठी से बनी लकड़ी लम्बे समय तक सड़ती नहीं है इसलिये इसका प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता रहा है.पीढ़ियों से बर्तन बनाने की इस विरासत को उत्तराखंड के चुनार जाति के दस्तकारों ने संभाला है.
उन्हें स्थानीय भाषा में चुनेरे कहा जाता है. मूलरुप से बागेश्वर जिले के रहने वाली ये लोग हर साल रामनगर में आकर कोसी और बौर नदी किनारे अपना डेरा जमाकर पनचक्की की मदद से लकड़ी के बर्तन तैयार करते हैं.ये लोग हर साल फरवरी से अप्रैल तक नदी के किनारे अपनी खराद लगाते हैं. खराद पर लकड़ी के टुकड़ों को अपने अनुभवी और कुशल हाथों से संवार कर सुन्दर बर्तनों में बदल देते हैं. आज इनकी माली-हालत बहुत ख़राब हो चुकी है.बर्तन बनाने की जरुरत की लकड़ी ये लोग वन विभाग से कर चुकाकर पाते हैं. तीन-तीन महिने अपने परिवार से दूर नदी के निर्जन किनारे पर बर्तन बनाकर भी दो वक्त की रोटी निकाल पाना इनके लिये मुश्किल है.
कठ्यूड़ी कटोरे के समान चौड़े मुख और कम उंचाई वाला एक बर्तन है. समतल आधार और किनारे उंचाई वाली वाली दीवारों से बना बर्तन ठेकी कहलाता है. ठेकी का प्रयोग दही ज़माने के लिये किया जाता था.इसी तरीके का कम उंचाई वाला बर्तन हड़प्या कह लाता है जिसका उपयोग दही रखने के लिये किया जाता था.बिंडा अब भी पहाड़ों में प्रयोग में लाया जाने वाला एक लकड़ी का बर्तन है. बिंडा सामान्य रूप से ढक्कन वाला बनता है जिसका उपयोग दही मथने में किया जाता है. पशुओं को पानी आदि पिलाने के लिये’ दूने का प्रयोग किया जाता है.नमक रखने के लिये नमी को सोखने वाले तुन की लकड़ी का करुवा नामक छोटा बर्तन बनाया जाता था. तुन की लकड़ी के ही आटा गूंथने व अन्य कार्य को बड़ी पाई या परात का इस्तेमाल होता था.
छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए केतलीनुमा गड़वे का प्रयोग होता था. वहीं कटोरी के रूप में फरवा प्रयोग में किया जाता था.उत्तराखंड की संस्कृति एवं जनजीवन से ताल्लुक रखने वाली पारम्परिक काष्ठ से निर्मित वस्तुएं अब संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैबर्तनों के अलावा, काष्ठ हस्तकला की रचनात्मकता भवनों और मंदिरों में भी देखी जा सकती थी, जहां लकड़ी के दरवाजों और भीतरी छतों पर सजावट के लिए नक्काशी की जाती थी. काष्ठ हस्तकला में देवी-देवताओं की आकृतियां भी बनाई जाती थी.
बिजली से चलने वाली खराद मशीनों और प्लाईवुड के आज के ज़माने में गढ़वाल और कुमाऊं में अब उंगली में गिनती के घर ऐसे होंगे जिनमें यह नक्काशी आज भी बनायी जाती होगी. काष्ठ कला के हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिए श्रीनगर के पापड़ी में खुला काष्ठ कला केंद्र बंद पड़ा है। अब यहां पर न तो प्रशिक्षण दिया जाता और न ही काष्ठ कला को बढ़ावा देने के लिए कोई गतिविधियां चल रही है।
यदि सरकार इस केंद्र का विस्तारीकरण कर शिल्पियों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दे तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इस पहल को पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर उतारना सुनिश्चित करे. पिछले कई वर्षों से कला के प्रति रुचि घटती चली गई। आजादी के बाद तो कारीगर ही नहीं नजर आए। सरकार की ओर से संरक्षण की कोई पहल नहीं हुई। नई पीढ़ी के लिए तो यह विधा सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट गई है।