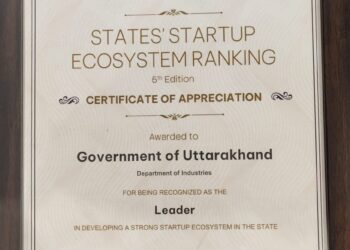डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला:
थुलमा भेड़ की ऊन से बनने वाला विशेष प्रकार का कम्बल है। थुलमा पिटलूम (एक प्रकार का खांचा) में बनाया जाता है। चार हिस्सों में ऊन बुनी जाती है। जिन्हें बाद में आपस में जोड़ा जाता है। अभी तक सीमांत में सफेद, काले रंग के ही थुलमे बनते हैं। ऊन की रंगाई नहीं होने के कारण यह दिखने में ज्यादा आकर्षक नहीं होता, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से यह बेहतरीन है। हीट इंसुलेटर का काम करने वाले एक ही थुलमा शून्य से नीचे तापमान में भी शरीर को खासी गर्मी देता है।
उच्च हिमालयी क्षेत्र में शीतकाल में ठंड से बचाव के लिए इसी का उपयोग होता है। एक थुलमे की कीमत 2200 से 2500 रुपये के बीच होती है। चीन सीमा से लगे धारचूला और मुनस्यारी के हस्तशिल्प थुलमा को जीआइ टैग (भौगोलिक संकेत) मिलना बड़ी उपलब्धि है। दम तोड़ रहे इस उद्यम के अब फिर से रफ्तार पकडऩे की उम्मीद बढ़ गई है। जीआई टैग मिल जाने के बाद अब कारीगरों को इसकी गुणवत्ता के लिए ग्राहकों को सफाई नहीं देनी होगी। ग्लोबल ब्रांड बनने की उम्मीदों के बीच थुलमा चाइनीज कंबलों से मुकाबला कर सकेगा। राज्य की सीमांत तहसील धारचूला और मुनस्यारी के लोग सदियों से हस्तशिल्प के कारोबार से जुड़े हैं।
दन, कालीन, पंखी, चुटके के साथ ही थुलमा भी बनाया जाता है। कभी सीमांत के इस हस्तशिल्प की बाजार में भारी मांग हुआ करती है। यहां के उत्पाद देश भर में पहुंचते थे। 1991 में देश में शुरू हुए उदारीकरण के बाद सीमांत का हस्तशिल्प पिछडऩे लगा। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण का अभाव इसका सबसे बड़ा कारण रहा। बावजूद इसके दोनों तहसीलों में अभी भी 200 परिवार हस्तशिल्प के कारोबार से जुड़े हैं। सीमांत के थुलमा उद्यम को अब जीआइ टैग (भौगोलिक संकेत) मिल गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इससे थुलमा की ब्रांडिंग होगी और उद्यम रफ्तार पकड़ेगा। 1962 से पहले थुलमा बनाने के लिए तिब्बत से ऊन आती थी।
सीमांत के व्यापारी तिब्बत से ऊन लाकर स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराते थे। 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद तिब्बत से ऊन आना बंद हुआ तो भारत ने सीमांत में पशुपालन विभाग के माध्यम से भेड़ पालन को बढ़ावा दिया। अब क्षेत्र ऊन उत्पादन के मामले में निर्भर हो चुका है। आस्ट्रेलियन भेड़े भी अब सीमांत में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे आने वाले दिनों मेें ऊन का उत्पादन और बढ़ेगा। 93 वर्षीय वयोवृद्ध व्यापारी का कहना है कि थुलमा उद्योग को बढ़ाने के लिए उसे आधुनिक तकनीक से जोड़े जाने की जरू रत है। नए यंत्रों के साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशिक्षण देकर सीमांत में रोजगार के नए अवसर बनाए जा सकते हैं।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि जीआइ टैग मिलने से अब थुलमा की ब्रांडिंग हो सकेगी। गुणवत्ता को लेकर खरीदारों में अब किसी तरह का संशय नहीं रहेगा। इससे थुलमा के दुनिया के ठंडे देशों में निर्यात के अवसर बढ़ेंगे। सीमांत मुनस्यारी-धारचूला का ऊन कारोबार पांच दशक पहले तक प्रमुख व्यापार में शामिल था। मुनस्यारी, धारचूला के लोग पहले तिब्बत की ज्ञानिमा और तकलाकोट मंडी से व्यापार करते थे।
वहीं से तिब्बती भेड़ों का ऊन खरीदकर घोड़े-खच्चरों, भेड़-बकरियों में लादकर लाते थे। इसके बाद ऊन के कपड़े तैयार किए जाते थे। तिब्बत से लाया जाने वाले काले और सफेद ऊन को मिलाकर ग्रे कलर (स्थानीय भाषा में भन्नेन रंग) बनाया जाता था। कताई, सफाई, रंगाई करके कोट, पंखी, दन-कालीन, आसन, मफलर, टोपी बनाकर बाजार में बेचे जाते थे। कारोबार को उबारने के लिए तकनीक के साथ ही प्रशिक्षण, सरकारी अनुदान एवं बाजार उपलब्ध कराने की भी दरकार है।1907 में जोहार- दारमा तथा ब्याँस के मार्गों से केवल दो लाख रुपए की ऊन का आयात किया गया।
नीती घाटी से होने वाले ऊन के आयात कमी आई और माणा के मार्ग से होने वाला आयात बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक काफी कम हो गया। ऊन के कारोबार को सर्वाधिक हानि भारत वर्तमान में भी मशीन से निर्मित अपेक्षाकृत काफी सस्ते उत्पादों से प्रतियोगिता के कारण ऊन तथा अन्य तंतुओं से संबन्धित हस्तशिल्प के अस्तित्व पर संकट है। फिर भी स्थानीय स्तर पर आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण आज भी होता है।
परंपरागत रूप से चली आ रही ऊन के उत्पादों से संबन्धित तकनीक में केवल इतना ही अन्तर आया है कि कताई से पहले ऊन को धोने की प्रक्रिया के बाद उसे अलग करने के लिए जहाँ पहले कंघेनुमा ब्रुश का प्रयोग होता था] वहींवर्तमान में कार्डिंग प्लांट का प्रयोग होने लगा है।\
उद्योग विभागजनजाति विभाग खादी बोर्ड आदि के द्वारा स्थानीय निवासियोंको कच्चा ऊन दिया जाना भी बन्द कर दिया गया है। उसके स्थान पर अब ऋण दिये जाने लगे हैं। पर्वतीय अंचल में उत्पन्न होने वाली बिच्छू घास के रेशों को भी वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाने का प्रयास हो रहा है, परंतु अभी यह बड़े पैमाने पर सामने नहीं आया है।
उत्तराखण्ड के इस हस्तशिल्प की मूल्यवान विरासत को संरक्षित करने तथा शिल्पियों द्वारा अपनायी जाने वाली तकनीक का वर्तमान तकनीक के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए संवर्धित किये जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड का प्राचीन हस्तशिल्प कालीन उद्योग तकनीकी युग में धीरे-धीरे सिमट रहा है। जबकि किसी जमाने में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जैसे दूरदराज के पर्वतीय जिले कभी इसी उद्योग से फल फूल रहे थे। लेकिन अब युवा पीढ़ी की इस पारंपरिक हस्तशिल्प से दूरी बना कर पलायन मजबूर बन गई है।आजीविका के तौर पर युवा पीढ़ी इस पुस्तैनी कारोबार को अपनाना नहीं चाहती है। रोजगार के अन्य विकल्प तलाशने के लिए पलायन कर रहे हैं।
पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी पिथौरागढ़ से युवाओं ने रोजगार के लिए पलायन किया है। यदि सरकार इस परंपरागत उद्योग को आधुनिक स्वरूप दे तो युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन सकता है। कभी पूरे देश में अलग पहचान रखने वाले धारचूला-मुनस्यारी के दन कालीन का कारोबार अब सिमटने लगा है। चीन और कोरिया सहित मशीनों में निर्मित आकर्षक डिजाइन के कपड़ों के बाजार में आने से परंपरागत हस्तशिल्प को नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार में मांग घटने से युवा पीढ़ी हस्तशिल्प से किनारा करने लगी है। धारचूला और मुनस्यारी में कभी पांच हजार से अधिक परिवार ऊनी हस्तशिल्प पर निर्भर थे।
बाकी जनजातियों के मुकाबले भोटिया समाज की हालत काफी बेहतर है। पहले तिब्बत के साथ व्यापार से हुई आमदनी से ये जीवनयापन करते थे । भोटिया जनजाति के लोग यहां से ऊनी कपड़े और नमक आदि ले जाकर तिब्बत में बेचते थे। इस व्यापार में भाषा भी कभी आड़े नहीं आती थी। भोटिया जनजाति के लोग मनमाफिक कीमत ना मिलने तक अपने हाथों से सामान को ढक लिया करते थे । जब मनमाफिक कीमत मिल जाती थी तभी वो सामान दिया करते थे लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पारंपरिक रूप से चला आ रहा ये व्यापारिक रिश्ता खत्म हो गया ।
ऐसे में ये अपना सामान आसपास की आबादी को बेचने के लिए मजबूर हो गए हालांकि इन्होंने अभी तक अपना पारंपरिक व्यवसाय नहीं छोड़ा है । इऩके गावों में हर घर में रांच होती है । जिस पर ये वॉल हैंगिंग, कालीन जैसी तमाम चीजें बनाते हैं । ऊनी कपड़े बनाने में भी ये माहिर हैं लेकिन अपना सामान बेचने में इन्हें कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं । कोई ठोस व्यापारिक नीति नहीं होने और सरकारी मदद नहीं होने की वजह से धीरे धीरे इस व्यापार पर असर पड़ने लगा है ।
राज्य के लिए यह गौरव का विषय है कि यहां के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। वोकल फार लोकल और स्थानीय उत्पाद के प्रचार-प्रसार में जीआइ टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में और भी ऐसे उत्पाद हैं जो भौगोलिक क्षेत्र विशेष के आधार पर अपनी वैश्विक पहचान बना रहे थुलमा शामिल हैं।