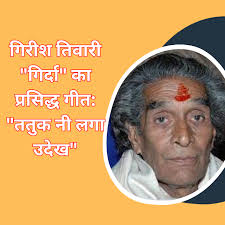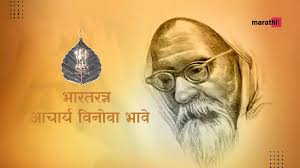डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता था, अब आपदाओं की भूमि बन गया है।
बारिश, भूस्खलन, बादल फटना, नदी का रुख बदल जाना — अब ये आम हो
गया है। हर मानसून एक गांव बहा ले जाता है, हर बरसात किसी के घर उजाड़
जाती है, और हर बारिश एक नई लाश गिनती है। लेकिन इसके बावजूद सरकारें
चुप हैं, योजनाएं गूंगी हैं और जनता बेबस।जिसे हम विकास कहते हैं, दरअसल
वह विनाश का दूसरा नाम बन चुका है। पहाड़ों पर सड़कें बनाने के लिए
डायनामाइट से विस्फोट किए जाते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है। पूरी की
पूरी पर्वत श्रृंखलाएं काटी जाती हैं, ताकि टनल बने, चौड़ी सड़कें बनें, जल
परियोजनाएं बनें। लेकिन ये सब किस कीमत पर? प्रकृति की शांति और संतुलन
को तोड़कर हम क्या हासिल कर रहे हैं? जो सड़कें सुरक्षा लानी चाहिए थीं, वे
अब मौत की राह बन गई हैं। जो टनल सुगमता का वादा करती थीं, वे अब
आपदा का द्वार बन चुकी हैं।पर्यटन के नाम पर उत्तराखंड का जिस तरह से दोहन
किया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है। सैकड़ों गाड़ियाँ, हजारों पर्यटक, प्लास्टिक का
पहाड़, ट्रैफिक की कतारें यह सब मिलकर उत्तराखंड के पर्यावरण पर ऐसा बोझ
डाल रहे हैं, जिसे अब पहाड़ सह नहीं पा रहे। कभी यहां गर्मियों में पंखा नहीं
चलता था, अब अक्टूबर में भी लोग एसी चला रहे हैं। यह सिर्फ जलवायु
परिवर्तन नहीं, यह चेतावनी है कि हमने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं।बाहरी
लोग भारी संख्या में आकर जमीनें खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, कॉलोनियां उगा
रहे हैं। स्थानीय लोगों की जमीनें औने-पौने दामों में छीनी जा रही हैं। संस्कृति
खतरे में है, भाषा गुम हो रही है, और पहचान मिट रही है। उत्तराखंड अब उत्तर-
हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुका है। जो भूमि कभी साधु-संतों की थी, अब रियल
एस्टेट माफिया की गिरफ्त में है। और सरकारें बस तमाशबीन बनी बैठी
हैं।दिल्ली से उत्तराखंड तक एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इस पर कोई गर्व महसूस
कर सकता है, लेकिन जो लोग उत्तराखंड की आत्मा को जानते हैं, उन्हें पता है
कि यह सड़क उस दरवाजे की आखिरी कड़ी होगी जो शांति की ओर जाता था।
यह मार्ग विकास के नाम पर उत्तराखंड की आत्महत्या की कहानी बन जाएगा।
अभी तो वीकेंड में ही दिल्ली से हजारों लोग आते हैं, सोचिए जब यह सड़क पूरी
होगी और हर दिन लाखों की भीड़ पहाड़ों पर चढ़ेगी — तब क्या बचेगा
यहां?विनाश का यह सिलसिला नियमों की कमी से नहीं, नियत की कमी से है।
पर्यावरणीय रिपोर्टें बस एक औपचारिकता बन चुकी हैं। परियोजनाओं को मंजूरी
देने वाले अधिकारी जानते हैं कि उनका हर हस्ताक्षर एक पेड़ को मार रहा है,
एक चट्टान को कमजोर कर रहा है, एक गांव को डुबो रहा है। लेकिन धन, पद
और प्रभाव के आगे ये सारी चेतावनियां बेअसर हो जाती हैं। इसीलिए तो आज
स्थिति यह है कि हिमालय जैसा अचल पर्वत भी थरथराने लगा है।यह केवल
प्राकृतिक संकट नहीं, यह हमारी नैतिक विफलता भी है। हमने न सिर्फ पेड़ काटे,
बल्कि भरोसे भी काट डाले। नदियों की धारा मोड़ी, तो साथ में भविष्य भी मोड़
दिया। हम भूल गए कि हिमालय सिर्फ बर्फ से नहीं बना, वह आस्था से बना है,
संतुलन से बना है। और इस संतुलन को तोड़ने की हमारी कोशिश अब हर
बरसात में लाशों की गिनती बढ़ाकर जवाब दे रही है।समाधान कठिन है, पर
असंभव नहीं। हमें तत्काल प्रभाव से नई निर्माण परियोजनाओं पर रोक लगानी
होगी। पहाड़ों की सहनशीलता को विज्ञान से नहीं, विवेक से समझना होगा।
पर्यटन को सीमित करना होगा उसके लिए जैसी अवधारणाओं को गंभीरता से
लागू करना होगा। पर्यटकों की संख्या तय हो, वाहनों की सीमा तय हो, और
सबसे जरूरी स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना कोई भी निर्णय न लिया
जाए। आपदा का दंश झेल रहे उत्तराखंड की नजरें अब इससे उबरने को केंद्रीय
मदद पर टिक गई हैं। राज्य की ओर से 5700 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का
प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम राज्य के
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षति के आकलन में जुटी है। जमीन की खरीद-फरोख्त
पर रोक लगानी होगी। यह जरूरी है कि कोई बाहरी व्यक्ति पहाड़ में जमीन
खरीदने से पहले उस भूमि की संस्कृति और पारिस्थितिकी को समझे। नहीं तो
वह सिर्फ एक नया खतरा लेकर आएगा।शिक्षा के स्तर पर हमें जलवायु संकट
और पर्यावरणीय जागरूकता को स्कूलों से जोड़ना होगा। बच्चों को यह सिखाना
होगा कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे पहाड़ों को थामे रहते हैं। नदी सिर्फ
पानी नहीं देती, वह जीवन देती है। चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं होतीं, वे इतिहास,
भूगोल और संस्कृति की नींव होती हैं। अगर अब भी हम नहीं रुके, तो अगली
बार यह हादसा किसी और गांव में नहीं, आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। दिल्ली,
देहरादून, हल्द्वानी, मसूरी — कोई सुरक्षित नहीं बचेगा।उत्तराखंड सिर्फ एक
राज्य नहीं, वह एक चेतना है। उसे बचाना केवल स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी
नहीं, यह पूरे देश की जिम्मेदारी है। सरकारों को अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, कठोर
और साहसी निर्णय लेने होंगे। वरना वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड का हर
गांव एक थराली बन जाएगाऔर फिर हम सिर्फ शोक सभा कर पाएंगे, समाधान
नहीं।आज समय है संकल्प लेने का। समय है यह स्वीकार करने का कि हमने
गलती की है — और समय है उसे सुधारने का। अगर अभी नहीं चेते, तो हम
इतिहास में दर्ज हो जाएंगे उन लोगों के रूप में, जिन्होंने देवभूमि को विनाशभूमि
बना दिया। साल 2013 के केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से
गठित विशेषज्ञ समिति ने बताया था कि उच्च हिमालयी घाटियां भूस्खलन और
मलबा प्रवाह प्रभुत्व वाली अचानक बाढ़ों की चपेट में आ सकती हैं. इस समिति
ने सिफारिश की थी कि उच्च हिमालयी घाटियों में भगीरथी पर्यावरण-
संवेदनशील क्षेत्र (बीईएसजेड) जैसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों का चिह्नांकन
किया जाना चाहिए. इससे उच्च हिमालयी घाटियों में मानवजनित हस्तक्षेप को
न्यूनतम किया जा सकेगा.समिति ने सुझाव दिया था कि नदियों को मानवजनित
अतिक्रमण और जलबिजली बैराज से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ के
दौरान नदी बिना किसी रुकावट के बह सके.उनका कहना है कि इन सिफारिशों
को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसके बजाय निर्माण सामग्री, लकड़ी या जमीन
का अत्यधिक दोहन किया गया. उत्तराखंड में लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं
केवल पर्यावरणीय घटनाएं नहीं हैं, अपितु वे हमारे विकास मॉडल, नीति-
निर्धारण एवं प्रकृति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर गहरे प्रश्नचिह्न खड़ा करती
हैं। भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, वनाग्नि और भू-धंसाव जैसी घटनाएँ न केवल
राज्य की पारिस्थितिकी को, बल्कि उसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना को
भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं।यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन तथा
मानवीय हस्तक्षेप की संयुक्त परिणति ने उत्तराखंड को आपदा-प्रवणता की चरम
सीमा तक पहुँचा दिया है। ऐसी परिस्थिति में मात्र तात्कालिक राहत उपाय
पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता है एक दीर्घकालिक, पर्यावरण-संवेदी और समुदाय-
आधारित नीति दृष्टिकोण की, जो विकास को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व के रूप
में पुनर्परिभाषित करे।इस दृष्टिकोण में सतत विकास, पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय
भागीदारी और वैज्ञानिक विवेक का संतुलन अनिवार्य है। उत्तराखंड की जैव-
विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और संवेदनशील पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु यह
अत्यावश्यक है कि हम अब सजग होकर ठोस कार्यवाही करें।अतः, राज्य सरकार,
वैज्ञानिक संस्थान, गैर-सरकारी संगठन और स्थानीय समुदायों को मिलकर एक
साझा, समावेशी और पर्यावरणोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक
विकास को ‘प्रकृति-विरोधी लाभ’ के बजाय ‘प्रकृति-संगत जीवन’ के रूप में
पुनर्परिभाषित नहीं किया जाएगा, तब तक उत्तराखंड की आपदाएं निरंतर तीव्र
होती रहेंगी।यही समय है जब हमें चेतने, सीखने और ठोस बदलाव लाने की
दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अन्यथा वह समय दूर नहीं जब 'देवभूमि' की पहचान
केवल त्रासदियों और आपदाओं तक सीमित होकर रह जाएगी। हमें अब 'प्रकृति
के अनुरूप विकास' की राह अपनाने का सार्थक संकल्प लेना होगा, इसी में
उत्तराखंड की दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि निहित है।इससे हिमालयी
पर्यावरण पर अत्यधिक बोझ डालना निर्बाध रूप से जारी रहा.इन दोनों
वैज्ञानिकों ने कहा है कि भगीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (बीईएसजेड)
अधिसूचना को लागू किया जाए. उनका कहना है कि हिमालय की अमूल्य जैव
विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का विस्तार लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे ऊपरी
हिमालयी घाटियों तक किया जाना चाहिए. इससे जलवायु परिवर्तन के कारण
हिमालय पर मंडराने वाले आपदा जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी. *लेखक*
*विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*