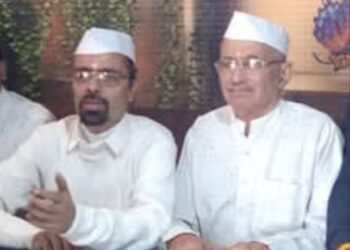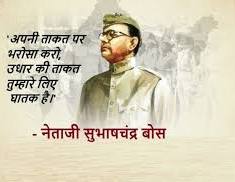डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
देवदार को ‘देवताओं की लकड़ी’ माना जाता है और इसे इसके औषधीय, धार्मिक और व्यावसायिक उपयोगों के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया है। संस्कृत में इसे ‘देवदारु’ कहा जाता है, जिसमें ‘देव’ का अर्थ है ‘ईश्वर’ और ‘दारु’ का अर्थ है ‘वृक्ष’। इसे ‘सुरदारु’ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ‘जो देवभूमि में उत्पन्न होता है’। यह वृक्ष मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिमी हिमालय (पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान) में पाया जाता है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग में पाया जाता है।देवदार एक सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है जो लगभग 40 से 50 मीटर ऊँचा होता है। इसकी छाल काली-भूरी होती है, जिसमें लम्बवत दरारें होती हैं। इसकी पत्तियाँ सुई जैसी होती हैं और यह वृक्ष नर और मादा दोनों प्रकार के फूल उत्पन्न करता है। शंकुएकल या जोड़े में उत्पन्न होते हैं, जो परिपक्व होने पर नीले से भूरे-लाल रंग के हो जाते हैं। प्राचीन काल में देवदार वनों को ध्यान और तपस्या के लिए पवित्र माना जाता था। यह भगवान शिव को समर्पित वृक्ष माना जाता है। वेदकाल में इसकी सुगंधित लकड़ी से मंदिर और अगरबत्तियाँ बनाई जाती थीं। यह माना जाता था कि इसकी छाया में बैठने से अस्थमा और अन्य बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं।पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, जो विशालकाय होने के साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं. सेहत के लिए तो ये फायदेमंद होते ही हैं, साथ ही ये प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं. आध्यात्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व भी होता है. ऐसे में ये ऊंचे-ऊंचे पेड़ बेहद अनमोल होते हैं. ऐसा ही एक वृक्ष है देवदार या दावदारु का. यह एक विशाल और बेहद ऊंचा पेड़ होता है.देवदार या देवदारु का वृक्ष आपको हिमालय की पहाड़ियों में देखने को मिल जाएगा. इसे देवताओं की लकड़ी के रूप में जाना जाता है. इस पेड़ का हर भाग महत्वपूर्ण है और सभी का इस्तेमाल कई तरह के विभिन्न औषधीय लाभों के लिए किया जाता है. देवदार का पेड़ उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में उगता है. इसकी ऊंचाई 40-60 मीटर तक हो सकती है. इसकी शंकुधारी पत्तियां और सुगंधित लकड़ी इसे विशिष्ट बनाती हैं.हिंदू धर्म में देवदारु को पवित्र माना जाता है. पुराणों में इसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है. कई धार्मिक स्थलों पर इसके वृक्ष लगाए जाते हैं. इसकी शीतल छाया और सुगंधित वातावरण ध्यान और योग के लिए बेहतर माहौल प्रदान करते हैं. आयुर्वेद में देवदार का खास स्थान है. इसकी पत्तियां, तेल, छाल, राल का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, देवदारु में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं. इसका तेल जोड़ों के दर्द, गठिया और मांसपेशियों की अकड़न को कम करने में प्रभावी है. इसके अलावा यह त्वचा रोगों में भी उपयोगी है.-आपको सर्दी-जुकाम, खांसी हो तो देवदार काफी कारगर हो सकता है. शरीर से अतिरिक्त कफ बाहर निकालता है. इसमें मौजूद गुण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बलगम निकालकर खांसी जैसे कफ विकार रोगों से राहत दिलाने में मदद करता है. देवदार उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी काष्ठीय है। प्राचीनकाल से ही इसका उपयोग मंदिरों एवं भवन निर्माण में होता रहा है। विगत कुछ दशकों से इसका इस्तेमाल रेलवे के स्लीपरों में हो रहा था। परन्तु इसकी टीजी से घटती संख्या के चलते इसे रोक दिया गया है। इसकी उच्च गुणवत्ता लकड़ी उत्पाद है। इसकी लकड़ी में पसीना व मूत्र बढ़ाने वाले औषधीय गुण पाये जाते हैं। बुखार, बबासीर, फेफड़ों एवं मूत्राशय संबंधी रोगों में देवदार प्रयुक्त होता है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में इसकी लकड़ी का पेस्ट चन्दन की तरह ललाट पर लगाया जाता है तथा ऐसी मान्यता है कि इससे सिरदर्द ठीक हो जाता है। देवदार की छाल भी औषधीय महत्व की होती है तथा इसका उपयोग बुखार, अपच, दस्त आदि रोगों में होता है। देवदार का ऑलिव- रेजिन तथा इसकी लकड़ी के विनाशात्मक संघनन से प्राप्त तेल का उपयोग अल्सर एवं त्वचा रोगों में होता है। देवदार के तेल की माँग इत्र, साबुन, तथा अन्य कई उद्योगों में है।देवदार के उपयोगों एवं इसकी लकड़ी की बढ़ती माँग के चलते इसके वर्तमान वनों के संरक्षण एवं नए वनों के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके वनों को आग एवं बर्फ के अलावा करीब ६० प्रकार के कीड़े भी हानि पहुँचाते हैं। आज के युग की जरुरत है कि इसकी प्रजाति के वनों को पूर्णतः सुरक्षित बनाया जाय और वनों की तेजी से वृद्धि की जाए ताकि इस वृक्ष की रक्षा व संवर्धन हो सके। उत्तराखंड के हिमालयी वृक्ष देवदार का पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी पहचान का अभिन्न अंग है। इसकी ऊंचाई, सुगंधित सुगंध और मजबूत लकड़ी ने इसे सदियों से श्रद्धा और महत्व दिलाया है। उत्तराखंड की पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ समझा जाने वाला देवदार का संबंध भगवान शिव से है। इसकी सदाबहार प्रकृति अमरता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। “देवदार” शब्द का शाब्दिक अर्थ ही “देवताओं की लकड़ी” है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि ये वन कभी देवताओं का निवास स्थान थे। देवदार की लकड़ी को पवित्र मानकर विभिन्न धार्मिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। प्राचीन पसंद वाले लोगों को देवदार की लकड़ी बहुत आकर्षक लग सकती है। हालांकि, उपयोग के लिए लकड़ी का पालन करने से पहले उसकी विशेषताओं को महसूस करना महत्वपूर्ण है। देवदार की लकड़ी की बात करें तो कुछ ऐसे कारण हैं जो पाइनवुड को फर्नीचर के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।चीड़ की लकड़ी हल्के रंग की लकड़ी होती है। इसमें एक बहुत ही पीला मूल रंग है जो लकड़ी को दागने और नए रंगों के अनुकूल बनाने में आसान बनाता है। यह हल्के रंग के शरीर और गहरे रंग की गांठों के साथ अपने विशिष्ट रूप के लिए भी लोकप्रिय है। यह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, और यदि वांछित है, तो इसे अपनी मूल त्वचा के साथ एक स्पष्ट कोट के साथ भी छोड़ा जा सकता है जो एक असाधारण रूप भी देता है।देवदार की लकड़ी हल्की होती है। जबकि देवदार की लकड़ी के फर्नीचर का वजन काफी हो सकता है, जब ओक के फर्नीचर की तुलना में, देवदार की लकड़ी बहुत हल्की और संभालने में आसान होती है। फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करने या एक के निर्माण का मामला हो, देवदार की लकड़ी की हल्की प्रकृति इससे संबंधित किसी भी बोझ को रोकती है।देवदार की लकड़ी सबसे सस्ती लकड़ी है। देवदार की लकड़ी को आमतौर पर इसकी सस्ती प्रकृति के कारण भी जाना जाता है। यह पूरी दुनिया में उगाया जाता है, और इसे किसी भी अन्य लकड़ी की तुलना में तेजी से उगाया जा सकता है। यदि कोई बजट के तहत फर्नीचर की तलाश में है, तो देवदार की लकड़ी उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर सकती है।कठोर और सदमे प्रतिरोधी लकड़ी। देवदार की लकड़ी की कठोरता टिकाऊ और मजबूत फर्नीचर बना सकती है। हालांकि ओक जितना मजबूत नहीं है, फिर भी इसे काफी अच्छा और मजबूत माना जाता है। इसकी शॉक-प्रतिरोधी प्रकृति भी बहुत कुछ प्रदान करती है क्योंकि यह हानिकारक प्रभाव को कम करती है। चीड़ की लकड़ी नरम लकड़ी है, लेकिन देवदार की लकड़ी का फर्नीचर आसानी से एक दशक तक काम कर सकता है आज के युग में लोग जहां शान-ओ-शौकत दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी बिल्ड़िंग बना रहे हैं लेकिन भूकंप के दौरान इन मकानों में रहने वालों की जान पर भी बन आती है. जबकि जौनसार बावर में बने देवदार के लकड़ी के मकान भूकंप रोधी बताए जाते हैं. लेकिन, आधुनिकता की इस दौड़ में ग्रामीण इलाकों में भी सीमेंट कंक्रीट आदि से निर्मित मकानों को तवज्जो दी जा रही है, जिससे धीरे-धीरे काष्ठ कला विलुप्ति की ओर बढ़ रही है. *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*