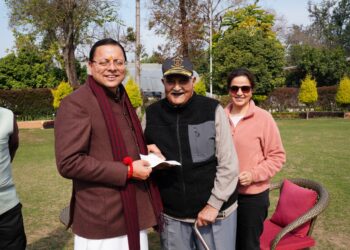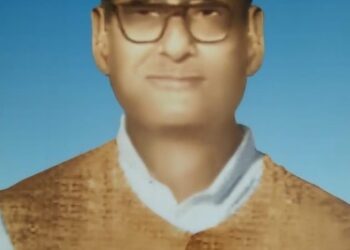डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
जहां उत्तराखंड को देवों की भूमि देवभूमि के नाम से जाना जाता है वहीं उत्तराखंड में बहुत से पर्व भी मनाए जाते हैं उनमें से एक त्यौहार है सातू आठूं का जो सभी जगह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है मल्ली नैनी भी यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया आइए आपको बताते हैं कि यह त्यौहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। बताया जाता है कि यह त्यौहार भाद्रमास कि सप्तमी व अष्टमी को मनाया जाता है।इस दिन माता गौरा व भगवान महेश की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सप्तमी के दिन माता गौरा अपने मायके से रूठ कर चली गई थी। तो उन्हें मनाने के लिए अष्टमी के दिन भगवान महेश को आना पड़ा। इस परंपरा को आज भी गांव की महिलाओं के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सप्तमी को बाजरे, मक्के की घास से गौरा और महेश की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है।ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन सप्तमी को महिलाएं व्रत रखकर एक तांबे के बर्तन में सात प्रकार के अनाज भिगोती है जिनको बिरूड कहा जाता है और भगवान महेश का स्वागत किया जाता है। अष्टमी के दिन माता गौरा को विदा किया जाता है। और इन दोनों की प्रतिमाओं को नजदीक के किसी मंदिर में विसर्जित कर दिया जाता है। और बिरुड का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत महिलाएं संतान की कामना तथा उनके कल्याण के लिए करती हैं। इस त्यौहार का बड़ा ही महत्व माना जाता है।सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य आदिकाल से ही अपने सुख दुःख में अपने परिजनों का साथ चाहता है। खुशी बाँट कर मनाना चाहता है। संभवतः इसी उद्देश्य से विभिन्न त्योहार और पर्व मनाने की परम्परा चली हो। घर-परिवार, समाज, धर्म, ऋतुओं और राष्ट्र पर आधारित विविध त्योहार हम मनाते हैं। देव-भूमि कहे जानेवाले उत्तराखंड में ऐसा ही एक पर्व है सातों-आठों या सातूँ-आठूँ। भाद्रपद मास में अमुक्ताभरण सप्तमी को सातूं, और दूर्बाष्टमी को आठूं मनाया जाता है। भाद्रपद मास में सातूं-आठूं कृष्ण पक्ष में होगा अथवा शुक्ल पक्ष में, इसका निर्धारण पंचांग से अगस्त्योदय के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार यदि यह पर्व कृष्ण पक्ष में निर्धारित हुआ तो कृष्ण जन्माष्टमी के साथ और यदि शुक्ल पक्ष में हुआ तो नंदाष्टमी के साथ मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में यह पर्व बहुत उल्लास से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ पार्वती अपने मायके आती है और दूसरे दिन शिव भगवान आते हैं। माँ पार्वती का मायका हिमालय माना जाता है। बेटी के घर आने पर उल्लास और उत्सव का माहौल होता है। उनका स्वागत, पूजन होता है और बाद में विदाईसमारोह।परंपरा के अनुसार पंचमी के दिन, जिसे बिरुड़ पंचमी कहा जाता है। पीतल के बर्तन में पाँच प्रकार के अनाज भिगोये जाते हैं। इन्हें बिरुड़ कहा जाता है। इन्हें कपड़े की पोटलियों में बाँध कर भिगोया जाता है। पोटलियों के ऊपर पाँच, सात या ग्यारह दूब के तिनके बाँधे जाते हैं। जिन्हें महिलाएँ सप्तमी के दिन पूजा में प्रयोग करती हैं। खेतों से मौसमी फसल के पौधों से गौरा की आकृति बनाई जाती है। उन्हें खूब सजाया जाता है। उन्हें सुन्दर डलिया या टोकरी में घर लाया जाता है। महिलायें सज धज कर उन्हें सर पर रखकर लाती हैं। गौरा देवी को घर के पूजा स्थल या मंदिर में स्थापित किया जाता है। महिलाएँ पूजा के समय ही पहले भिगोये अनाज की पोटलियों को गीत गाती हुई खोलती हैं और थाली में रखती हैं। सभी अपनी अपनी थालियों को आँचल से ढक कर एक दूसरे के हाथों में देती हैं। घर की लड़कियाँ-ननदें इन को छुपाती हैं बाद में भाभियाँ उन्हें ढूँढ के लाती हैं। इन अन्न के दानों को हीरे मोती कहा जाता है। बाद में कुछ अनाज के दाने और मौसमी संतरा, सेव, आँवला, नाशपाती आदि फलों को एक पिछौड़े या वस्त्र में लेकर उछाला जाता है। कुँवारी कन्याओं के आँचल में यदि ये गिरे तो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। इस अवसर पर महिलाएँ अपने पारम्परिक परिधान और गहने पहनती हैं। नृत्य और गायन होता है। इसी दिन स्त्रियाँ धागे में सात गाँठें बाँध कर बाजू में पहनती हैं। इसे ”डोर” कहते हैं। इसे सुख-सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और पति की लम्बी आयु की कामना की जाती है। इस दिन आग में पका हुआ गरम खाना नहीं खाया जाता।अगले दिन इसी तरह कुछ विशेष पौधों से शिव जी की आकृति बना कर उन्हें लाया जाता है और देवी के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। देवी को पुत्री के रूप में मायके में भरपूर स्नेह दिया जाता है और शिव शंकर का दामाद के रूप में सम्मान और पूजन किया जाता है। अनाज, धतूरे और फल-फूलों से उनकी नियम से पूजा की जाती है, और उनसे संबंधित लोक गीत गाए जाते है। एक गीत में पार्वती पेड़ पौधों से अपने मायके का पता पूछते हुए कहती है- ‘‘बाटा में की निमुवा डाली म्यर मैत जान्या बाटो कां होलो’’ अर्थात् राह के नींबू के पेड़, मेरे मायके का रास्ता कौन सा है, इसके उत्तर में नीबू का पेड़ कहता है-‘‘दैनु बाटा जालो देव केदार, बों बाटा त्यार मैत जालो’’ अर्थात् दांया रास्ता केदारनाथ की ओर जाता है, और बांया रास्ता तुम्हारे मायके की ओर जाता है। झोड़ा चांचरी और खेल के द्वारा भी विशेष गायन होता है। देव डंगरिये भक्तों को रोली अक्षत लगाकर आशीर्वाद देते है। चार पाँच दिन के बाद उनकी विधिवत विदाई की जाती है। उन्हें फिर से टोकरियों में सर पर रखकर किसी पवित्र जलधार में विसर्जित किया जाता है। विदाई का यह समारोह इतना भाव पूर्ण होता है कि महिलाओं की आँखों में आँसू भर आते हैं वे उसी तरह रोने लगती हैं मानों अपनी बेटी को विदा कर रही हों।भाद्रपद माह की इसी अष्टमी को महिलायें मुक्ताभरण सप्तमी का व्रत भी करती हैं। संतान प्राप्ति और संतान की कुशल क्षेम के लिए यह महत्त्व पूर्ण व्रत है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण ने युद्धिष्ठिर को इस व्रत की महत्ता बताई थी कि किस तरह प्राचीन समय में महर्षि लोमश ने मथुरा आकर देवकी और वसुदेव को भी अपनी संतानों के विछोह के दुख से मुक्त किया था। अयोध्या के राजा नहुष और उनकी पत्नी की कथा भी सुनाई थी। इस दिन शिव पार्वती और कृष्ण की पूजा की जाती है। सोने, चाँदी या रेशम के सूत्र में सात गाँठे लगाकर पहनने का विधान भी बताया। इस व्रत के दूसरे दिन दूर्वाष्टमी का व्रत किया जाता है। दूब की तरह वंश के फैलने की कामना से ये व्रत किया जाता है। दूब पवित्र होती है और सामान्य अवस्था में पनप जाती है और सर्वत्र फ़ैल जाती है। उत्तराखंड में महिलायें इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करती हैं। व्रत में पूजा विधि विधान से करने के साथ साथ वे एक लोक कथा भी कहती सुनती हैं। जिनमें महिलाओं के मातृत्व भाव और संतान की रक्षा का भाव परिलक्षित होता है।यह कथा एक महिला सुनाती है और सभी महिलायें प्रत्युत्तर में हामी भरती जाती हैं। कथा कुछ इस प्रकार है- प्राचीन समय में बिण भाट नामक राजा था। उसकी सात रानियाँ थीं। पर निःसंतान होने से वह बहुत दुखी रहता था। कालांतर में सबसे छोटी रानी गर्भवती हुई। राजा उसी रानी को विशेष प्रेम करता था। अन्य रानियों को बहुत ईर्ष्या होने लगी। छोटी रानी ने जब संतान को जन्म दिया तो अन्य रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने छोटी रानी से कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उन्होंने उसे बुलाया है अतः उसे उन्हें देखने ले लिए जाना चाहिए पता नहीं वो जीवित रहे या नहीं। रानी बच्चे को घर पर ही छोड़ अपनी माँ से मिलने चली गयी। वहाँ जाकर उसने देखा कि माँ तो बिलकुल स्वस्थ है। माँ से पूछने पर पता चला कि उसने कोई सन्देश भेजा ही नहीं था। वह समझ गयी कि यह उसकी सौतों का षड्यंत्र है। उसने अपनी पुत्री को वापस लौटने को कहा। इस बीच छहों रानियों ने अपनी योजना के अनुसार बच्चे को एक नौले (बावड़ी) में फेंक दिया। वह रानी दुखी मन से घर लौटी। घरवालों ने उसे बताया कि उसके कोई संतान नहीं हुई थी उसने एक शिलाखंड को जन्म दिया था। रानी दुखी होकर इधर उधर घूमने लगी उसे प्यास लगी तो वह उस बावड़ी से पानी पीने के लिए झुकी तो उसे वहाँ एक बालक दिखाई दिया उसने माँ के हार को पकड़ लिया रानी ने उसे बाहर निकाल लिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रानी ने दूब घास की रस्सी बनाकर उस बच्चे को निकाला। तभी से इस व्रत में महिलायें दूब की लम्बी जड़ों को धागे की तरह पहनती हैं जिसे “दुबज्यौड़” कहा जाता है। आधुनिक समय में स्त्रियाँ धागों से बनी कंठी या गंडे को धारण करती हैं।कुल मिलाकर यह पर्व भी जनमानस के व्यस्त जीवन में हर्षोल्लास, प्रकृति प्रेम और आस्था का प्रतीक बनकर आता है और हमें संबंधों में संवेदना की गहराई का अनुभव कराकर चला जाता है। सातूं-आठूं जो गमरा-मैसर अथवा गमरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल नेपाल और भारत की साझी संस्कृति का एक बड़ा लोक पर्व है। हिमालयी परम्परा में रचा-बसा यह पर्व सीमावर्ती काली नदी के आर-पार बसे गांवों में समान रुप से मनाया जाता है। संस्कृति के जानकार लोगों के अनुसार सातूं-आठूं का मूल उद्गम क्षेत्र पश्चिमी नेपाल है, जहां दार्चुला, बैतड़ी, डडेल धुरा व डोटी अंचल में यह पर्व सदियों से मनाया जाता रहा है। भारत से लगे सीमावर्ती गांवो के मध्य रोजी व बेटी के सम्बन्ध होने से अन्य रीति-रिवाजों की तरह इस पर्व का भी पदार्पण कुमाऊं की ओर हुआ। वर्तमान में कुमाऊं में यह पर्व मुख्य रुप से पिथौरागढ़ जनपद के सोर, गंगोलीहाट, बेरीनाग इलाके, बागेश्वर जनपद के दुग, कमस्यार ,नाकुरी तथा चम्पावत जनपद के मडलक व गुमदेश इलाकों में अटूट श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाता है।इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसमें गाई जाने वाली गौरा-महेश्वर की गाथा है जिसमें महादेव शिव व गौरा पार्वती के विवाह व उनके पुत्र गणेश के जन्म तक तमाम प्रंसगों का उल्लेख मिलता है। बिण भाट की कथा, अठवाली ,आठौं या सातूं-आठूं की कथा के नाम से प्रचलित यह धार्मिक गाथा प्रत्यक्षतः हिमालय के प्रकृति-परिवेश व स्थानीय जनमानस से जुड़ी दिखायी देती है। गौरा-महेश्वर की गाथा में हिमालय की तमाम स्थानीय वनस्पतियों-बांज, हिंसालू, घिंगारु,नीबूं, नारंगी, ककड़ी, किलमोड़ी और काफल, चीड़, देवदार सहित अनेक वृक्षों तथा वन लताओं का जो वर्णन मिलता है वह निश्चित ही अलौकिक व गूढ़ है।गाथाओं में आये गीत-प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि हमारे पुरखों को इन तमाम वनस्पतियों की उपयोगिता और उसके पर्यावरणीय महत्व की अच्छी तरह से समझ थी। गौरा के मायके जाने के प्रसंग में चीड़ को छोड़कर अन्य सभी वनस्पतियों की संवेदनशीलता प्रमुखता से उभर कर सामने आती है वे गौरा का सहचर बन कर उसका मार्ग प्रसस्त करते हैं। इसमें देवदार का वृक्ष बहुत ही आत्मीयता के साथ गौरा को अपनी पुत्री कहकर सम्बोधित करता है और उससे अपनी छांव में मायके का आश्रय पाने का अनुरोध करता है। यर्थातता में यह कथन भले ही मानवीय कल्पना लगती हो पर सही मायनों में यहां पर प्रकृति और मानव के आपसी रिश्तों को अभिव्यक्ति देने की बहुत बड़ी कोशिश की गयी है।पर्यावरण के सन्दर्भ में देखें तो बांज, देवदार, हिंसालू, और काफल आदि भूमि में जल संचित करने की क्षमता बहुत अधिक मानी जाती है, जबकि चीड़ में यह गुण नहीं पाया जाता। गाथा में आये प्रसंगों के अनुसार गौरा ने चीड़ को अभिशप्त किया हुआ है।’गौरा महेश्वर गाथा में सबसे बड़ी बात जो देखने में आती है वह यह है कि शिव व पार्वती अपने देव रुप से इतर आम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। इस गाथा में पहाड़ी जन-जीवन व मौजूद समाज के विविध पक्षों को यथार्थ तौर पर गूंथने की अद्भुत कोशिश हुई है। गौरा महेश्वर की गाथा में इन दोनों का व्यक्तित्व एक सामान्य नर-नारी के रुप में इस तरह उद्घाटितहुआहै।
नदि का किनार लौलि गोवा चराली
नदी पार मैसर गुसैं बाकरा चराला
इस अलौकिक बिम्ब में मैसर यानि महेश्वर गुंसै (गुंसाई) नदी के पार बड़ी तन्मयता से बकरी चराते हुए नजर आ रहे हैं। महेश्वर की इस असाधारण भूमिका के जरिये एक साधारण किसान का जो संघर्षमय व कर्मशील चरित्र जिस सहजता से उजागर हुआ है उसे निश्वित ही मानवीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस गाथा के अनेक मार्मिक गीत गौरा के सीधे-सादे व्यक्तित्व और आम स्त्री मन की व्यथा व उसकी पीड़ा को उद्दात भाव से प्रकट करते हैं। प्रो. देवसिंह पोखरिया के अनुसार आंठू में गाये जाने वाले सभी गीतों में गेय तत्व की प्रधानता दिखायी पड़ती है।इन गाथाओं में पहाड़ के जनजीवन की यथार्थता का गूढ़ भाव दिखायी देता है।जीवन के कठिन संघर्ष में में लौलि यानी गौरा जब अपने ससुराल हिमालय से मायके को जा रही होती है तो वह बार-बार मार्ग भटकती रहती है जगह-जगह पर तमाम पेड़-पौंधों व लता झाड़ियों से वह रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ती रहती है। प्रतीक रूप में यहां पर समूची प्रकृति गौरा के मदद के लिए पथ प्रदर्शक और आश्रय दाता की भूमिका निभाने का प्रयास कर रही होती है। गौरा ने मायके जाने के लिए चीड़, बांज ,हिसालू, ककडी़ सहित,अनेकानेक वनस्पतियों से रास्ता पूछते-पूछते वह नींबू व नारिंग के पेड़ के पास भी आती है और उन्हें आर्शीवचन स्वरुप कहती है-
‘बाटा में की निमुवा डाली, म्यर मैत जान्या बाटो कां होला
दैनु बाटा जालो देव केदार, बों बाटा त्यार मैत जालो
धौला रंग फुलिये डाली, पीला रंगन पाके
तेरा फल निमुवा डाली, मनुसिया रे खाला
बाटा में की नारिंग डाली, म्यर मैत जान्या बाटो कां होला
दैनु बाटा तिरजुगी जालो, बों बाटा त्यार मैत जालो
नीला रंगन फुलिये डाली, राता रंगन पाके
तेरा फल नारिंग डाल, देवता चढ़ला।’
अर्थात नींबू की डाली बताओे मेरे मायके को जाने वाला रास्ता कौन सा है? तब नींबू की डाली विनम्र भाव से उत्तर देती है कि दाहिनी ओर का रास्ता शिव के केदार को जाता है और बांई ओर का रास्ता तुम्हारे मायके को जाता है। तब गौरा खुस होकर उसे आर्शीवचन देती है कि तुम धवल (सफेद)रंग के फूलों से भरे रहो और तुझ में पीले रंग के फल पकें और तेरे फल मनुष्य के काम आते रहें। इसी तरह की बात गौरा नारिंग के पेड़ के लिए भी कहती है जिसमें उसको नीले रंग के फूलों, व सुनहरे रंग के फलों से आवृत रहने और उसका फल देवताओं को अर्पित होने का आर्शीवाद देती है।कुल मिलाकर श्रुति परम्परा में चली आ रही इन गाथाओं व लोकगीतों में वेद-पुराणों से लेकर स्थानीय प्रकृति और समाज से जुड़े एक से बढ़कर एक रोचक आख्यान समाहित हैं। यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गौरा और महेश्वर हिमालय वासियों के साथ एक अत्यंत ही आत्मीय रिश्ते में नजर आते हैं। यंहा पर यह बात अति महत्व की है कि पहाड़ के लोक ने निश्छल भाव से गौरा को बेटी/दीदी तथा महेश्वर को जवाईं/भीना (जीजा) के रुप में प्रतिस्थापित किया हुआ है जो कि अन्यत्र र्दुलभ है। इस पर्व की मान्यता है कि सप्तमी को मां गौरा ससुराल से रूठकर अपने मायके आ जाती हैं, और उन्हें लेने के लिए अष्टमी को भगवान महेश (मैसर) यानी शिव आते हैं। इस अवसर पर सों नामक घास और धान के पौधों से गौरा-महेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आकर्षक कुमाऊनी वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाया जाता है।कुमाऊं में भगवान शिव को ‘मैसर’ या ‘भिनज्यू’ (जीजा जी) और गौरा को ‘गंवरा दीदी’ के रूप में संबोधित किया जाता है, जो इस क्षेत्र के लोगों के देवी-देवताओं के साथ गहरे मानवीय संबंध को दर्शाता है। इस दौरान दीदी-जीजू से संबंधित लोकगीत ‘झोड़ा चांचरी’ के रूप में गाए जाते हैं।महिलाएं दोनों दिन उपवास रखती हैं। अष्टमी की सुबह गौरा-महेश को बिरुड़ अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। मंगल गीत गाते हुए मां गौरा को ससुराल के लिए विदा किया जाता है। अंत में, मूर्तियों को स्थानीय मंदिर या नौलों में विसर्जित किया जाता है।यह त्योहार कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*