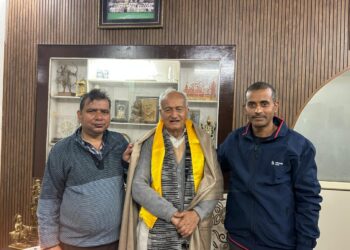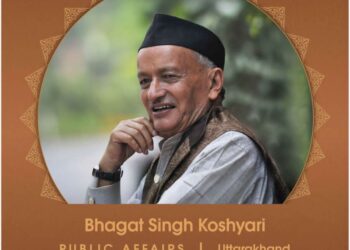डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
उत्तराखंड की लोक संस्कृति में हरेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की संक्रांति को मनाया जाता है। यह खेती, हरियाली और प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है।यह त्योहार मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी है। बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला हरेला उत्सव केवल एक सांस्कृतिक परंपरा से कहीं अधिक है, यह पारिस्थितिकी संतुलन, स्थिरता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का आह्वान है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। कई जगह इसे हरियाली तीज के रूप में भी देखा जाता है। महिलाएं नए वस्त्र पहनकर पूजा करती हैं और हरियाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। लोकगीत, झोड़ा-छपेली और पारंपरिक नृत्य इस दिन की विशेषता होते हैं। हरेला पर्व हमें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। इस दिन स्कूल, पंचायत, वन विभाग, और स्वयंसेवी संस्थाएं वृक्षारोपण अभियान चलाती हैं। यह पर्व बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है।उत्तराखंड सरकार भी अब हरेला को राजकीय पर्व के रूप में मना रही है। हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे हम हरियाली बोते हैं और उसे सींचते हैं, वैसे ही हमें अपने रिश्तों, समाज और पर्यावरण को भी प्रेम और सेवा से सींचना चाहिए। आइए, हम सभी मिलकर इस पर्व को उत्साह से मनाएं और वृक्षारोपण करके अपनी धरती को हराभरा बनाएं। भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति कहा जाता है। हमारे पूर्वज सर्वज्ञ थे। वे सृष्टि के सबसे बड़े सत्य को जान गए थे कि सृष्टि का अस्तित्व प्रकृति की समृद्धि पर आश्रित है, इसलिए उन्होंने ऐसा जीवनदर्शन विकसित किया जो प्रकृति उपासक था, अरण्य आदृत था और इसी दर्शन से विकसित हुईं ऐसी जीवनशैली जो पर्यावरण के प्रति सजग और आस्थावान थी। हमारे पूर्वज वन सम्पदा का महत्व समझते थे और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक थे। पर्यावरण के तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति आदि के प्रति हमारे ग्रंथों में, हमारी लोकसंस्कृति में असीम श्रद्धा का भाव परिलक्षित होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल में विष्णु जी का वास और ज्ञान देवता के माध्यम से बरगद और शीतला माई का वास, मांगलिक कार्यों में आम की लकड़ी व आम के बौर को शुभ मानकर वृक्षों का संरक्षण करने वाले हमारे पूर्वज कैसी अनूठी दूरदृष्टि रखते थे। भारत की महान संस्कृति में तुलसी एकादशी, आंवला नवमी, वट सावित्री आदि पर्व प्रकृति संरक्षण के मुख्य सोपान हैं।भारतीय संस्कृति चौरासी लाख योनियों में मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ मानती है,लेकिन अन्य योनियों की महत्ता को भी स्वीकार करती है। आशय है कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है और यह तभी संभव है जब प्रकृति के प्रति मनुष्य की आत्मीयता ठीक उसी प्रकार हो जैसे अपने माता-पिता, भाई, बहन, गुरु और सखा आदि प्रियजन से होती है। यह आत्मीयता भारतीय संस्कृति में इस तरह रची-बसी है कि उसकी झलक अशेष व्रत पूजाओं तीज त्योहार, उत्सवों, लोकगीतों, लोककथाओं, कहावतों, परंपराओं के साथ ही लोकव्यवहार में देखी जा सकती है। लोक जीवन की धारणा में नदी मां हैं, पहाड़ मित्र हैं, चिरैया सहेली है, धरती मां हैं तो अन्न देवता हैं और वन हमारे आधार। प्रकृति के वे सारे तत्व जिनसे मिल कर यह पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जड़-चेतन बने, वे मनुष्य के घनिष्ठ हैं, पूज्य हैं ताकि मनुष्य का उनसे तादात्म्य बना रहे और मनुष्य इन सभी तत्वों की रक्षा के लिए सजग रहे। रामायण, महाभारत, गीता, वायु-पुराण, स्कन्दपुराण, भविष्य पुराण, वराहपुराण, ब्रह्मपुराण, मार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण, गरुणपुराण, श्री विष्णुपुराण, भागवतपुराण, श्रीदेवी भागवत पुराण वेद, उपनिषद तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थ, पेड़-पौधे, जीव-जन्तुओं पर दया करने की सीख देते हैं. मानसिक शान्ति, शारीरिक सुख, इन सबकी पूर्ति के साधन प्राकृतिक सम्पदा ही है. गेहूँ, जौ, तिल, चना, चन्दन, लाल पुष्प, केसर, खस, कमल, ताम्बूल, श्वेतपुष्प, बांस, मिट्टी, फल, तुलसी, हल्दी, पीत-पुष्प, शहद इलाइची, सौंफ, उड़द, काले-पुष्प, सरसों के फूल, मुलेठी देवदारू, बिल्व वृक्ष की छाल, आम, पला, खैर, पीपल, गूलर, दूब, कुश आदि को संरक्षित रखने के उद्देश्य से इन्हें किसी दिन, त्यौहार, देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना से जोड़ा गया है. औषधि के रूप में फलों तथा जड़ी-बूटियों की रक्षा करने की बात कही गयी है और इन्हें घरों के निकटस्थ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की सलाह दी गयी है. जैसे- अंगूर, केला, अनार, सेव, जामुन, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, नींबू, अदरक, आंवला, घिया, बादाम, आम, टमाटर, अखरोट, अजवाइन, अनानास, असगन्द, गिलोय, तम्बाकू, तरबूज, तुलसी, दालचीनी धनिया, पुदिना, संतरा, पान, पीपल, बबूल, ब्राह्मीबूटी, कालीमिर्च, लालमिर्च, लौंग, हरड़, बहेड़ा आदि अनेक बूटियों का प्रयोग करने से मनुष्य निरोग रह सकता है. वेदों में कहा गया है कि मनुष्य शरीर पृथ्वी, जल, अंतरिक्ष, अग्नि और वायु जैसे पांच तत्वों से निर्मित है। यदि इनमें से एक भी तत्व दूषित होता है तो इसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ेगा। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को देवी-देवताओं का स्थान दिया है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु व नदियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता था। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों को औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। पेड़ों जैसे पीपल, वटवृक्ष व केला को आज भी पूजा जाता है। पेड़ों को लगाना पुत्र प्राप्ति के समान माना गया है परंतु समय परिवर्तन के साथ-साथ सब कुछ परिवर्तित होता गया। हम सब आधुनिकता के पथ पर अग्रसर हो गए। पूर्वजों की ओर से बताए गए मूल्य और संस्कार हमें अंधविश्वास लगने लगे। हम विकास और तकनीक पर गर्व करने लगे। औद्योगीकरण एवं असंख्य वाहनों के आवागमन के फलस्वरूप वायुमंडल पूर्ण रुप से दूषित हो चुका है। फसलों की पैदावार में वृद्धि करने के लिए उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा। परिणामस्वरूप मृदा के साथ-साथ उसमें उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न भी विषैले होने लगे हैं। उद्योगों से उत्पन्न अनावश्यक विषैले पदार्थों से नदियां भी प्रदूषित हो चुकी हैं। भूजल स्तर निम्न हो चुका है। कुल मिलाकर आज के समय में हम अन्न, जल व वायु को प्रदूषित कर चुके हैं। अधिकतर जंगल मैदानों में परिवर्तित हो चुके हैं। वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है। बहुत सी प्रजातियां हमेशा के लिए लुफ्त हो चुकी हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण के सभी घटक असंतुलित एवं प्रदूषित हो चुके हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़कर जा रहे हैं जिसमें जल, वायु और मृदा संपूर्ण रूप से प्रदूषित होंगे और संसाधन समाप्त हो चुके होंगे। इस सबके लिए मात्र मानव जाति ही जिम्मेदार है। जनमानस में जागृति लाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन व नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख रहे हैं। समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होते रहते हैं और इनमें अधिकतर देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं परंतु पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सब पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना होगा, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक एवं एक सतर्क प्रहरी की भूमिका निभानी होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें पुन: वेदों का रुख करने के लिए कहा था। वह यह कहना चाहते थे कि वेद हमारी हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना होगा। जंगलों को बचाना होगा, अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगेतभी धरती पर जीवन संभव रहेगा। आओ सभी मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम पर्यावरण संरक्षण में पूर्ण योगदान देंगे।. *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*