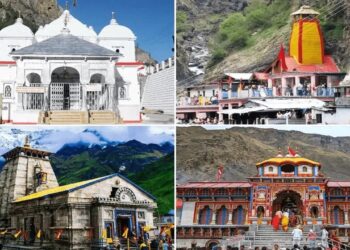डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
आज की व्यस्ततम् और भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखना हर व्यक्ति के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भौतिक विकास की दौड़ में आमजन हमारी पारम्परिक पोषणीय भोजन व्यवस्था के पुरातन आयामों को भूलता जा रहा है। आमजन के कीचन से ऐसे कई खाद्यान्न नदारद होते जा रहे है जिनका कुछ दशको पूर्व हमारे घरों में अपरिहार्य स्थान हुआ करता था। बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ भोजनशैली मे जंक फुड़ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो का चलन अनियंत्रित रूप से बढ़ता जा रहा है और यह हमारा तथा कथित स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। असंतुलित खानपान और जीवनशैली जनित बीमारियाँ आम होती जा रही है। भोजन न केवल मनुष्य जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि के साथ-साथ पर्यावरण सततता को भी आकार देता है। इसका प्रभाव जैव विविधता, जल उपयोग पर पड़ता है तथा यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। जैसा कि हमारा लक्ष्य मानव स्वास्थ्य को हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के साथ संतुलित करना है, संधारणीय भोजन विकल्प हमारे लिए अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।अध्ययनों से पता चलता है कि हमारा वर्तमान खाद्य प्रणालियाँ ग्रह संसाधन पर दबाव डाल रही हैं। फिर भी, इस चुनौती के बीच आशा की एक किरण है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट भारत की खाद्य प्रथाओं पर टिकाऊ मॉडल के रूप में काश डालती है। उल्लेखनीय रूप से, यदि दुनिया ने भारत की उपभोग आदतों को अपनाया, तो वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए 2050 तक पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता पड़ेगी। यह मान्यता पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वैश्विक आंदोलन में भारत एक संभावित नेता के रूप में भारत को स्थापित करता है। पारंपरिक भारतीय आहार, जो काफी हद तक है वनस्पति-आधारित है, पर्यावरण की दृष्टिकोण से एक टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आता है। संसाधन गहन पशु उत्पाद के बजाये अनाज, दाल, मसूर, तथा सब्ज़ियों आदि पर निर्भर रहते हुए, भारतीय आहार कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं।डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी देश भारत के उपभोग पैटर्न का पालन करें, तो संसाधनों की वैश्विक मांग काफी कम होगी। रिपोर्ट का अनुमान है कि यदि भारत के आहार मॉडल को दुनिया भर में अपनाया जाता है, तो 2050 तक दुनिया को खाद्य उत्पादन बनाए रखने के लिए केवल 0.84 पृथ्वी की आवश्यकता होगी।रिपोर्ट में विशेष रूप से 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। यह राष्ट्रीय श्री अन्न (मिलेट्स) अभियान जैसी पहल के माध्यम से मिलेट्स जैसी पारंपरिक और लचीली फसलों पर जोर देती है।भारत की प्रथाएँ दर्शाती हैं कि कैसे स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएँ भूमि उपयोग को कम करते हुए, प्रकृति को बहाल करते हुए और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए स्वस्थ आहार का समर्थन कर सकती हैं। मिलेट के पोषण संबंधी लाभों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने इसे पोषक अनाज के रूप में वर्गीकृत करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अलावा, इसे श्री अन्ना नाम देकर इस चमत्कारी भोजन को एक नया अर्थ और आयाम दिया गया है।वैश्विक मंच पर इन प्राचीन अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। यह मील का पत्थर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि सरकार बाजरा उत्पादकता बढ़ाने और इन पौष्टिक अनाजों को रोजमर्रा के आहार में शामिल करते हुए खाद्य उपभोग पैटर्न को बदलने का प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न पहल शुरू की गई हैं, जिनमें शामिल हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 खाद्य उत्पादन के लिए भारत के समग्र और सतत दृष्टिकोण की सराहना करती है, जो दूसरे देशों के अनुसरण के लिए एक वैश्विक उदाहरण के रूप में स्थापित करती है। सांस्कृतिक रूप से आधारित आहार को प्राथमिकता देकर तथा पारंपरिक खाद्य पदार्थों को रोजमर्रा के भोजन में विशेष रूप से विविध भारतीय थाली में सम्मेलित करकर; भारत न केवल पोषण सुरक्षा बढ़ा रहा है बल्कि जैव विविधता तथा पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है। ये पहलें स्थानीय कृषि पद्धतियों और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती हैं, जो स्वस्थ, अधिक लचीली खाद्य प्रणालियाँ बनाने के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित हैं। जैसा कि भारत स्थायी खाद्य प्रथाओं का चैंपियन बना हुआ है, यह अन्य देशों को ऐसी ही रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है जो लोगों और ग्रह दोनों का सम्मान करते हैं। भारतीय थाली का जिक्र होते ही मन में अलग-अलग व्यंजनों से भरी तस्वीर उभरती है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है।हर राज्य की अपनी विशेष थाली होती है, जिसमें अलग-अलग व्यंजन शामिल होते हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए खास सामग्री की जरूरत होती है, जो स्वाद और पोषण देती हैं। *लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*