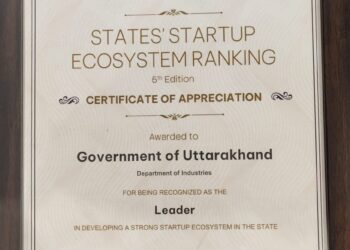डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला
वनरावत जनजाति पिथौरागढ़ के डीडीहाट, धारचूला विकासखंड के कूटा चौरानी, मदनपुरी, किमखोला, कमतोली, जमतड़ी समेत करीब आठ गांवों में निवास करती हैं। यह राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। यह जनजाति तेजी से विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को भी चिंता जता चुके हैं। इस जनजाति का साक्षरता दर मात्र 35 फीसद है। यहां स्वास्थ्य सेवाएं भी न के बराबर हैं। विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही उत्तराखंड की एकमात्र वनरावत जनजाति आदिम जनजाति को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने चिंता जताई है। दरअसल, एनसीपीसीआर ने एक खबर का संज्ञान लिया है, जिसमें पिथौरागढ़ की वनरावत जनजाति के घटने के लिए वहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को उजागर किया गया है। इसमें नवजात शिशुओं को टीकाकरण जैसी बुनियादी सेवाएं तक न मिलने की बात कही गई है।
पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट खंड के निकटस्थ सघन वनों में आखेटकीय एवं गुहावासी जीवन बिताने वाले वनरौतों राजियों को अपनी पृथक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण एक पृथक वर्ग के रूप में माना जाता है। इनकी प्रजातीयता एवं जातीयता के विषय में इतिहासज्ञ, नृविज्ञानी एवं समाजशात्री एकमत नहीं हैं। कोई भाषा के आधार पर इनका संबंध आग्नेय मुंडा परिवार से आए मानता है, तो कोई राजकिरात कहे जाने के कारण रावत, राउत, रौत, कहते हैं। फलतः इनके संबंध में प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार इन्हें अस्कोट के रजवार शासकों के द्वारा इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने से पूर्व तक इस क्षेत्र पर इस वनरौतों का अधिकार था। किंतु रजवारों द्वारा इस क्षेत्र को अधिकृत करने के बाद या तो ये स्वयं इस क्षेत्र को छोड़कर जंगलों में चले गए या इन्हें खदेड़ दिया गया।
जो भी हो ये लोग पुराने समय से ही यहां पर घनघोर जंगलों के बीच पर्वतीय गुफाओं को आश्रय बनाकर, कंदमूल एवं शिकार कर जीते आ रहे हैं। राजकिरात के नाम से जाने जाने वाले ये गुहाश्रयी लोग कभी इस क्षेत्र के अधिपति हुआ करते थे। इसका संकेत वाराही संहिता के उन प्रकरण में मिलता है, जिसमें अमरवन तथा चीड़ा के मध्यस्थ क्षेत्र में राज्य किरातों की स्थिति बताई गई है। इसमें पुरतत्वविदों के द्वारा अमरवन की पहचान जागेश्वर से तथा चीड़ की तिब्बत से की गई है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर इनमें कतिपय हिन्दू परम्पराओं का अनुपालन पाया जाने पर इन्हें हिन्दू समाज की परिधि में रखा जाता है। राजी और रावत नाम से पहचाने जाने वाले ये लोग अपनी एक भाषा बोलते थे, जिसका सम्बन्ध शायद तिब्बत-वर्मा परिवार से है। सामान्य रूप से पतले और चेहरे पर कम बाल वाले ये राजी दिखने में मंगोलियन नस्ल के दिखाई देते हैं। सियासी लाभ के लिए खोले गए तमाम स्कूल.कॉलेज जहां नाममात्र की छात्र संख्या होने पर भी अस्तित्व में हैं, वहीं राजनीति में नगण्य दखल रखने वाले आदम जनजाति वनराजि बच्चों को शिक्षित करने के लिए जौलजीबी में खोला गया स्कूल वर्ष 2017 में कम छात्रसंख्या के बहाने बंद कर दिया गया। हालांकि इस स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के आदेश हुए थे, लेकिन अधिकतर बच्चे दूर के स्कूल में जाने की बजाय घर बैठ गए। बच्चों को शिक्षित कर इस आदम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों को इससे खासा झटका लगा है।
वनराजियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पूर्व विधायक स्वण् हीरा सिंह बोरा ने कई दशकों तक काम किया। उनका संघर्ष काम आया। वर्ष 2000 में आदिम वनराजि बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति सेवा संस्थान संस्था के माध्यम से जौलजीबी में विद्यालय स्थापित किया। आवासीय स्कूल खुला तो वनराजि परिवार बच्चों को इस स्कूल में भेजने लगे। वनराजि बच्चों को घर जैसा ही माहौल मिल सके और किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए हॉस्टल में वार्डन भी वनराजि परिवार के लोगों को ही रखा गया। पूर्व विधायक बोरा के प्रयासों से इस विद्यालय में वनराजि बच्चों की संख्या 50 से अधिक हो गई थी। स्कूल संचालन के लिए सालाना केवल 10 लाख रुपये की धनराशि मिलती थी। वर्ष 2013 में हीरा सिंह बोरा की मृत्यु के बाद स्कूल प्रबंधन अधिक ध्यान नहीं दे पाया। इसके बाद दिल्ली की एक संस्था सार्थक प्रयास के माध्यम से भी स्कूल संचालन की कोशिश की गई। मार्च 2017 में इस स्कूल को फंड मिलना भी बंद हो गया। मार्च 2017 से 31 जुलाई तक अपने प्रयासों से डीडीहाट यूथ सोसाइटी ने इस स्कूल को संचालित किया। अगस्त 2017 में यहां पढ़ने वाले सभी 48 वनराजि बच्चों को बलुवाकोट के जनजाति स्कूल में दाखिला दिलाने के निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी हुए, लेकिन कक्षा तीन से पांच तक के 12 बच्चों और कक्षा एक व दो के 20 बच्चों ने किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया। यह 32 बच्चे अब भी घरों में ही बैठे हैं।
डेढ़ हजार से भी कम है वनराजि जनजाति की आबादी पिथौरागढ़ जिले के अलावा कुछ परिवार चंपावत जिले के खिरद्वारी गांव में भी रहते हैं। राज्य में इनकी जनसंख्या 1500 से कम है। वनराजि समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा रहा। तमाम प्रयासों के बावजूद बालिकाओं की शिक्षा में रुचि कम ही रही। वनराजि समाज से जानकी ने वर्ष 2016 में हाईस्कूल पास किया था। जानकी अपने समाज से हाईस्कूल पास करने वाली पहली बालिका बनी थी। इस समाज से केवल दो ही लोग सरकारी नौकरी में हैं। गगन रजवार दो बार विधायक रहे, भले ही वनराजि समाज अभी भी पूरी तरह से समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सका है, लेकिन वनराजि समाज से राजनीति में विधान सभा तक प्रतिनिधित्व हो चुका है। गगन रजवार दो बार धारचूला से विधायक चुने गए।1964 से वनराजियों के लिए काम करते रहे हीरा सिंह बोरा डीडीहाट, अनुसूचित जनजाति सेवा संस्थान के माध्यम से वनराजियों के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम चलाने वाले पूर्व विधायक स्वण्हीरा सिंह बोरा ने वर्ष 1964 से कार्य शुरू किया था। उस दौर में उन्होंने बियाबान जंगलों में रहने वाले वनराजियों के बीच जाकर उनको अक्षर ज्ञान कराने की मुहिम शुरू की। पिथौरागढ़ के वनराजि गांवों के साथ ही चंपावत के खिरद्वारी गांव जाकर भी वनराजियों को भी शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजी बोली पर देश में पहली पीएचडी करने वाले भाषाविद डॉण् शोभाराम शर्मा बताते हैं कि यूनेस्को ने पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में रहने वाले राजी जनजाति की बोली को एटलस में शामिल नहीं किया है, यह भाषा भी विलुप्ति की कगार पर है।
शिक्षा ही नहीं पूरे जीवन और समाज के प्रति इनका भाव उदासीनता का रहता है। ये अब अपनी शिकारी संग्राहक की जीवन शैली को कभी का त्याग चुके हैं। मगर धन संचय की प्रवृति इनमें अभी भी नहीं है। भविष्य को लेकर एक बेफिक्री इनके पूरे समाज में देखी जा सकती है। जिन्हें बस अभी की चिंता है। एक तरह से इन्हें सुखी और मस्त कहा जा सकता है। मगर बीमारी, आपात स्थिति, दुर्घटना या भुखमरी के हालात में इन्हें स्थानीय साहूकारों या ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस कारण ये उनके कर्ज तले हमेशा दबे रहते हैं। कोई भी बचत ये करते नहीं देखे गए हैं। मनरेगा के लिए खाते जरूर खुले हैं जो पैसा निकालने के काम अधिक आते हैं। उपभोक्तावादी विलासिताओं के नाम पर इनके पास आजकल मोबाइल काफी परिवारों के पास हैं। जिन गांवों में बिजली है वहां टेलीविजन भी दिखने लगे हैं। मगर जो गांव अभी भी अस्कोट मृग विहार की सीमा के भीतर आते हैं, वहां बिजली नहीं पहुंची है वे एमपी3 साउंड सिस्टम चलाते हैं। इनके बीच कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों के अनुदान लिए जा चुके होंगे, मगर इनके बीच स्थान बनाने और सार्थक बदलाव लाने में गिने चुने लोगों और संस्थाओं को ही कुछ हद तक सफलता मिल सकी है। वन विभाग से इनका लगातार संघर्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहता है। प्रत्यक्ष तौर पर इनके रोजगार जिसमें लकड़ी चिरान और वन्य उत्पाद इकट्ठे कर बेचना मुख्य है और मृग विहार के बीचों बीच स्थित इनकी बसासतें वन विभाग की नजर में अवैध हैं। जिन्हें पूर्व में कई बार इधर से उधर खदेड़ा भी गया है। जिस कारण आधुनिक समय में भी अपना पूर्व का घूमंतू व्यवहार त्यागने के बावजूद भी पूरी तरह से किसी एक गांव के नहीं हो सके हैं, क्योंकि इनके नाम किसी गांव की कोई जमीन दर्ज ही नहीं है। इनकी जितनी भी बसासतें हैं उनमें इनके नाम जमीनें न के बराबर हैं। कुछ ही परिवारों को जमीन के पट्टे मिल पाए हैं। आरक्षित जनजाति का दर्जा दिया गया है। जिसका लाभ इन्हें सरकारी नौकरियों में तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है।