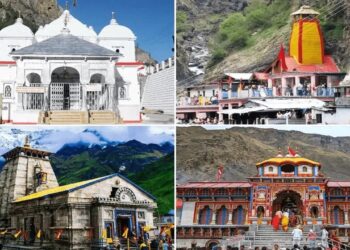डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, इसका अंदाजा इस से लगाया जा सकता है कि लोगों को मजबूरी में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। रविवार को इंडिया गेट पर जब नागरिक ‘साफ हवा’ की मांग लेकर सड़कों पर उतरे, तो यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह उस शहर की पुकार थी, जो हर साल अपने बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को प्रदूषण की भेंट चढ़ते देख रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, लेकिन सवाल यह है कि सरकारें आखिर कब तक आंखें मूंदे रहेंगी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। आईटीओ जैसे इलाकों में यह 498 तक दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी की सीमा से भी आगे है। वजीरपुर, बवाना, विवेक विहार, रोहिणी और नेहरू नगर में हालात लगभग समान हैं।एनसीआर के शहरों में भी स्थिति बेहतर नहीं है, नोएडा 391, गाजियाबाद 387, गुरुग्राम 252 पर है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली-एनसीआर अब गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने अब तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू नहीं की हैं, यानी निर्माण कार्य, ट्रक प्रवेश और डीजल जेनरेटरों पर प्रतिबंध अब तक टाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपदा है। विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण अब सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि यह कण शरीर में प्रवेश कर खून के जरिए लीवर, किडनी और अन्य अंगों तक पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को पहले से हृदय, अस्थमा, किडनी या लिवर की बीमारी है, उनके लिए यह हवा मौत का फरमान साबित हो सकती है।अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्थमा, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के केस तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जैसी समस्याएं भी अब आम होती जा रही हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार, साल 2023 में दिल्ली में करीब 17,188 लोगों की मौत प्रदूषित हवा के कारण हुई। यानी हर सात में से एक व्यक्ति की मौत का कारण अब वायु प्रदूषण है। यह आंकड़ा 2018 के मुकाबले कहीं अधिक है, जब यह संख्या 15,786 थी। इतना ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर से 14,874 मौतें और मधुमेह (हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लुकोज) से 10,653 मौतें दर्ज की गई। लेकिन प्रदूषण से होने वाली मौतें इन दोनों से भी ज्यादा हैं, बताता है कि यह सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक जनस्वास्थ्य संकट बन चुकी है।ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र का कहना है कि वायु प्रदूषण अब दिल्ली के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना किसी महामारी का प्रकोप। जब तक विज्ञान-आधारित नीतियां लागू नहीं होंगी, तब तक दिल्ली एक गैस चेंबर बनी रहेगी। इतने भयावह हालात के बावजूद सरकार की ओर से ठोस कदमों की कमी दिखती है। जनता के धैर्य की सीमा अब खत्म हो रही है। इसलिए रविवार को जब सैकड़ों नागरिक इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए, तो यह केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष था। लोगों ने नारे लगाए ‘हमें सांस दो’, ‘साफ हवा हमारा अधिकार है’, ‘जीना है तो कुछ करना होगा।’ दरअसल दिल्ली का प्रदूषण कई स्रोतों से आता है, पराली जलना, वाहन उत्सर्जन, धूल, औद्योगिक धुआं और निर्माण कार्य। पराली पर हर साल वही बहस दोहराई जाती है, लेकिन व्यावहारिक समाधान अब तक नहीं निकला।सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, ई-वाहनों को प्रोत्साहन देने और निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी जैसे कदम अभी भी आधे अधूरे हैं। सरकारें केंद्र और राज्य में एक-दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली की हवा किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानती। यह पूरे एनसीआर की समस्या है और इसका हल भी सामूहिक जिम्मेदारी से ही निकलेगा। यह समय ‘कमेटी बनाने’ का नहीं, बल्कि ‘कार्रवाई करने’ का है। स्कूल बंद करने या दफ्तरों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ पर भेजने से समस्या अस्थायी रूप से टल सकती है, लेकिन खत्म नहीं होती। सरकार को दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे, जैसे कि सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण के लिए एयर-कलिटी एक्शन प्लान को सफिय करना, निर्माण स्थलों पर स्वचालित मॉनिटरिंग, डीजल वाहनों पर सख्त नियंत्रण, और पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना। साफ हवा केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकार का सवाल है।जब दिल्ली के नागरिकों को हर सांस के साथ अपने स्वास्थ्य की कीमत चुकानी पड़ रही है, तो यह लोकतंत्र के लिए भी शर्म की बात है। दिल्ली की हवा अब एक अदृश्य हत्यारा बन चुकी है, जो धीरे-धीरे, चुपचाप हर घर में दस्तक दे रही है। डॉक्टर, रिसर्चर और पर्यावरणविद् सभी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले सालों में यह शहर रहने लायक नहीं बचेगा। सरकारों को समझना होगा कि जनता की यह लड़ाई सिर्फ एक दिन की ‘प्रोटेस्ट फोटो’ नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। आज अगर हम सांस नहीं ले पा रहे, तो कल शायद बोल भी न पाएं। हकिकत यह है कि सरकारें बदलती रहें, नीतिर्या बनती रहें, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक दिल्ली का आसमान धुएं में डूबा रहेगा।अब वक्त है कि’ स्वच्छ हवा’ को एक मौलिक अधिकार की तरह लागू किया जाए क्योंकि अगर सांस ही नहीं बची, तो शासन और राजनीति दोनों बेअर्थ हैं। दिल्ली को बचाना अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आपातकालीन जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी हर नागरिक, हर नेता, हर संस्थान की है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन-मृत्यु का प्रश्न बन चुकी है। यह लोकतंत्र का दर्पण है, जो हमें बताता है कि अगर नागरिक अपने ही शहर में सांस लेने को मजबूर हों, तो विकास का सारा शोर बेमानी है। इसलिए उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब केंद्र और राज्य मिलकर दिल्ली में ऐसी नीतियां बनायें जिससे लोगों के सांसों पर जो संकट मंडरा रहा है उस से निजात दिलाने में मदद मिले। प्रकृति कितनी हमारे साथ है, यह बात अब हम सबको साफ हो ही चुकी है। हमने जंगल, हवा और पानी— इन तीनों का बहुत तिरस्कार किया है। हमने पृथ्वी को तो लगभग समाप्त कर ही दिया, लेकिन समुद्र और आकाश को भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज प्रकृति के सभी तत्व गहरी चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि इन बिगड़ते हालात का सीधा और गंभीर प्रभाव किस पर पड़ेगा। यह जानकारी केवल अध्ययनों, शोध पत्रों और अखबारों तक सीमित रह गई। शोर-शराबे के बावजूद हमने कभी गंभीरता से उन बातों को नहीं लिया, जिनसे हमारा शरीर वर्तमान और आने वाले समय में किसी न किसी रूप में प्रभावित होता रहेगा। हमें अपने घर और आसपास अधिक से अधिक हरियाली बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पौधे वायु प्रदूषण को अवशोषित करके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अब तो ऐसे पोधे भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जहां तक संभव हो, पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। यह न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। इस समय निर्माण कार्यो से भी बचें। यह स्पष्ट है कि अब हमें व्यक्तिगत रूप से भी कदम उठाने होंगे, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तब जबकि इसका नियंत्रण स्वयं लोगों के हाथ में हो। यही सबसे बड़ा और प्रभावी कदम होगा। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं*